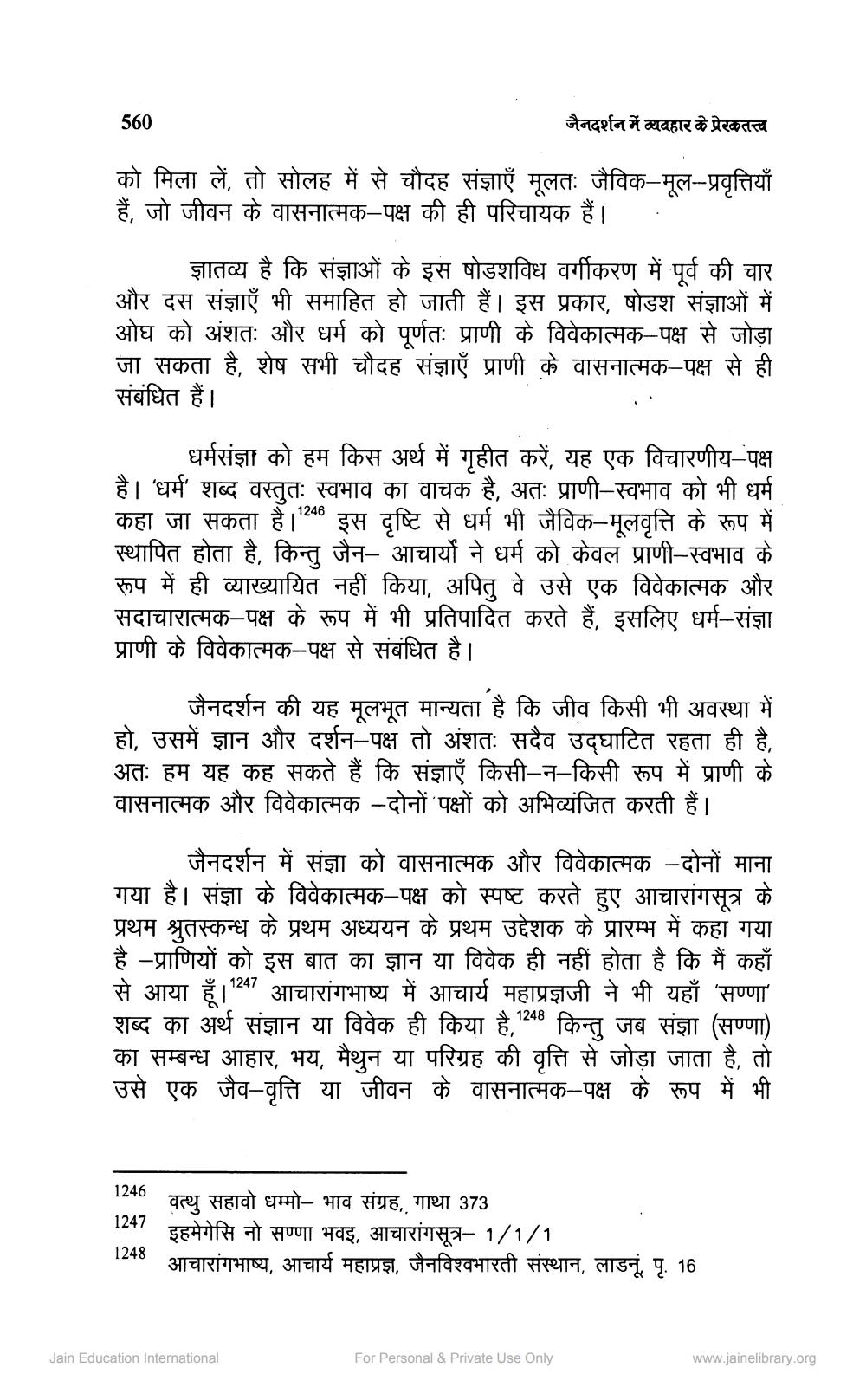________________
जैनदर्शन में व्यवहार के प्रेरकतत्त्व
को मिला लें, तो सोलह में से चौदह संज्ञाएँ मूलतः जैविक-मूल-प्रवृत्तियाँ हैं, जो जीवन के वासनात्मक - पक्ष की ही परिचायक हैं ।
560
ज्ञातव्य है कि संज्ञाओं के इस षोडशविध वर्गीकरण में पूर्व की चार और दस संज्ञाएँ भी समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार, षोडश संज्ञाओं में ओघ को अंशतः और धर्म को पूर्णतः प्राणी के विवेकात्मक पक्ष से जोड़ा जा सकता है, शेष सभी चौदह संज्ञाएँ प्राणी के वासनात्मक पक्ष से ही संबंधित हैं।
I
1246
धर्मसंज्ञा को हम किस अर्थ में गृहीत करें, यह एक विचारणीय पक्ष है। 'धर्म' शब्द वस्तुतः स्वभाव का वाचक है, अतः प्राणी - स्वभाव को भी धर्म कहा जा सकता है । इस दृष्टि से धर्म भी जैविक मूलवृत्ति के रूप में स्थापित होता है, किन्तु जैन - आचार्यों ने धर्म को केवल प्राणी - स्वभाव के रूप में ही व्याख्यायित नहीं किया, अपितु वे उसे एक विवेकात्मक और सदाचारात्मक - पक्ष के रूप में भी प्रतिपादित करते हैं, इसलिए धर्म-संज्ञा प्राणी के विवेकात्मक पक्ष से संबंधित है ।
जैनदर्शन की यह मूलभूत मान्यता है कि जीव किसी भी अवस्था में हो, उसमें ज्ञान और दर्शन - पक्ष तो अंशतः सदैव उद्घाटित रहता ही है, अतः हम यह कह सकते हैं कि संज्ञाएँ किसी-न-किसी रूप में प्राणी के वासनात्मक और विवेकात्मक - दोनों पक्षों को अभिव्यंजित करती हैं।
जैनदर्शन में संज्ञा को वासनात्मक और विवेकात्मक - दोनों माना गया है। संज्ञा के विवेकात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हुए आचारांगसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ में कहा गया है - प्राणियों को इस बात का ज्ञान या विवेक ही नहीं होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ । आचारांगभाष्य में आचार्य महाप्रज्ञजी ने भी यहाँ 'सण्णा' शब्द का अर्थ संज्ञान या विवेक ही किया है, 1248 किन्तु जब संज्ञा ( सण्णा) का सम्बन्ध आहार, भय, मैथुन या परिग्रह की वृत्ति से जोड़ा जाता है, तो उसे एक जैव -वृत्ति या जीवन के वासनात्मक पक्ष के रूप में भी
1247
1246
1247
1248
वत्थु सहावो धम्मो - भाव संग्रह, गाथा 373
इहमेगेसि नो सण्णा भवइ, आचारांगसूत्र - 1/1/1
आचारांगभाष्य, आचार्य महाप्रज्ञ, जैनविश्वभारती संस्थान, लाडनूं, पृ. 16
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org