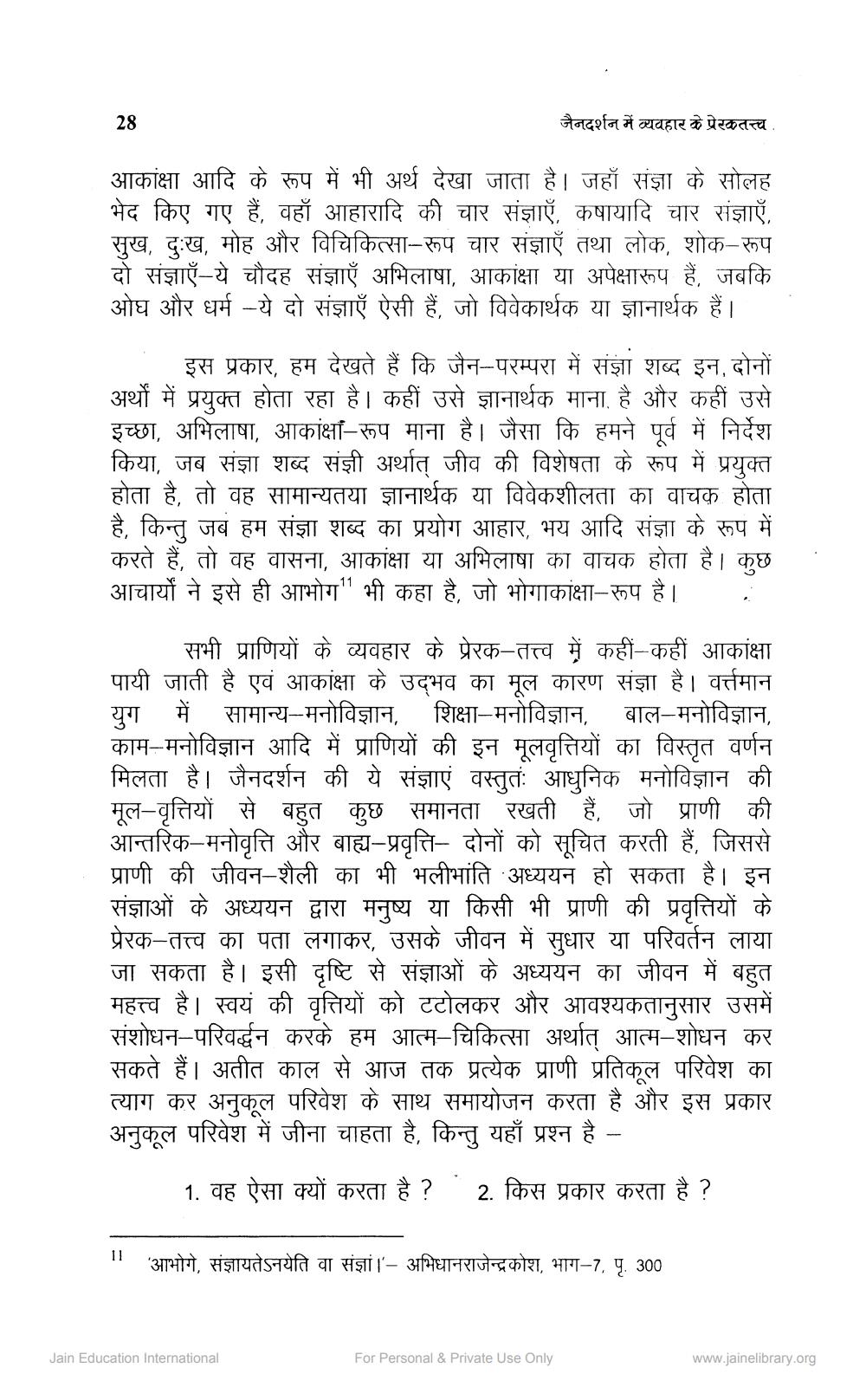________________
28
जैनदर्शन में व्यवहार के प्रेरकतत्त्व
आकांक्षा आदि के रूप में भी अर्थ देखा जाता है। जहाँ संज्ञा के सोलह भेद किए गए हैं, वहाँ आहारादि की चार संज्ञाएँ, कषायादि चार संज्ञाएँ, सुख, दुःख, मोह और विचिकित्सा-रूप चार संज्ञाएँ तथा लोक, शोक-रूप दो संज्ञाएँ-ये चौदह संज्ञाएँ अभिलाषा, आकांक्षा या अपेक्षारूप हैं, जबकि ओघ और धर्म -ये दो संज्ञाएँ ऐसी हैं, जो विवेकार्थक या ज्ञानार्थक हैं।
इस प्रकार, हम देखते हैं कि जैन-परम्परा में संज्ञा शब्द इन, दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। कहीं उसे ज्ञानार्थक माना है और कहीं उसे इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा-रूप माना है। जैसा कि हमने पूर्व में निर्देश किया, जब संज्ञा शब्द संज्ञी अर्थात् जीव की विशेषता के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह सामान्यतया ज्ञानार्थक या विवेकशीलता का वाचक होता है, किन्तु जब हम संज्ञा शब्द का प्रयोग आहार, भय आदि संज्ञा के रूप में करते हैं, तो वह वासना, आकांक्षा या अभिलाषा का वाचक होता है। कुछ आचार्यों ने इसे ही आभोग' भी कहा है, जो भोगाकांक्षा-रूप है। ,
सभी प्राणियों के व्यवहार के प्रेरक-तत्त्व में कहीं-कहीं आकांक्षा पायी जाती है एवं आकांक्षा के उद्भव का मूल कारण संज्ञा है। वर्तमान युग में सामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल-मनोविज्ञान, काम-मनोविज्ञान आदि में प्राणियों की इन मूलवृत्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जैनदर्शन की ये संज्ञाएं वस्तुतः आधुनिक मनोविज्ञान की मूल-वृत्तियों से बहुत कुछ समानता रखती हैं, जो प्राणी की आन्तरिक-मनोवृत्ति और बाह्य-प्रवृत्ति- दोनों को सूचित करती हैं, जिससे प्राणी की जीवन-शैली का भी भलीभांति अध्ययन हो सकता है। इन संज्ञाओं के अध्ययन द्वारा मनुष्य या किसी भी प्राणी की प्रवृत्तियों के प्रेरक-तत्त्व का पता लगाकर, उसके जीवन में सुधार या परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी दृष्टि से संज्ञाओं के अध्ययन का जीवन में बहुत महत्त्व है। स्वयं की वृत्तियों को टटोलकर और आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन-परिवर्द्धन करके हम आत्म–चिकित्सा अर्थात् आत्म–शोधन कर सकते हैं। अतीत काल से आज तक प्रत्येक प्राणी प्रतिकूल परिवेश का त्याग कर अनुकूल परिवेश के साथ समायोजन करता है और इस प्रकार अनुकूल परिवेश में जीना चाहता है, किन्तु यहाँ प्रश्न है -
1. वह ऐसा क्यों करता है ? 2. किस प्रकार करता है ?
। 'आभोगे, संज्ञायतेऽनयेति वा संज्ञां। - अभिधानराजेन्द्रकोश, भाग-7, पृ. 300
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org