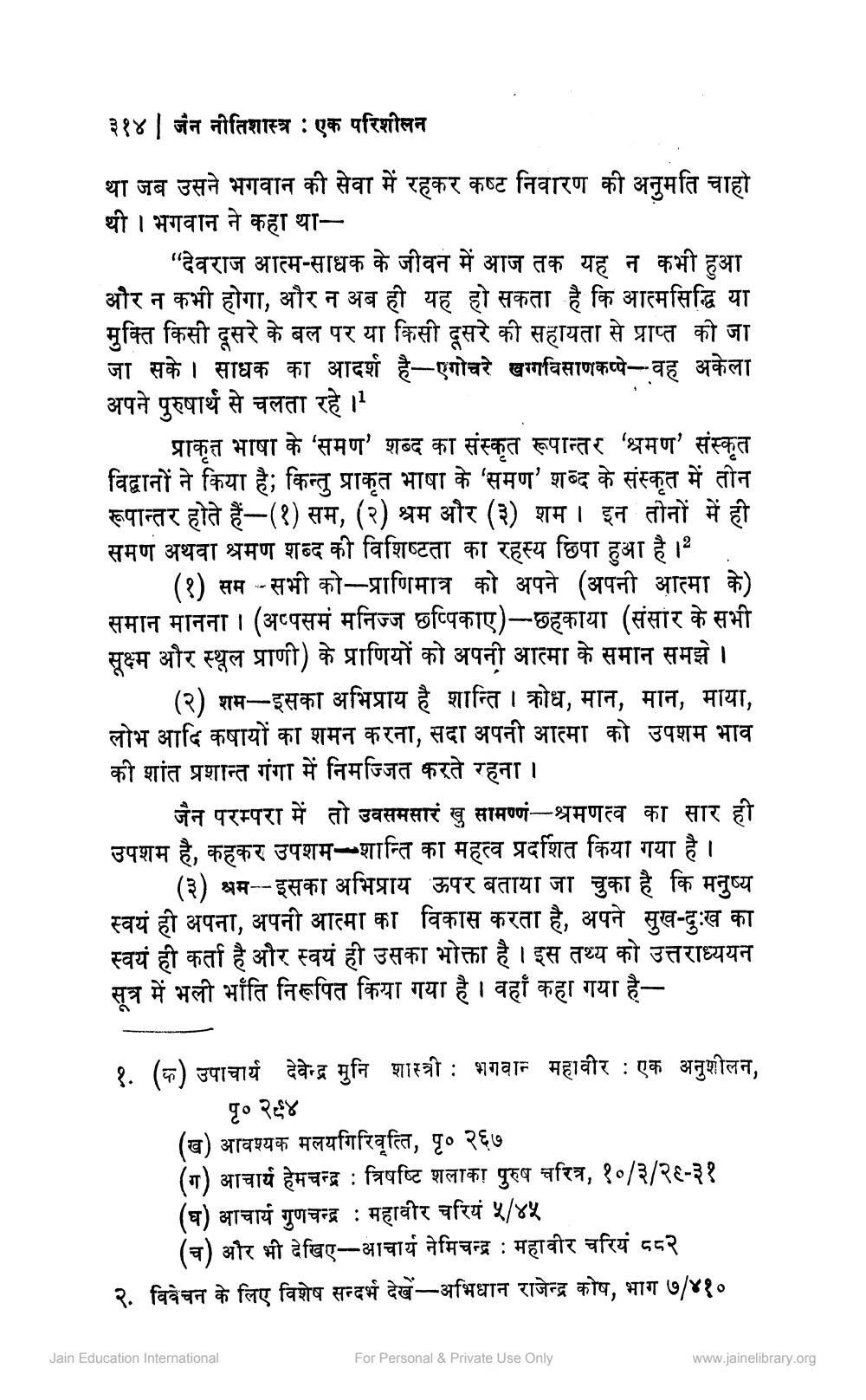________________
३१४ | जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन था जब उसने भगवान की सेवा में रहकर कष्ट निवारण की अनुमति चाहो थी। भगवान ने कहा था
___ "देवराज आत्म-साधक के जीवन में आज तक यह न कभी हुआ और न कभी होगा, और न अब ही यह हो सकता है कि आत्मसिद्धि या मुक्ति किसी दूसरे के बल पर या किसी दूसरे की सहायता से प्राप्त की जा जा सके। साधक का आदर्श है-एगोचरे खग्गविसाणकप्पे-वह अकेला अपने पुरुषार्थ से चलता रहे ।
प्राकृत भाषा के 'समण' शब्द का संस्कृत रूपान्तर 'श्रमण' संस्कृत विद्वानों ने किया है; किन्तु प्राकृत भाषा के 'समण' शब्द के संस्कृत में तीन रूपान्तर होते हैं-(१) सम, (२) श्रम और (३) शम । इन तीनों में ही समण अथवा श्रमण शब्द की विशिष्टता का रहस्य छिपा हुआ है।
(१) सम सभी को-प्राणिमात्र को अपने (अपनी आत्मा के) समान मानना । (अप्पसमं मनिज्ज छप्पिकाए)-छहकाया (संसार के सभी सूक्ष्म और स्थूल प्राणी) के प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझे।
(२) शम-इसका अभिप्राय है शान्ति । क्रोध, मान, मान, माया, लोभ आदि कषायों का शमन करना, सदा अपनी आत्मा को उपशम भाव की शांत प्रशान्त गंगा में निमज्जित करते रहना।
जैन परम्परा में तो उवसमसारं खु सामण्णं-श्रमणत्व का सार ही उपशम है, कहकर उपशम-शान्ति का महत्व प्रदर्शित किया गया है ।
(३) श्रम-- इसका अभिप्राय ऊपर बताया जा चुका है कि मनुष्य स्वयं ही अपना, अपनी आत्मा का विकास करता है, अपने सुख-दुःख का स्वयं ही कर्ता है और स्वयं ही उसका भोक्ता है । इस तथ्य को उत्तराध्ययन सत्र में भली भाँति निरूपित किया गया है । वहाँ कहा गया है
१. (क) उपाचार्य देवेन्द्र मुनि शास्त्री : भगवान महावीर : एक अनुशीलन,
पृ० २६४ (ख) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, पृ० २६७ (ग) आचार्य हेमचन्द्र : त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, १०/३/२६-३१ (घ) आचार्य गुणचन्द्र : महावीर चरियं ५/४५
(च) और भी देखिए-आचार्य नेमिचन्द्र : महावीर चरियं ८८२ २. विवेचन के लिए विशेष सन्दर्भ देखें-अभिधान राजेन्द्र कोष, भाग ७/४१०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org