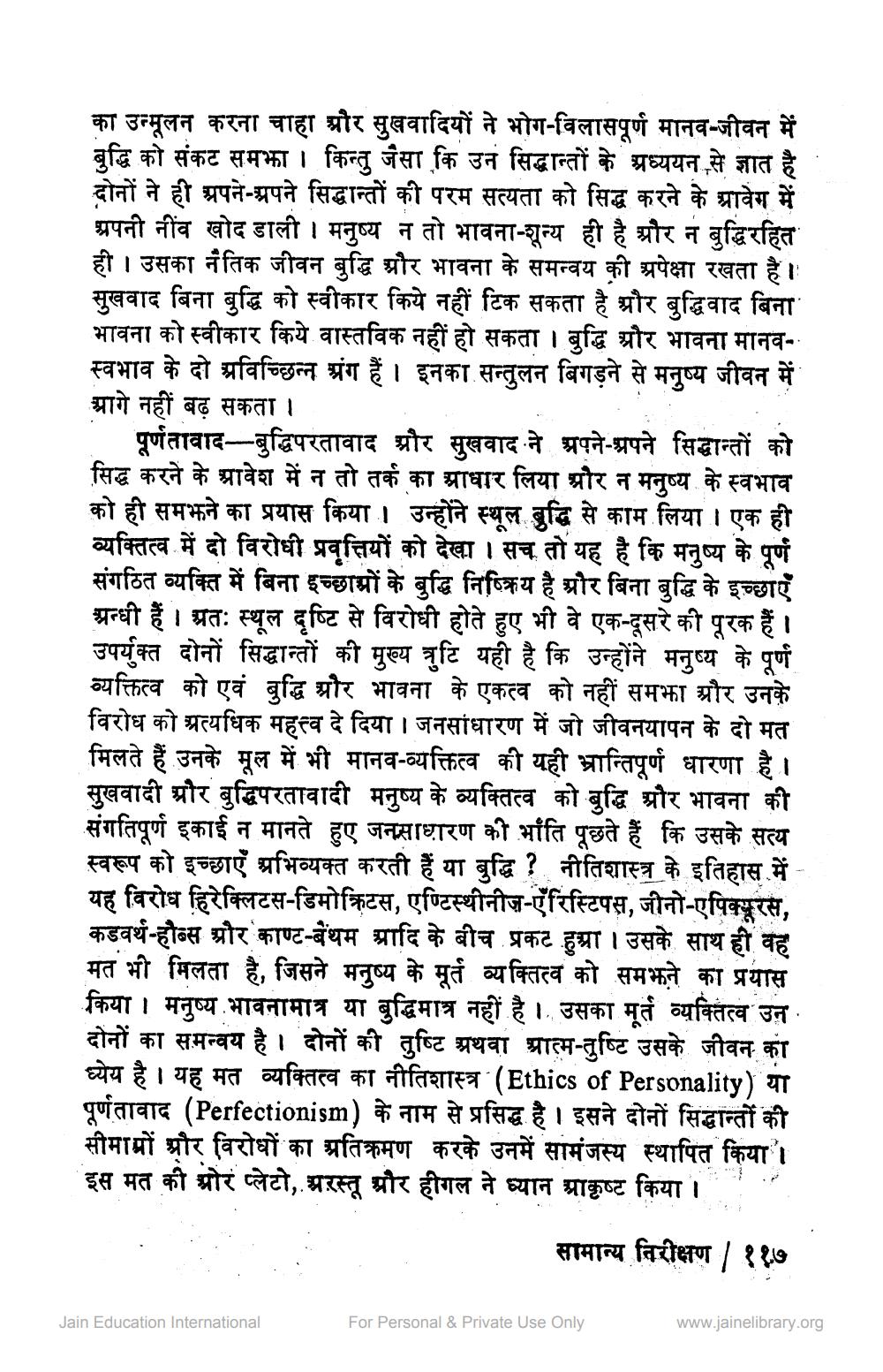________________
का उन्मूलन करना चाहा और सुखवादियों ने भोग-विलासपूर्ण मानव-जीवन में बुद्धि को संकट समझा। किन्तु जैसा कि उन सिद्धान्तों के अध्ययन से ज्ञात है दोनों ने ही अपने-अपने सिद्धान्तों की परम सत्यता को सिद्ध करने के आवेग में अपनी नींव खोद डाली। मनुष्य न तो भावना-शून्य ही है और न बुद्धिरहित ही । उसका नैतिक जीवन बुद्धि और भावना के समन्वय की अपेक्षा रखता है। सुखवाद बिना बुद्धि को स्वीकार किये नहीं टिक सकता है और बुद्धिवाद बिना भावना को स्वीकार किये वास्तविक नहीं हो सकता। बुद्धि और भावना मानवस्वभाव के दो अविच्छिन्न अंग हैं। इनका सन्तुलन बिगड़ने से मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता।
पूर्णतावाद-बुद्धिपरतावाद और सुखवाद ने अपने-अपने सिद्धान्तों को सिद्ध करने के आवेश में न तो तर्क का आधार लिया और न मनुष्य के स्वभाव को ही समझने का प्रयास किया। उन्होंने स्थूल बुद्धि से काम लिया। एक ही व्यक्तित्व में दो विरोधी प्रवृत्तियों को देखा । सच तो यह है कि मनुष्य के पूर्ण संगठित व्यक्ति में बिना इच्छाओं के बुद्धि निष्क्रिय है और बिना बुद्धि के इच्छाएं अन्धी हैं । अतः स्थूल दृष्टि से विरोधी होते हुए भी वे एक-दूसरे की पूरक हैं। उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों की मुख्य त्रुटि यही है कि उन्होंने मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व को एवं बुद्धि और भावना के एकत्व को नहीं समझा और उनके विरोध को अत्यधिक महत्त्व दे दिया। जनसांधारण में जो जीवनयापन के दो मत मिलते हैं उनके मूल में भी मानव-व्यक्तित्व की यही भ्रान्तिपूर्ण धारणा है। सुखवादी और बुद्धिपरतावादी मनुष्य के व्यक्तित्व को बुद्धि और भावना की संगतिपूर्ण इकाई न मानते हुए जनसाधारण की भांति पूछते हैं कि उसके सत्य स्वरूप को इच्छाएँ अभिव्यक्त करती हैं या बुद्धि ? नीतिशास्त्र के इतिहास मेंयह विरोध हिरेक्लिटस-डिमोक्रिटस, एण्टिस्थीनीज-ऍरिस्टिपस, जीनो-एपिक्यूरस, कडवर्थ-होब्स और काण्ट-बेंथम आदि के बीच प्रकट हुआ । उसके साथ ही वह मत भी मिलता है, जिसने मनुष्य के मूर्त व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। मनुष्य भावनामात्र या बुद्धिमात्र नहीं है। उसका मूर्त व्यक्तित्व उन . दोनों का समन्वय है। दोनों की तुष्टि अथवा आत्म-तुष्टि उसके जीवन का ध्येय है। यह मत व्यक्तित्व का नीतिशास्त्र (Ethics of Personality) या पूर्णतावाद (Perfectionism) के नाम से प्रसिद्ध है । इसने दोनों सिद्धान्तों की सीमामों और विरोधों का अतिक्रमण करके उनमें सामंजस्य स्थापित किया। इस मत की ओर प्लेटो, अरस्तू और हीगल ने ध्यान आकृष्ट किया।
सामान्य निरीक्षण | ११७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org