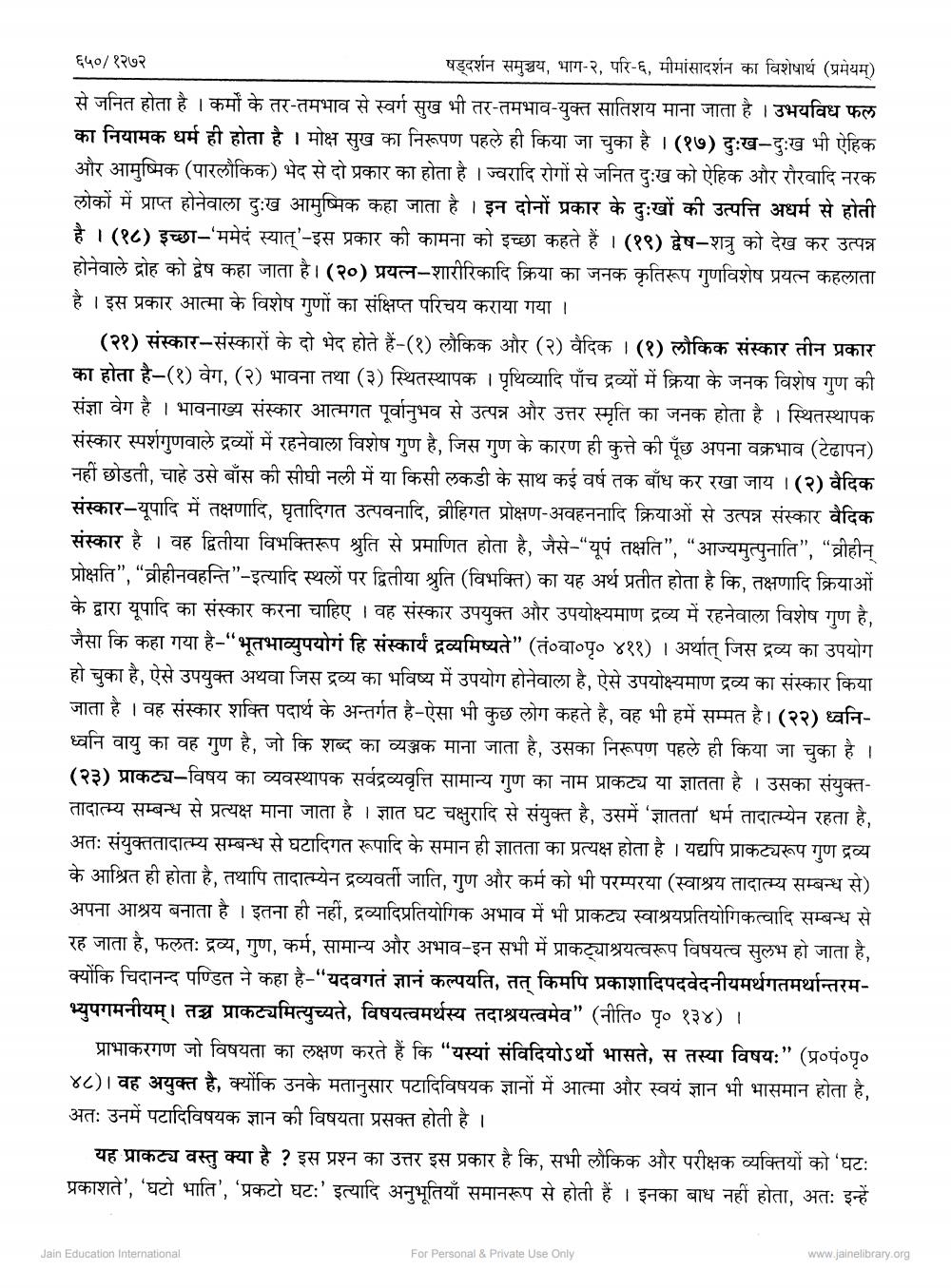________________
६५०/१२७२
षड्दर्शन समुच्चय, भाग-२, परि-६, मीमांसादर्शन का विशेषार्थ (प्रमेयम)
से जनित होता है । कर्मों के तर-तमभाव से स्वर्ग सुख भी तर-तमभाव-युक्त सातिशय माना जाता है । उभयविध फल का नियामक धर्म ही होता है । मोक्ष सख का निरूपण पहले ही किया जा चुका है । (१७) दःख-दुःख भी ऐहिक
और आमुष्मिक (पारलौकिक) भेद से दो प्रकार का होता है । ज्वरादि रोगों से जनित दुःख को ऐहिक और रौरवादि नरक लोकों में प्राप्त होनेवाला दु:ख आमुष्मिक कहा जाता है । इन दोनों प्रकार के दुःखों की उत्पत्ति अधर्म से होती है । (१८) इच्छा-'ममेदं स्यात्'-इस प्रकार की कामना को इच्छा कहते हैं । (१९) द्वेष-शत्रु को देख कर उत्पन्न होनेवाले द्रोह को द्वेष कहा जाता है। (२०) प्रयत्न-शारीरिकादि क्रिया का जनक कृतिरूप गुणविशेष प्रयत्न कहलाता है । इस प्रकार आत्मा के विशेष गुणों का संक्षिप्त परिचय कराया गया ।
(२१) संस्कार-संस्कारों के दो भेद होते हैं-(१) लौकिक और (२) वैदिक । (१) लौकिक संस्कार तीन प्रकार का होता है-(१) वेग, (२) भावना तथा (३) स्थितस्थापक । पृथिव्यादि पाँच द्रव्यों में क्रिया के जनक विशेष गुण की संज्ञा वेग है । भावनाख्य संस्कार आत्मगत पूर्वानुभव से उत्पन्न और उत्तर स्मृति का जनक होता है । स्थितस्थापक संस्कार स्पर्शगुणवाले द्रव्यों में रहनेवाला विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही कुत्ते की पूँछ अपना वक्रभाव (टेढापन) नहीं छोडती, चाहे उसे बाँस की सीघी नली में या किसी लकडी के साथ कई वर्ष तक बाँध कर रखा जाय । (२) वैदिक संस्कार-यूपादि में तक्षणादि, घृतादिगत उत्पवनादि, व्रीहिगत प्रोक्षण-अवहननादि क्रियाओं से उत्पन्न संस्कार वैदिक संस्कार है । वह द्वितीया विभक्तिरूप श्रुति से प्रमाणित होता है, जैसे-“यूपं तक्षति", “आज्यमुत्पुनाति", “व्रीहीन् प्रोक्षति", "व्रीहीनवहन्ति"-इत्यादि स्थलों पर द्वितीया श्रुति (विभक्ति) का यह अर्थ प्रतीत होता है कि, तक्षणादि क्रियाओं के द्वारा यूपादि का संस्कार करना चाहिए । वह संस्कार उपयुक्त और उपयोक्ष्यमाण द्रव्य में रहनेवाला विशेष गुण है, जैसा कि कहा गया है-"भूतभाव्युपयोगं हि संस्कार्यं द्रव्यमिष्यते" (तं०वा०पृ० ४११) । अर्थात् जिस द्रव्य का उपयोग हो चुका है, ऐसे उपयुक्त अथवा जिस द्रव्य का भविष्य में उपयोग होनेवाला है, ऐसे उपयोक्ष्यमाण द्रव्य का संस्कार किया जाता है । वह संस्कार शक्ति पदार्थ के अन्तर्गत है-ऐसा भी कुछ लोग कहते है, वह भी हमें सम्मत है। (२२) ध्वनिध्वनि वायु का वह गुण है, जो कि शब्द का व्यञ्जक माना जाता है, उसका निरूपण पहले ही किया जा चुका है । (२३) प्राकट्य-विषय का व्यवस्थापक सर्वद्रव्यवृत्ति सामान्य गुण का नाम प्राकट्य या ज्ञातता है । उसका संयुक्ततादात्म्य सम्बन्ध से प्रत्यक्ष माना जाता है । ज्ञात घट चक्षुरादि से संयुक्त है, उसमें 'ज्ञातता धर्म तादात्म्येन रहता है, अतः संयुक्ततादात्म्य सम्बन्ध से घटादिगत रूपादि के समान ही ज्ञातता का प्रत्यक्ष होता है । यद्यपि प्राकट्यरूप गुण द्रव्य के आश्रित ही होता है, तथापि तादात्म्येन द्रव्यवर्ती जाति, गुण और कर्म को भी परम्परया (स्वाश्रय तादात्म्य सम्बन्ध से) अपना आश्रय बनाता है । इतना ही नहीं, द्रव्यादिप्रतियोगिक अभाव में भी प्राकट्य स्वाश्रयप्रतियोगिकत्वादि सम्बन्ध से रह जाता है, फलतः द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव-इन सभी में प्राकट्याश्रयत्वरूप विषयत्व सुलभ हो जाता है, क्योंकि चिदानन्द पण्डित ने कहा है-"यदवगतं ज्ञानं कल्पयति, तत् किमपि प्रकाशादिपदवेदनीयमर्थगतमर्थान्तरमभ्युपगमनीयम्। तञ्च प्राकट्यमित्युच्यते, विषयत्वमर्थस्य तदाश्रयत्वमेव" (नीति० पृ० १३४) ।
प्राभाकरगण जो विषयता का लक्षण करते हैं कि “यस्यां संविदियोऽर्थो भासते, स तस्या विषयः" (प्र०पं०पृ० ४८)। वह अयुक्त है, क्योंकि उनके मतानुसार पटादिविषयक ज्ञानों में आत्मा और स्वयं ज्ञान भी भासमान होता है, अतः उनमें पटादिविषयक ज्ञान की विषयता प्रसक्त होती है ।
यह प्राकट्य वस्तु क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि, सभी लौकिक और परीक्षक व्यक्तियों को 'घट: प्रकाशते', 'घटो भाति', 'प्रकटो घटः' इत्यादि अनुभूतियाँ समानरूप से होती हैं । इनका बाध नहीं होता, अतः इन्हें
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org