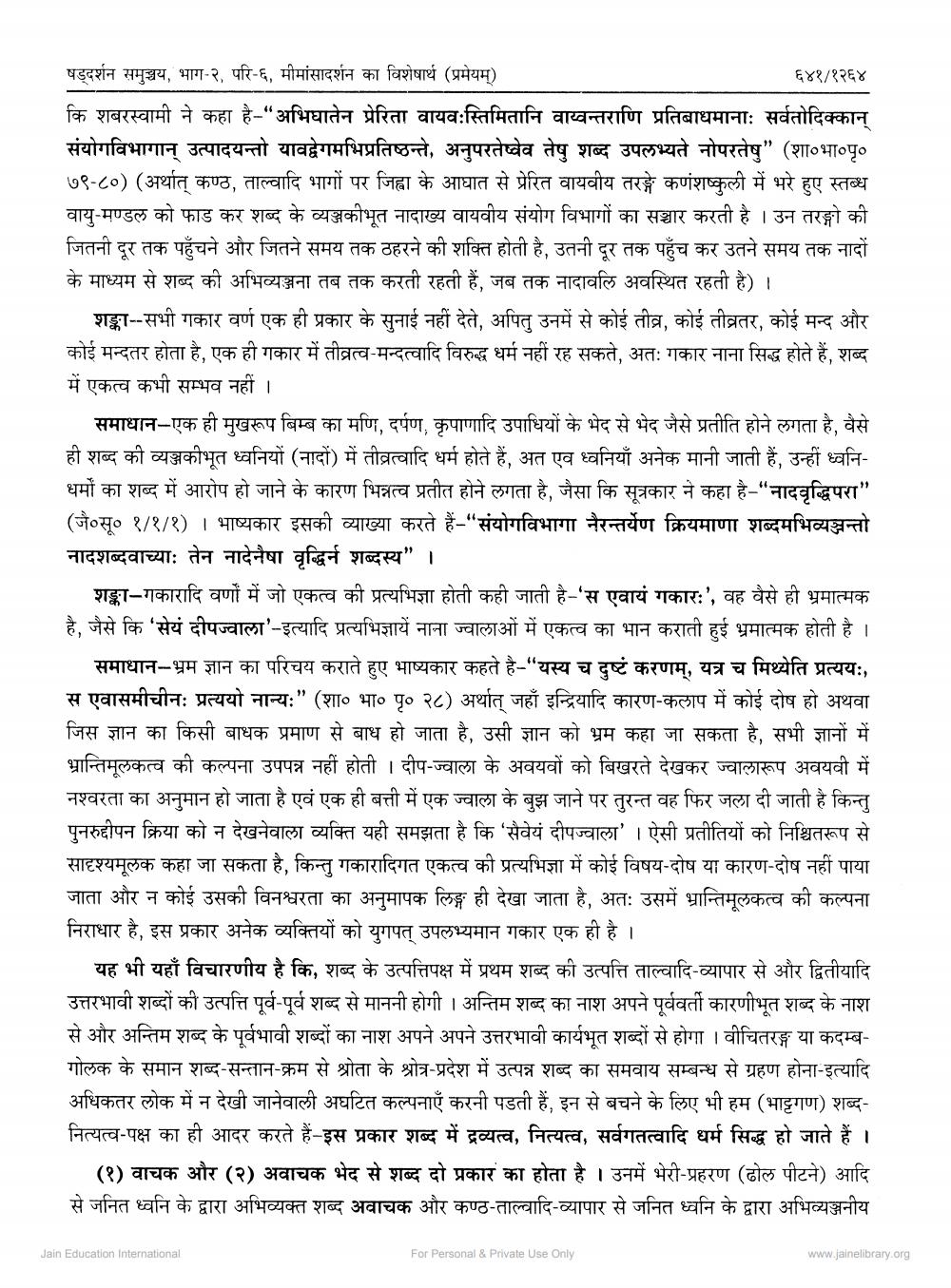________________
षड्दर्शन समुच्चय, भाग-२, परि ६, मीमांसादर्शन का विशेषार्थ (प्रमेयम्)
६४१ / १२६४
कि शबरस्वामी ने कहा है- " अभिघातेन प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाय्वन्तराणि प्रतिबाधमानाः सर्वतोदिक्क संयोगविभागान् उत्पादयन्तो यावद्वेगमभिप्रतिष्ठन्ते, अनुपरतेष्वेव तेषु शब्द उपलभ्यते नोपरतेषु" (शा०भा०पृ० ७९-८०) (अर्थात् कण्ठ, ताल्वादि भागों पर जिह्वा के आघात से प्रेरित वायवीय तरङ्गे कणशष्कुली में भरे हुए वायु-मण्डल को फाड कर शब्द के व्यञ्जकीभूत नादाख्य वायवीय संयोग विभागों का सञ्चार करती है । उन तरङ्गो की जितनी दूर तक पहुँचने और जितने समय तक ठहरने की शक्ति होती है, उतनी दूर तक पहुँच कर उतने समय तक नादों के माध्यम से शब्द की अभिव्यञ्जना तब तक करती रहती हैं, जब तक नादावलि अवस्थित रहती है ) ।
शङ्का--सभी गकार वर्ण एक ही प्रकार के सुनाई नहीं देते, अपितु उनमें से कोई तीव्र, कोई तीव्रतर, कोई मन्द और कोई मन्दतर होता है, एक ही गकार में तीव्रत्व-मन्दत्वादि विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते, अतः गकार नाना सिद्ध होते हैं, शब्द में एकत्व कभी सम्भव नहीं ।
समाधान - एक ही मुखरूप बिम्ब का मणि, दर्पण, कृपाणादि उपाधियों के भेद से भेद जैसे प्रतीति होने लगता है, वैसे ही शब्द की व्यञ्जकीभूत ध्वनियों (नादों) में तीव्रत्वादि धर्म होते हैं, अत एव ध्वनियाँ अनेक मानी जाती हैं, उन्हीं ध्वनिधर्मों का शब्द में आरोप हो जाने के कारण भिन्नत्व प्रतीत होने लगता है, जैसा कि सूत्रकार ने कहा है- "नादवृद्धिपरा" (जै०सू० १/१ / १) । भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं- “संयोगविभागा नैरन्तर्येण क्रियमाणा शब्दमभिव्यञ्जन्तो नादशब्दवाच्याः तेन नादेनैषा वृद्धिर्न शब्दस्य " I
शङ्का - गकारादि वर्णों में जो एकत्व की प्रत्यभिज्ञा होती कही जाती है- 'स एवायं गकारः', वह वैसे ही भ्रमात्मक है, जैसे कि 'सेयं दीपज्वाला' - इत्यादि प्रत्यभिज्ञायें नाना ज्वालाओं में एकत्व का भान कराती हुई भ्रमात्मक होती है ।
समाधान-भ्रम ज्ञान का परिचय कराते हुए भाष्यकार कहते है- “यस्य च दुष्टं करणम्, यत्र च मिथ्येति प्रत्यय:, स एवासमीचीनः प्रत्ययो नान्यः " ( शा० भा० पृ० २८) अर्थात् जहाँ इन्द्रियादि कारण-कलाप में कोई दोष हो अथवा जिस ज्ञान का किसी बाधक प्रमाण से बाध हो जाता है, उसी ज्ञान को भ्रम कहा जा सकता है, सभी ज्ञानों में भ्रान्तिमूलकत्व की कल्पना उपपन्न नहीं होती । दीप ज्वाला के अवयवों को बिखरते देखकर ज्वालारूप अवयवी में नश्वरता का अनुमान हो जाता है एवं एक ही बत्ती में एक ज्वाला के बुझ जाने पर तुरन्त वह फिर जला दी जाती है किन्तु पुनरुद्दीपन क्रिया को न देखनेवाला व्यक्ति यही समझता है कि 'सैवेयं दीपज्वाला' । ऐसी प्रतीतियों को निश्चितरूप से सादृश्यमूलक कहा जा सकता है, किन्तु गकारादिगत एकत्व की प्रत्यभिज्ञा में कोई विषय - दोष या कारण-दोष नहीं पाया जाता और न कोई उसकी विनश्वरता का अनुमापक लिङ्ग ही देखा जाता है, अतः उसमें भ्रान्तिमूलकत्व की कल्पना निराधार है, इस प्रकार अनेक व्यक्तियों को युगपत् उपलभ्यमान गकार एक ही है ।
यह भी यहाँ विचारणीय है कि, शब्द के उत्पत्तिपक्ष में प्रथम शब्द की उत्पत्ति ताल्वादि व्यापार से और द्वितीयादि उत्तरभावी शब्दों की उत्पत्ति पूर्व- पूर्व शब्द से माननी होगी । अन्तिम शब्द का नाश अपने पूर्ववर्ती कारणीभूत शब्द के नाश और अन्तिम शब्द के पूर्वभावी शब्दों का नाश अपने अपने उत्तरभावी कार्यभूत शब्दों से होगा । वीचितरङ्ग या कदम्बगोलक के समान शब्द - सन्तान -क्रम से श्रोता के श्रोत्र- प्रदेश में उत्पन्न शब्द का समवाय सम्बन्ध से ग्रहण होना- इत्यादि अधिकतर लोक में न देखी जानेवाली अघटित कल्पनाएँ करनी पडती हैं, इन से बचने के लिए भी हम (भाट्टगण) शब्दनित्यत्व-पक्ष का ही आदर करते हैं- इस प्रकार शब्द में द्रव्यत्व, नित्यत्व, सर्वगतत्वादि धर्म सिद्ध हो जाते
1
(१) वाचक और (२) अवाचक भेद से शब्द दो प्रकार का होता है । उनमें भेरी-प्रहरण ( ढोल पीटने) आदि से जनित ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त शब्द अवाचक और कण्ठ-ताल्वादि-व्यापार से जनित ध्वनि के द्वारा अभिव्यञ्जनीय
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org