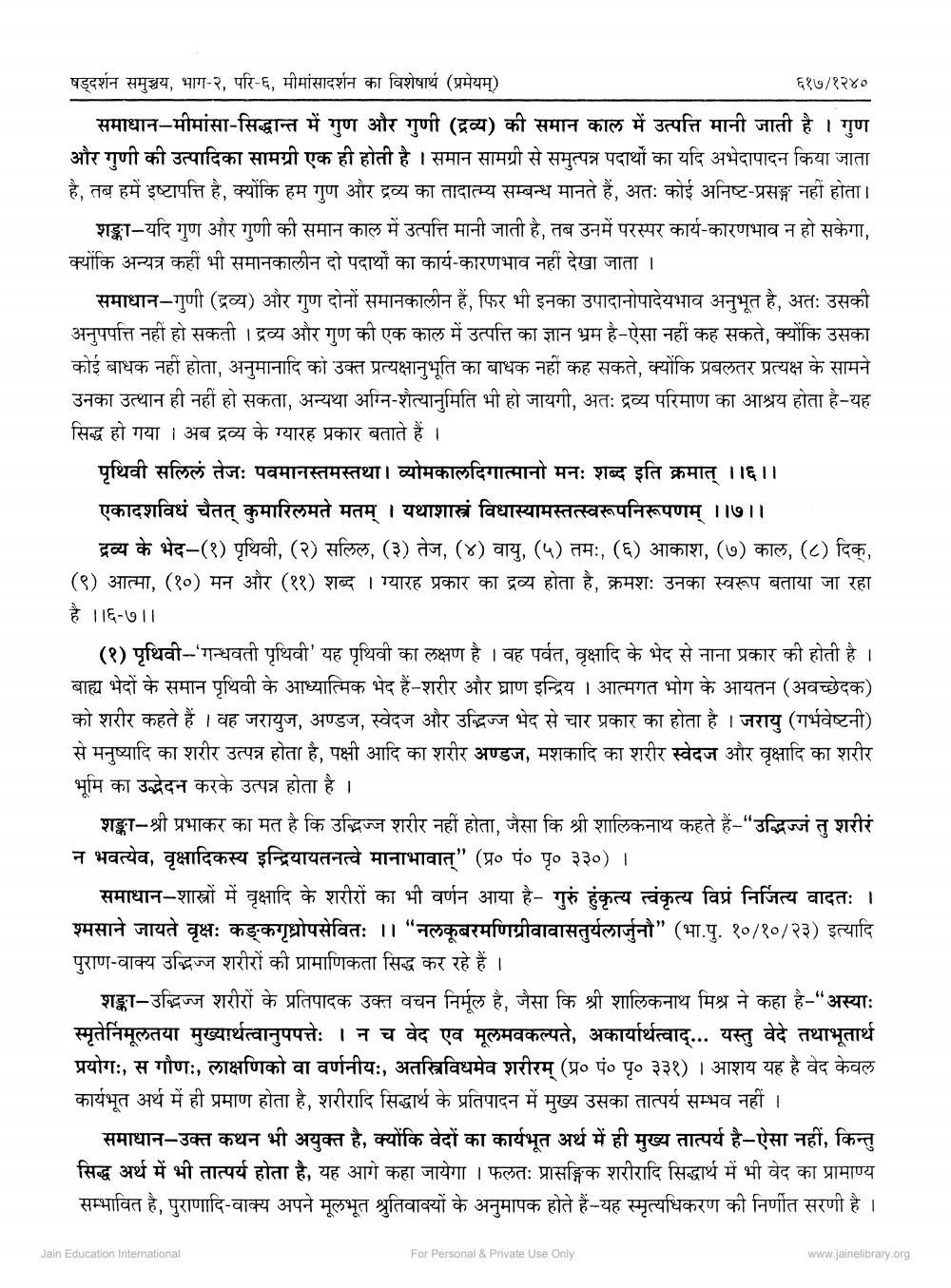________________
षड्दर्शन समुच्चय, भाग-२, परि-६, मीमांसादर्शन का विशेषार्थ (प्रमेयम्)
६१७/१२४० समाधान-मीमांसा-सिद्धान्त में गुण और गुणी (द्रव्य) की समान काल में उत्पत्ति मानी जाती है । गुण और गुणी की उत्पादिका सामग्री एक ही होती है । समान सामग्री से समुत्पन्न पदार्थों का यदि अभेदापादन किया जाता है, तब हमें इष्टापत्ति है, क्योंकि हम गुण और द्रव्य का तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं, अतः कोई अनिष्ट-प्रसङ्ग नहीं होता।
शङ्का-यदि गुण और गुणी की समान काल में उत्पत्ति मानी जाती है, तब उनमें परस्पर कार्य-कारणभाव न हो सकेगा, क्योंकि अन्यत्र कहीं भी समानकालीन दो पदार्थों का कार्य-कारणभाव नहीं देखा जाता ।
समाधान-गुणी (द्रव्य) और गुण दोनों समानकालीन हैं, फिर भी इनका उपादानोपादेयभाव अनुभूत है, अत: उसकी अनुपपत्ति नहीं हो सकती । द्रव्य और गुण की एक काल में उत्पत्ति का ज्ञान भ्रम है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई बाधक नहीं होता, अनुमानादि को उक्त प्रत्यक्षानुभूति का बाधक नहीं कह सकते, क्योंकि प्रबलतर प्रत्यक्ष के सामने उनका उत्थान ही नहीं हो सकता, अन्यथा अग्नि-शैत्यानुमिति भी हो जायगी, अतः द्रव्य परिमाण का आश्रय होता है-यह सिद्ध हो गया । अब द्रव्य के ग्यारह प्रकार बताते हैं ।
पृथिवी सलिलं तेजः पवमानस्तमस्तथा। व्योमकालदिगात्मानो मनः शब्द इति क्रमात् ।।६।। एकादशविधं चैतत् कुमारिलमते मतम् । यथाशास्त्रं विधास्यामस्तत्स्वरूपनिरूपणम् ।।७।।
द्रव्य के भेद-(१) पृथिवी, (२) सलिल, (३) तेज, (४) वायु, (५) तमः, (६) आकाश, (७) काल, (८) दिक्, (९) आत्मा, (१०) मन और (११) शब्द । ग्यारह प्रकार का द्रव्य होता है, क्रमशः उनका स्वरूप बताया जा रहा है ।।६-७।।
(१) पृथिवी-'गन्धवती पृथिवी' यह पृथिवी का लक्षण है । वह पर्वत, वृक्षादि के भेद से नाना प्रकार की होती है । बाह्य भेदों के समान पृथिवी के आध्यात्मिक भेद हैं-शरीर और घ्राण इन्द्रिय । आत्मगत भोग के आयतन (अवच्छेदक) को शरीर कहते हैं । वह जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज भेद से चार प्रकार का होता है । जरायु (गर्भवेष्टनी) से मनुष्यादि का शरीर उत्पन्न होता है, पक्षी आदि का शरीर अण्डज, मशकादि का शरीर स्वेदज और वृक्षादि का शरीर भूमि का उद्भेदन करके उत्पन्न होता है ।
शङ्का-श्री प्रभाकर का मत है कि उद्भिज्ज शरीर नहीं होता, जैसा कि श्री शालिकनाथ कहते हैं-"उद्भिज्जं तु शरीरं न भवत्येव, वृक्षादिकस्य इन्द्रियायतनत्वे मानाभावात्" (प्र० पं० पृ० ३३०) ।
समाधान-शास्त्रों में वृक्षादि के शरीरों का भी वर्णन आया है- गुरुं हुंकृत्य त्वंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः । श्मसाने जायते वृक्षः कङ्कगृध्रोपसेवितः ।। "नलकूबरमणिग्रीवावासतुर्यलार्जुनौ" (भा.पु. १०/१०/२३) इत्यादि पुराण-वाक्य उद्भिज्ज शरीरों की प्रामाणिकता सिद्ध कर रहे हैं ।
शङ्का-उद्भिज्ज शरीरों के प्रतिपादक उक्त वचन निर्मूल है, जैसा कि श्री शालिकनाथ मिश्र ने कहा है-"अस्याः स्मृतेर्निमूलतया मुख्यार्थत्वानुपपत्तेः । न च वेद एव मूलमवकल्पते, अकार्यार्थत्वाद्... यस्तु वेदे तथाभूतार्थ प्रयोगः, स गौणः, लाक्षणिको वा वर्णनीयः, अतस्त्रिविधमेव शरीरम् (प्र० पं० पृ० ३३१) । आशय यह है वेद केवल कार्यभूत अर्थ में ही प्रमाण होता है, शरीरादि सिद्धार्थ के प्रतिपादन में मुख्य उसका तात्पर्य सम्भव नहीं ।
समाधान-उक्त कथन भी अयुक्त है, क्योंकि वेदों का कार्यभूत अर्थ में ही मुख्य तात्पर्य है-ऐसा नहीं, किन्तु सिद्ध अर्थ में भी तात्पर्य होता है, यह आगे कहा जायेगा । फलतः प्रासङ्गिक शरीरादि सिद्धार्थ में भी वेद का प्रामाण्य सम्भावित है, पुराणादि-वाक्य अपने मूलभूत श्रुतिवाक्यों के अनुमापक होते हैं-यह स्मृत्यधिकरण की निर्णीत सरणी है ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org