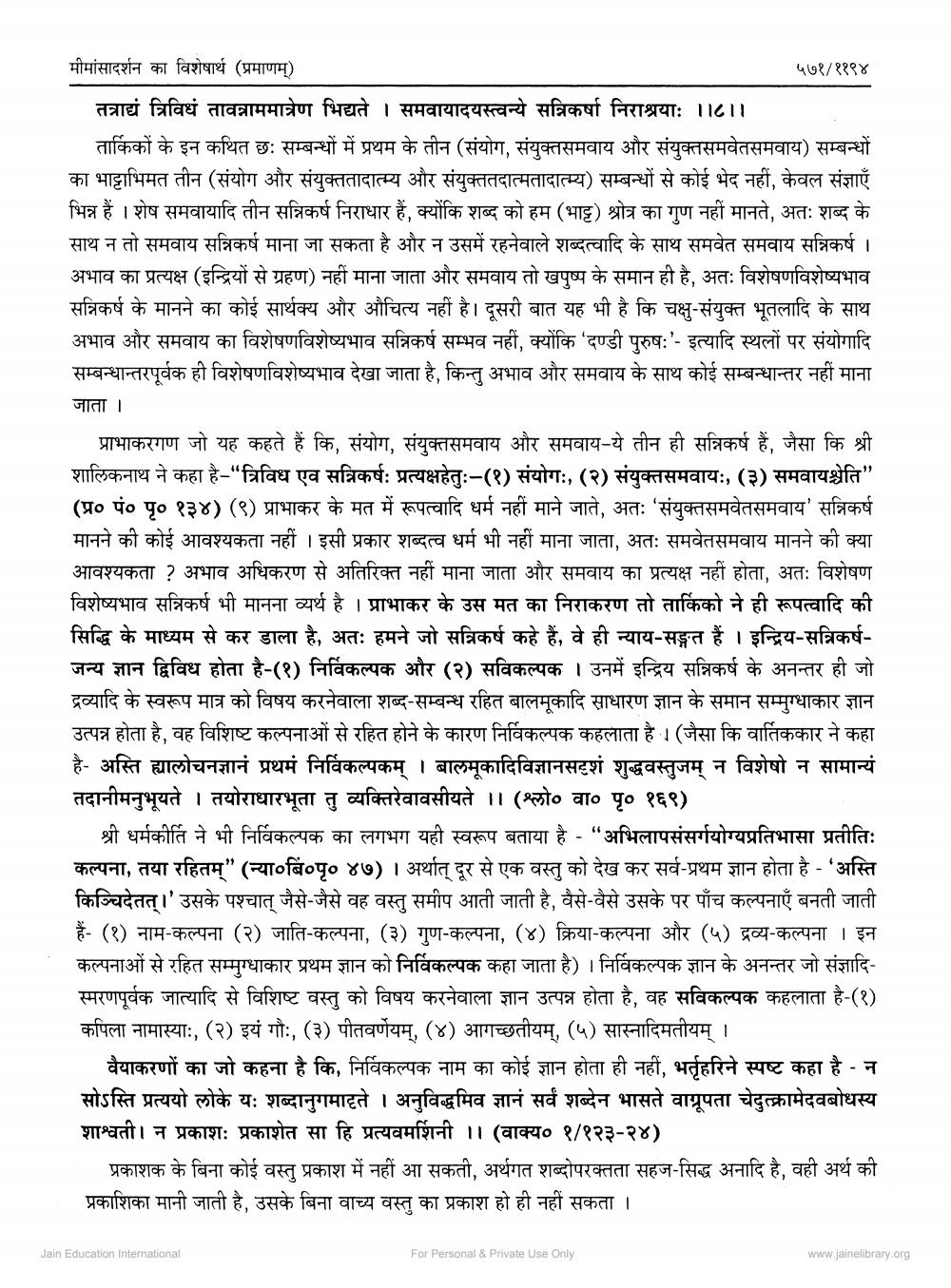________________
मीमांसादर्शन का विशेषार्थ (प्रमाणम्)
तत्राद्यं त्रिविधं तावन्नाममात्रेण भिद्यते । समवायादयस्त्वन्ये सन्निकर्षा निराश्रयाः ।।८ ॥
तार्किकों के इन कथित छः सम्बन्धों में प्रथम के तीन ( संयोग, संयुक्तसमवाय और संयुक्तसमवेतसमवाय) सम्बन्धों का भाट्टाभिमत तीन (संयोग और संयुक्ततादात्म्य और संयुक्ततदात्मतादात्म्य) सम्बन्धों से कोई भेद नहीं, केवल संज्ञाएँ भिन्न हैं । शेष समवायादि तीन सन्निकर्ष निराधार हैं, क्योंकि शब्द को हम (भाट्ट) श्रोत्र का गुण नहीं मानते, अतः शब्द के साथ न तो समवाय सन्निकर्ष माना जा सकता है और न उसमें रहनेवाले शब्दत्वादि के साथ समवेत समवाय सन्निकर्ष । अभाव का प्रत्यक्ष (इन्द्रियों से ग्रहण) नहीं माना जाता और समवाय तो खपुष्प के समान ही है, अतः विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष के मानने का कोई सार्थक्य और औचित्य नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि चक्षु संयुक्त भूतलादि के साथ अभाव और समवाय का विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष सम्भव नहीं, क्योंकि 'दण्डी पुरुष:'- इत्यादि स्थलों पर संयोगादि सम्बन्धान्तरपूर्वक ही विशेषणविशेष्यभाव देखा जाता है, किन्तु अभाव और समवाय के साथ कोई सम्बन्धान्तर नहीं माना
जाता ।
प्राभाकरगण जो यह कहते हैं कि, संयोग, संयुक्तसमवाय और समवाय- ये तीन ही सन्निकर्ष हैं, जैसा कि श्री शालिकनाथ ने कहा है- "त्रिविध एव सन्निकर्ष: प्रत्यक्षहेतुः - (१) संयोग:, (२) संयुक्तसमवायः, (३) समवायश्चेति" (प्र० पं० पृ० १३४) (९) प्राभाकर के मत में रूपत्वादि धर्म नहीं माने जाते, अतः 'संयुक्तसमवेतसमवाय' सन्निकर्ष मानने की कोई आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार शब्दत्व धर्म भी नहीं माना जाता, अतः समवेतसमवाय मानने की क्या आवश्यकता ? अभाव अधिकरण से अतिरिक्त नहीं माना जाता और समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः विशेषण विशेष्यभाव सन्निकर्ष भी मानना व्यर्थ है । प्राभाकर के उस मत का निराकरण तो तार्किको ने ही रूपत्वादि की सिद्धि के माध्यम से कर डाला है, अतः हमने जो सन्निकर्ष कहे हैं, वे ही न्याय - सङ्गत हैं । इन्द्रिय- सन्निकर्षजन्य ज्ञान द्विविध होता है- (१) निर्विकल्पक और ( २) सविकल्पक । उनमें इन्द्रिय सन्निकर्ष के अनन्तर ही जो द्रव्यादि के स्वरूप मात्र को विषय करनेवाला शब्द- सम्बन्ध रहित बालमूकादि साधारण ज्ञान के समान सम्मुग्धाकार ज्ञान उत्पन्न होता है, वह विशिष्ट कल्पनाओं से रहित होने के कारण निर्विकल्पक कहलाता है । (जैसा कि वार्तिककार ने कहा है- अस्ति ह्यालोचनज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् । बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम् न विशेषो न सामान्यं तदानीमनुभूयते । तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते ।। (श्लो० वा० पृ० १६९)
५७१ / ११९४
श्री धर्मकीर्ति ने भी निर्विकल्पक का लगभग यही स्वरूप बताया है- “अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना, तया रहितम्” (न्या०बिं० पृ० ४७) । अर्थात् दूर से एक वस्तु को देख कर सर्व प्रथम ज्ञान होता है - 'अस्ति किञ्चिदेतत्।' उसके पश्चात् जैसे-जैसे वह वस्तु समीप आती जाती है, वैसे-वैसे उसके पर पाँच कल्पनाएँ बनती जाती हैं- (१) नाम - कल्पना (२) जाति- कल्पना, (३) गुण-कल्पना, (४) क्रिया- कल्पना और (५) द्रव्य- कल्पना । इन कल्पनाओं से रहित सम्मुग्धाकार प्रथम ज्ञान को निर्विकल्पक कहा जाता है) । निर्विकल्पक ज्ञान के अनन्तर जो संज्ञादिस्मरणपूर्वक जात्यादि से विशिष्ट वस्तु को विषय करनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सविकल्पक कहलाता है- (१) कपिला नामास्याः, (२) इयं गौः, (३) पीतवर्णेयम्, (४) आगच्छतीयम्, (५) सास्नादिमतीयम् ।
वैयाकरणों का जो कहना है कि, निर्विकल्पक नाम का कोई ज्ञान होता ही नहीं, भर्तृहरिने स्पष्ट कहा है - न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते वाग्रूपता चेदुत्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती । न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ।। ( वाक्य ० १ / १२३-२४)
प्रकाशक के बिना कोई वस्तु प्रकाश में नहीं आ सकती, अर्थगत शब्दोपरक्तता सहज-सिद्ध अनादि है, वही अर्थ की प्रकाशिका मानी जाती है, उसके बिना वाच्य वस्तु का प्रकाश हो ही नहीं सकता ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org