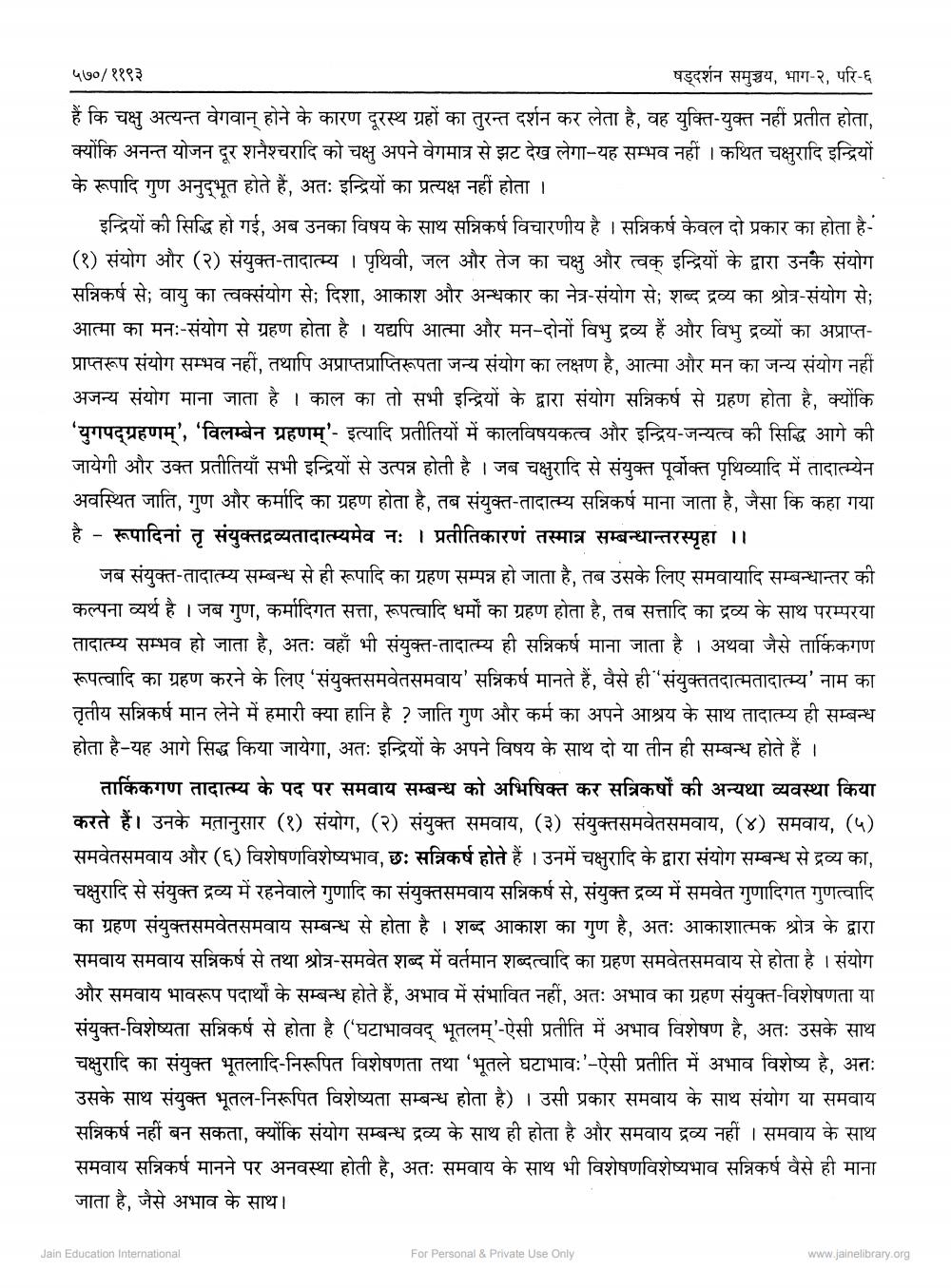________________
५७०/ ११९३
षड्दर्शन समुच्चय, भाग-२, परि-६ हैं कि चक्षु अत्यन्त वेगवान् होने के कारण दूरस्थ ग्रहों का तुरन्त दर्शन कर लेता है, वह युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि अनन्त योजन दूर शनैश्चरादि को चक्षु अपने वेगमात्र से झट देख लेगा-यह सम्भव नहीं । कथित चक्षुरादि इन्द्रियों के रूपादि गुण अनुद्भूत होते हैं, अतः इन्द्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता ।
इन्द्रियों की सिद्धि हो गई, अब उनका विषय के साथ सन्निकर्ष विचारणीय है । सन्निकर्ष केवल दो प्रकार का होता है(१) संयोग और (२) संयुक्त-तादात्म्य । पृथिवी, जल और तेज का चक्षु और त्वक् इन्द्रियों के द्वारा उनके संयोग सन्निकर्ष से; वायु का त्वक्संयोग से; दिशा, आकाश और अन्धकार का नेत्र-संयोग से; शब्द द्रव्य का श्रोत्र-संयोग से; आत्मा का मनः-संयोग से ग्रहण होता है । यद्यपि आत्मा और मन-दोनों विभु द्रव्य हैं और विभु द्रव्यों का अप्राप्तप्राप्तरूप संयोग सम्भव नहीं, तथापि अप्राप्तप्राप्तिरूपता जन्य संयोग का लक्षण है, आत्मा और मन का जन्य संयोग नहीं अजन्य संयोग माना जाता है । काल का तो सभी इन्द्रियों के द्वारा संयोग सन्निकर्ष से ग्रहण होता है, क्योंकि 'युगपद्ग्रहणम्', 'विलम्बेन ग्रहणम्'- इत्यादि प्रतीतियों में कालविषयकत्व और इन्द्रिय-जन्यत्व की सिद्धि आगे की जायेगी और उक्त प्रतीतियाँ सभी इन्द्रियों से उत्पन्न होती है । जब चक्षुरादि से संयुक्त पूर्वोक्त पृथिव्यादि में तादात्म्येन अवस्थित जाति, गुण और कर्मादि का ग्रहण होता है, तब संयुक्त-तादात्म्य सन्निकर्ष माना जाता है, जैसा कि कहा गया है - रूपादिनां तृ संयुक्तद्रव्यतादात्म्यमेव नः । प्रतीतिकारणं तस्मान्न सम्बन्धान्तरस्पृहा ।।
जब संयुक्त-तादात्म्य सम्बन्ध से ही रूपादि का ग्रहण सम्पन्न हो जाता है, तब उसके लिए समवायादि सम्बन्धान्तर की कल्पना व्यर्थ है । जब गुण, कर्मादिगत सत्ता, रूपत्वादि धर्मों का ग्रहण होता है, तब सत्तादि का द्रव्य के साथ परम्परया तादात्म्य सम्भव हो जाता है, अतः वहाँ भी संयुक्त-तादात्म्य ही सन्निकर्ष माना जाता है । अथवा जैसे तार्किकगण रूपत्वादि का ग्रहण करने के लिए संयुक्तसमवेतसमवाय' सन्निकर्ष मानते हैं, वैसे ही संयुक्ततदात्मतादात्म्य' नाम का तृतीय सन्निकर्ष मान लेने में हमारी क्या हानि है ? जाति गुण और कर्म का अपने आश्रय के साथ तादात्म्य ही सम्बन्ध होता है-यह आगे सिद्ध किया जायेगा, अतः इन्द्रियों के अपने विषय के साथ दो या तीन ही सम्बन्ध होते हैं ।
तार्किकगण तादात्म्य के पद पर समवाय सम्बन्ध को अभिषिक्त कर सत्रिकर्षों की अन्यथा व्यवस्था किया करते हैं। उनके मतानुसार (१) संयोग, (२) संयुक्त समवाय, (३) संयुक्तसमवेतसमवाय, (४) समवाय, (५) समवेतसमवाय और (६) विशेषणविशेष्यभाव, छः सन्निकर्ष होते हैं । उनमें चक्षुरादि के द्वारा संयोग सम्बन्ध से द्रव्य का, चक्षुरादि से संयुक्त द्रव्य में रहनेवाले गुणादि का संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष से, संयुक्त द्रव्य में समवेत गुणादिगत गुणत्वादि का ग्रहण संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध से होता है । शब्द आकाश का गुण है, अतः आकाशात्मक श्रोत्र के द्वारा समवाय समवाय सन्निकर्ष से तथा श्रोत्र-समवेत शब्द में वर्तमान शब्दत्वादि का ग्रहण समवेतसमवाय से होता है । संयोग
और समवाय भावरूप पदार्थों के सम्बन्ध होते हैं, अभाव में संभावित नहीं, अतः अभाव का ग्रहण संयुक्त-विशेषणता या संयुक्त-विशेष्यता सन्निकर्ष से होता है ('घटाभाववद् भूतलम्'-ऐसी प्रतीति में अभाव विशेषण है, अतः उसके साथ चक्षुरादि का संयुक्त भूतलादि-निरूपित विशेषणता तथा 'भूतले घटाभावः'-ऐसी प्रतीति में अभाव विशेष्य है, अतः उसके साथ संयुक्त भूतल-निरूपित विशेष्यता सम्बन्ध होता है) । उसी प्रकार समवाय के साथ संयोग या समवाय सन्निकर्ष नहीं बन सकता, क्योंकि संयोग सम्बन्ध द्रव्य के साथ ही होता है और समवाय द्रव्य नहीं । समवाय के साथ समवाय सन्निकर्ष मानने पर अनवस्था होती है, अतः समवाय के साथ भी विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष वैसे ही माना जाता है, जैसे अभाव के साथ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org