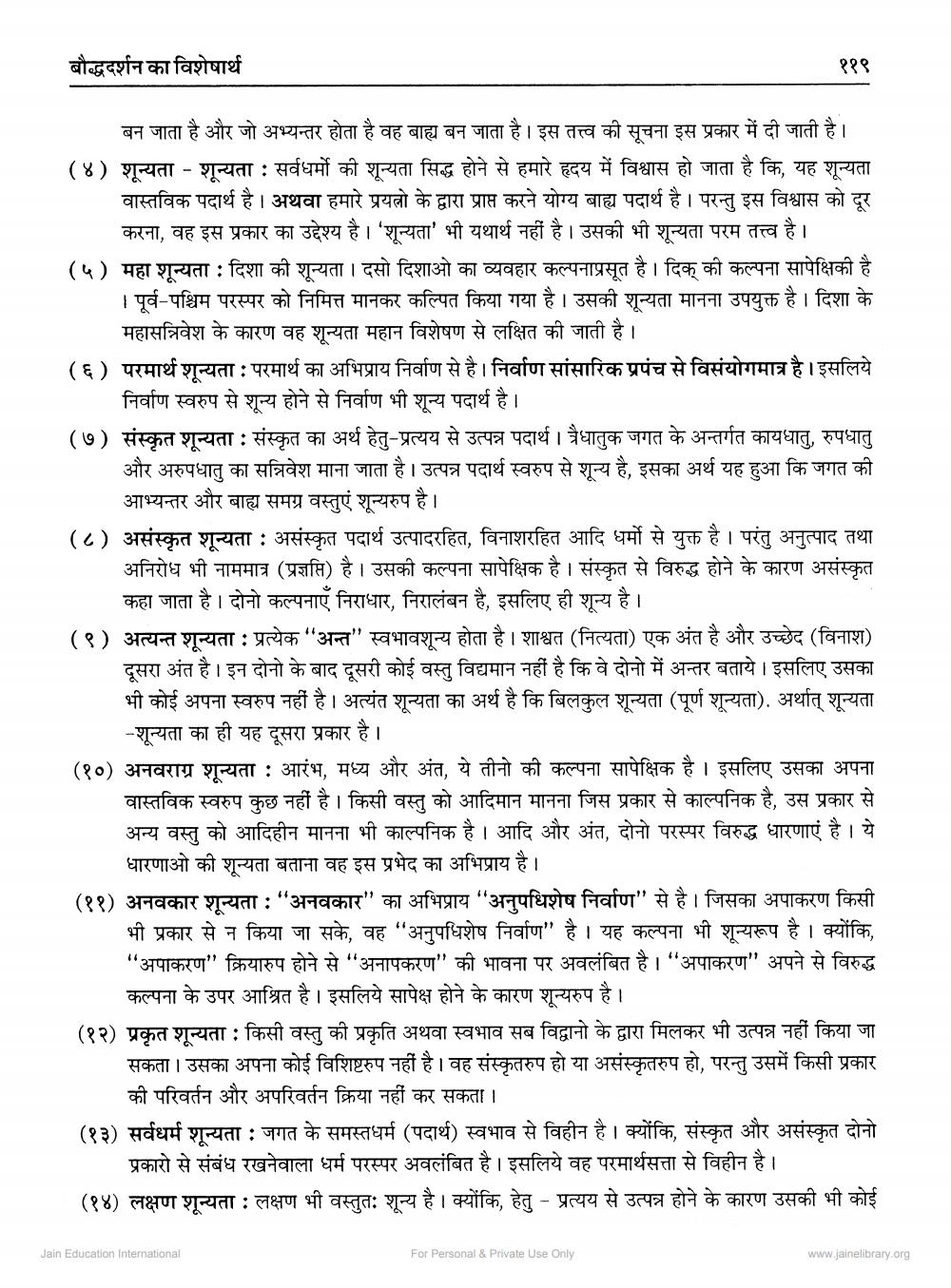________________
बौद्धदर्शन का विशेषार्थ
बन जाता है और जो अभ्यन्तर होता है वह बाह्य बन जाता है। इस तत्त्व की सूचना इस प्रकार में दी जाती है। (४) शून्यता - शून्यता : सर्वधर्मो की शून्यता सिद्ध होने से हमारे हृदय में विश्वास हो जाता है कि, यह शून्यता
वास्तविक पदार्थ है। अथवा हमारे प्रयत्नो के द्वारा प्राप्त करने योग्य बाह्य पदार्थ है । परन्तु इस विश्वास को दूर
करना, वह इस प्रकार का उद्देश्य है। 'शून्यता' भी यथार्थ नहीं है। उसकी भी शून्यता परम तत्त्व है। (५) महा शून्यता : दिशा की शून्यता । दसो दिशाओ का व्यवहार कल्पनाप्रसूत है। दिक् की कल्पना सापेक्षिकी है
। पूर्व-पश्चिम परस्पर को निमित्त मानकर कल्पित किया गया है। उसकी शून्यता मानना उपयुक्त है। दिशा के
महासन्निवेश के कारण वह शून्यता महान विशेषण से लक्षित की जाती है। (६) परमार्थ शून्यता : परमार्थ का अभिप्राय निर्वाण से है। निर्वाण सांसारिक प्रपंच से विसंयोगमात्र है। इसलिये
निर्वाण स्वरुप से शून्य होने से निर्वाण भी शून्य पदार्थ है। (७) संस्कृत शून्यता : संस्कृत का अर्थ हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न पदार्थ । वैधातुक जगत के अन्तर्गत कायधातु, रुपधातु
और अरुपधातु का सन्निवेश माना जाता है। उत्पन्न पदार्थ स्वरुप से शून्य है, इसका अर्थ यह हुआ कि जगत की
आभ्यन्तर और बाह्य समग्र वस्तुएं शून्यरुप है। (८) असंस्कृत शून्यता : असंस्कृत पदार्थ उत्पादरहित, विनाशरहित आदि धर्मो से युक्त है। परंतु अनुत्पाद तथा
अनिरोध भी नाममात्र (प्रज्ञप्ति) है। उसकी कल्पना सापेक्षिक है । संस्कृत से विरुद्ध होने के कारण असंस्कृत कहा जाता है। दोनो कल्पनाए निराधार, निरालंबन है, इसलिए ही शन्य है। अत्यन्त शून्यता : प्रत्येक "अन्त" स्वभावशून्य होता है । शाश्वत (नित्यता) एक अंत है और उच्छेद (विनाश) दूसरा अंत है। इन दोनो के बाद दूसरी कोई वस्तु विद्यमान नहीं है कि वे दोनो में अन्तर बताये । इसलिए उसका भी कोई अपना स्वरुप नहीं है। अत्यंत शून्यता का अर्थ है कि बिलकुल शून्यता (पूर्ण शून्यता). अर्थात् शून्यता
-शून्यता का ही यह दूसरा प्रकार है। (१०) अनवराग्र शून्यता : आरंभ, मध्य और अंत, ये तीनो की कल्पना सापेक्षिक है । इसलिए उसका अपना
वास्तविक स्वरुप कुछ नहीं है। किसी वस्तु को आदिमान मानना जिस प्रकार से काल्पनिक है, उस प्रकार से अन्य वस्तु को आदिहीन मानना भी काल्पनिक है। आदि और अंत, दोनो परस्पर विरुद्ध धारणाएं है। ये
धारणाओ की शून्यता बताना वह इस प्रभेद का अभिप्राय है। (११) अनवकार शून्यता : "अनवकार" का अभिप्राय "अनुपधिशेष निर्वाण" से है। जिसका अपाकरण किसी
भी प्रकार से न किया जा सके, वह "अनुपधिशेष निर्वाण" है । यह कल्पना भी शून्यरूप है । क्योंकि, "अपाकरण" क्रियारुप होने से "अनापकरण" की भावना पर अवलंबित है। "अपाकरण" अपने से विरुद्ध
कल्पना के उपर आश्रित है। इसलिये सापेक्ष होने के कारण शून्यरुप है। (१२) प्रकृत शून्यता : किसी वस्तु की प्रकृति अथवा स्वभाव सब विद्वानो के द्वारा मिलकर भी उत्पन्न नहीं किया जा
सकता। उसका अपना कोई विशिष्टरुप नहीं है। वह संस्कृतरुप हो या असंस्कृतरुप हो, परन्तु उसमें किसी प्रकार
की परिवर्तन और अपरिवर्तन क्रिया नहीं कर सकता। (१३) सर्वधर्म शून्यता : जगत के समस्तधर्म (पदार्थ) स्वभाव से विहीन है । क्योंकि, संस्कृत और असंस्कृत दोनो
प्रकारो से संबंध रखनेवाला धर्म परस्पर अवलंबित है। इसलिये वह परमार्थसत्ता से विहीन है। (१४) लक्षण शून्यता : लक्षण भी वस्तुतः शून्य है। क्योंकि, हेतु - प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण उसकी भी कोई
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org