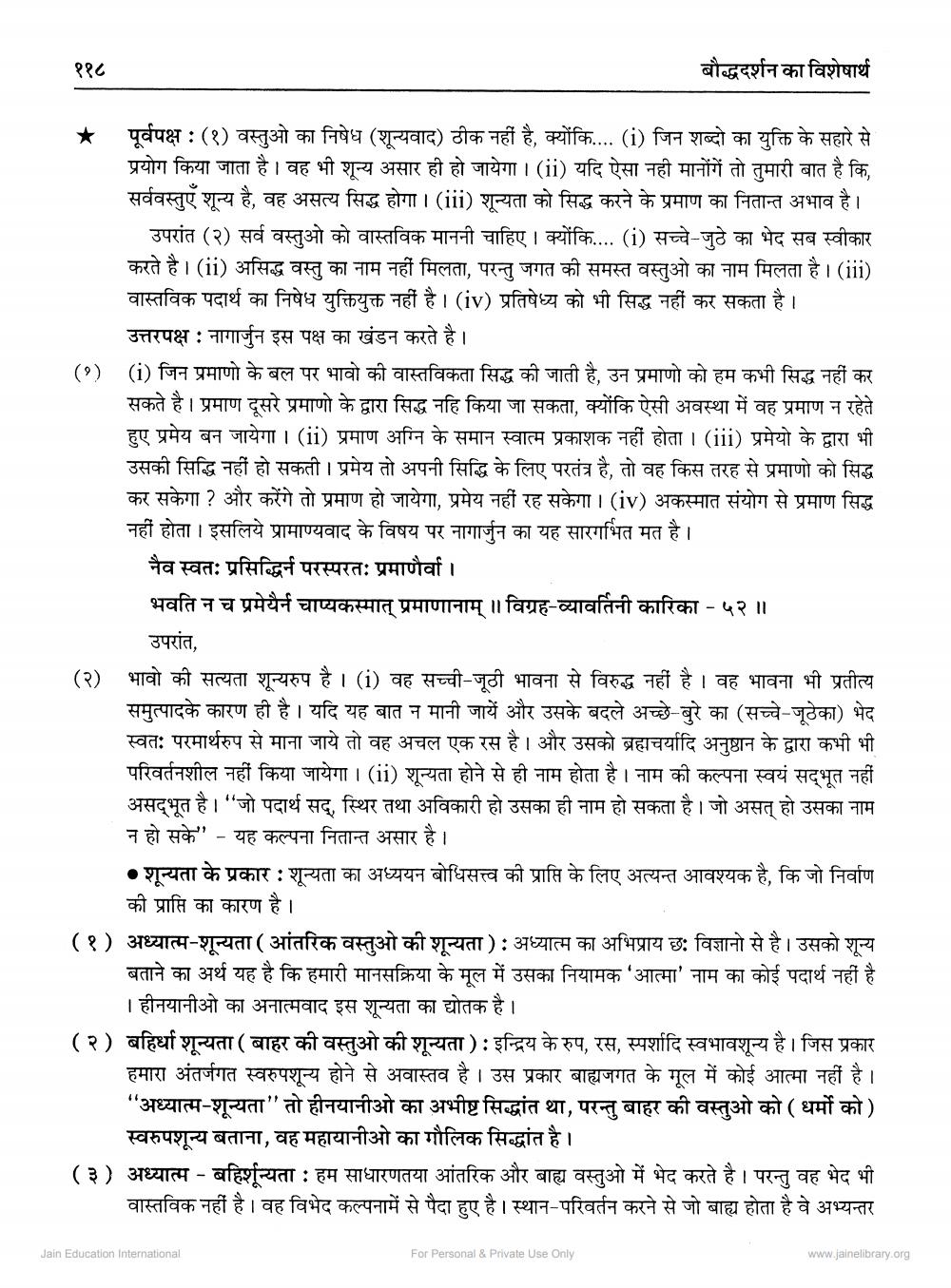________________
११८
बौद्धदर्शन का विशेषार्थ
★ पूर्वपक्ष : (१) वस्तुओ का निषेध (शून्यवाद) ठीक नहीं है, क्योंकि.... (i) जिन शब्दो का युक्ति के सहारे से
प्रयोग किया जाता है। वह भी शून्य असार ही हो जायेगा । (ii) यदि ऐसा नही मानोंगें तो तुमारी बात है कि, सर्ववस्तुएँ शून्य है, वह असत्य सिद्ध होगा। (iii) शून्यता को सिद्ध करने के प्रमाण का नितान्त अभाव है।
उपरांत (२) सर्व वस्तुओ को वास्तविक माननी चाहिए। क्योंकि.... (i) सच्चे-जुठे का भेद सब स्वीकार करते है। (ii) असिद्ध वस्तु का नाम नहीं मिलता, परन्तु जगत की समस्त वस्तुओ का नाम मिलता है। (iii) वास्तविक पदार्थ का निषेध युक्तियुक्त नहीं है। (iv) प्रतिषेध्य को भी सिद्ध नहीं कर सकता है। उत्तरपक्ष : नागार्जुन इस पक्ष का खंडन करते है। (i) जिन प्रमाणो के बल पर भावो की वास्तविकता सिद्ध की जाती है, उन प्रमाणो को हम कभी सिद्ध नहीं कर सकते है। प्रमाण दूसरे प्रमाणो के द्वारा सिद्ध नहि किया जा सकता, क्योंकि ऐसी अवस्था में वह प्रमाण न रहेते हुए प्रमेय बन जायेगा । (ii) प्रमाण अग्नि के समान स्वात्म प्रकाशक नहीं होता । (iii) प्रमेयो के द्वारा भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमेय तो अपनी सिद्धि के लिए परतंत्र है, तो वह किस तरह से प्रमाणो को सिद्ध कर सकेगा? और करेंगे तो प्रमाण हो जायेगा, प्रमेय नहीं रह सकेगा । (iv) अकस्मात संयोग से प्रमाण सिद्ध नहीं होता। इसलिये प्रामाण्यवाद के विषय पर नागार्जुन का यह सारगर्भित मत है।
नैव स्वतः प्रसिद्धिर्न परस्परतः प्रमाणैर्वा । भवति न च प्रमेयैर्न चाप्यकस्मात् प्रमाणानाम् ॥ विग्रह-व्यावर्तिनी कारिका - ५२ ॥ उपरांत, भावो की सत्यता शून्यरुप है । (i) वह सच्ची-जूठी भावना से विरुद्ध नहीं है । वह भावना भी प्रतीत्य समुत्पादके कारण ही है। यदि यह बात न मानी जायें और उसके बदले अच्छे-बुरे का (सच्चे-जूठेका) भेद स्वत: परमार्थरुप से माना जाये तो वह अचल एक रस है। और उसको ब्रह्मचर्यादि अनुष्ठान के द्वारा कभी भी परिवर्तनशील नहीं किया जायेगा । (ii) शून्यता होने से ही नाम होता है। नाम की कल्पना स्वयं सद्भूत नहीं असद्भूत है। "जो पदार्थ सद्, स्थिर तथा अविकारी हो उसका ही नाम हो सकता है। जो असत् हो उसका नाम न हो सके" - यह कल्पना नितान्त असार है। • शून्यता के प्रकार : शून्यता का अध्ययन बोधिसत्त्व की प्राप्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है, कि जो निर्वाण
की प्राप्ति का कारण है। (१) अध्यात्म-शून्यता (आंतरिक वस्तुओ की शून्यता): अध्यात्म का अभिप्राय छ: विज्ञानो से है। उसको शून्य
बताने का अर्थ यह है कि हमारी मानसक्रिया के मूल में उसका नियामक 'आत्मा' नाम का कोई पदार्थ नहीं है
। हीनयानीओ का अनात्मवाद इस शून्यता का द्योतक है। (२) बहिर्धा शून्यता ( बाहर की वस्तुओ की शून्यता): इन्द्रिय के रुप, रस, स्पर्शादि स्वभावशून्य है। जिस प्रकार
हमारा अंतर्जगत स्वरुपशून्य होने से अवास्तव है। उस प्रकार बाह्यजगत के मूल में कोई आत्मा नहीं है। "अध्यात्म-शून्यता" तो हीनयानीओ का अभीष्ट सिद्धांत था, परन्तु बाहर की वस्तुओ को (धर्मो को)
स्वरुपशून्य बताना, वह महायानीओ का गौलिक सिद्धांत है। (३) अध्यात्म - बहिशून्यता : हम साधारणतया आंतरिक और बाह्य वस्तुओ में भेद करते है। परन्तु वह भेद भी
वास्तविक नहीं है। वह विभेद कल्पनामें से पैदा हुए है। स्थान-परिवर्तन करने से जो बाह्य होता है वे अभ्यन्तर
(२) भारत
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org