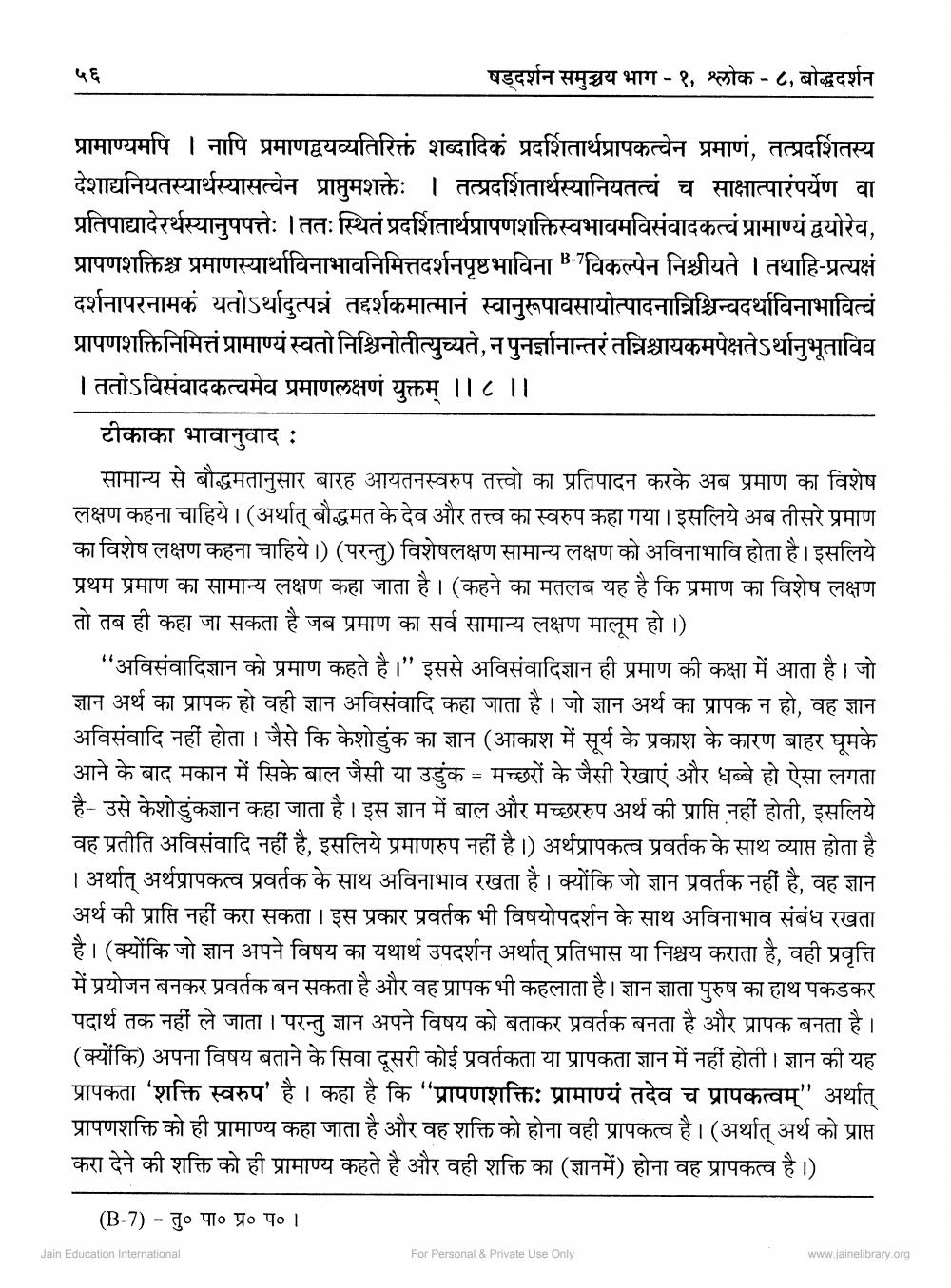________________
षड्दर्शन समुच्चय भाग - १, श्लोक - ८, बोद्धदर्शन
प्रामाण्यमपि । नापि प्रमाणद्वयव्यतिरिक्तं शब्दादिकं प्रदर्शितार्थप्रापकत्वेन प्रमाणं, तत्प्रदर्शितस्य देशाद्यनियतस्यार्थस्यासत्वेन प्राप्तुमशक्तेः । तत्प्रदर्शितार्थस्यानियतत्वं च साक्षात्पारंपर्येण वा प्रतिपाद्यादेरर्थस्यानुपपत्तेः । ततः स्थितं प्रदर्शितार्थप्रापणशक्तिस्वभावमविसंवादकत्वंप्रामाण्यं द्वयोरेव, प्रापणशक्तिश्च प्रमाणस्यार्थाविनाभावनिमित्तदर्शनपृष्ठभाविना B-7विकल्पेन निश्चीयते । तथाहि-प्रत्यक्ष दर्शनापरनामकं यतोऽर्थादुत्पन्नं तद्दर्शकमात्मानं स्वानुरूपावसायोत्पादनान्निश्चिन्वदर्थाविनाभावित्वं प्रापणशक्तिनिमित्तं प्रामाण्यं स्वतो निश्चिनोतीत्युच्यते, न पुनर्ज्ञानान्तरं तन्निश्चायकमपेक्षतेऽर्थानुभूताविव । ततोऽविसंवादकत्वमेव प्रमाणलक्षणं युक्तम् ।। ८ ।। टीकाका भावानुवाद :
सामान्य से बौद्धमतानुसार बारह आयतनस्वरुप तत्त्वो का प्रतिपादन करके अब प्रमाण का विशेष लक्षण कहना चाहिये। (अर्थात् बौद्धमत के देव और तत्त्व का स्वरुप कहा गया। इसलिये अब तीसरे प्रमाण का विशेष लक्षण कहना चाहिये।) (परन्तु) विशेषलक्षण सामान्य लक्षण को अविनाभावि होता है। इसलिये प्रथम प्रमाण का सामान्य लक्षण कहा जाता है। (कहने का मतलब यह है कि प्रमाण का विशेष लक्षण तो तब ही कहा जा सकता है जब प्रमाण का सर्व सामान्य लक्षण मालूम हो ।) ___ "अविसंवादिज्ञान को प्रमाण कहते है।" इससे अविसंवादिज्ञान ही प्रमाण की कक्षा में आता है। जो ज्ञान अर्थ का प्रापक हो वही ज्ञान अविसंवादि कहा जाता है। जो ज्ञान अर्थ का प्रापक न हो, वह ज्ञान अविसंवादि नहीं होता। जैसे कि केशोडंक का ज्ञान (आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण बाहर घूमके आने के बाद मकान में सिके बाल जैसी या उडंक = मच्छरों के जैसी रेखाएं और धब्बे हो ऐसा लगता है- उसे केशोडुंकज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान में बाल और मच्छररुप अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, इसलिये वह प्रतीति अविसंवादि नहीं है, इसलिये प्रमाणरुप नहीं है।) अर्थप्रापकत्व प्रवर्तक के साथ व्याप्त होता है । अर्थात् अर्थप्रापकत्व प्रवर्तक के साथ अविनाभाव रखता है। क्योंकि जो ज्ञान प्रवर्तक नहीं है, वह ज्ञान अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकता । इस प्रकार प्रवर्तक भी विषयोपदर्शन के साथ अविनाभाव संबंध रखता है। (क्योंकि जो ज्ञान अपने विषय का यथार्थ उपदर्शन अर्थात् प्रतिभास या निश्चय कराता है, वही प्रवृत्ति में प्रयोजन बनकर प्रवर्तक बन सकता है और वह प्रापक भी कहलाता है। ज्ञान ज्ञाता पुरुष का हाथ पकडकर पदार्थ तक नहीं ले जाता । परन्तु ज्ञान अपने विषय को बताकर प्रवर्तक बनता है और प्रापक बनता है। (क्योंकि) अपना विषय बताने के सिवा दूसरी कोई प्रवर्तकता या प्रापकता ज्ञान में नहीं होती । ज्ञान की यह प्रापकता ‘शक्ति स्वरुप' है। कहा है कि "प्रापणशक्तिः प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वम्" अर्थात् प्रापणशक्ति को ही प्रामाण्य कहा जाता है और वह शक्ति को होना वही प्रापकत्व है। (अर्थात् अर्थ को प्राप्त करा देने की शक्ति को ही प्रामाण्य कहते है और वही शक्ति का (ज्ञानमें) होना वह प्रापकत्व है।)
(B-7) - तु० पा० प्र० प० ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org