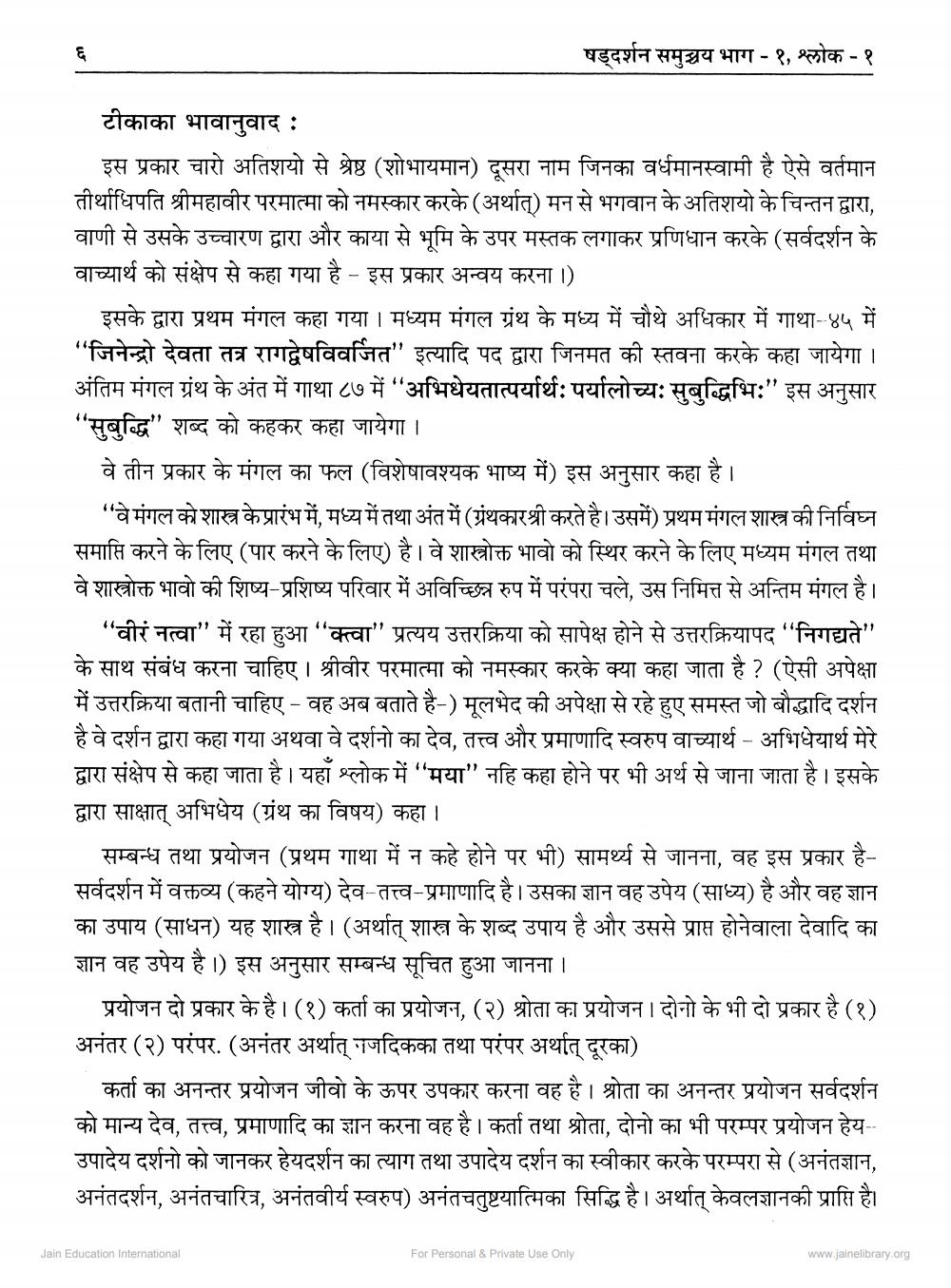________________
६
टीकाका भावानुवाद :
इस प्रकार चारो अतिशयो से श्रेष्ठ (शोभायमान) दूसरा नाम जिनका वर्धमानस्वामी है ऐसे वर्तमान तीर्थाधिपति श्रीमहावीर परमात्मा को नमस्कार करके (अर्थात्) मन से भगवान के अतिशयो के चिन्तन द्वारा, वाणी से उसके उच्चारण द्वारा और काया से भूमि के उपर मस्तक लगाकर प्रणिधान करके (सर्वदर्शन के वाच्यार्थ को संक्षेप से कहा गया है - इस प्रकार अन्वय करना ।)
षड्दर्शन समुच्चय भाग - १, श्लोक - १
इसके द्वारा प्रथम मंगल कहा गया । मध्यम मंगल ग्रंथ के मध्य में चौथे अधिकार में गाथा - -४५ में "जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्वेषविवर्जित" इत्यादि पद द्वारा जिनमत की स्तवना करके कहा जायेगा । अंतिम मंगल ग्रंथ के अंत में गाथा ८७ में "अभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः " इस अनुसार "सुबुद्धि" शब्द को कहकर कहा जायेगा ।
वे तीन प्रकार के मंगल का फल (विशेषावश्यक भाष्य में) इस अनुसार कहा है I
“वे मंगल को शास्त्र केप्रारंभ में, मध्य में तथा अंत में (ग्रंथकार श्री करते है। उसमें) प्रथम मंगल शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति करने के लिए (पार करने के लिए) है। वे शास्त्रोक्त भावो को स्थिर करने के लिए मध्यम मंगल तथा वे शास्त्रोक्त भावो की शिष्य-प्रशिष्य परिवार में अविच्छिन्न रुप में परंपरा चले, उस निमित्त से अन्तिम मंगल है।
"वीरं नत्वा" में रहा हुआ "क्त्वा" प्रत्यय उत्तरक्रिया को सापेक्ष होने से उत्तरक्रियापद "निगद्यते " के साथ संबंध करना चाहिए । श्रीवीर परमात्मा को नमस्कार करके क्या कहा जाता है ? (ऐसी अपेक्षा में उत्तरक्रिया बतानी चाहिए - वह अब बताते है -) मूलभेद की अपेक्षा से रहे हुए समस्त जो बौद्धादि दर्शन है वे दर्शन द्वारा कहा गया अथवा वे दर्शनो का देव, तत्त्व और प्रमाणादि स्वरुप वाच्यार्थ - अभिधेयार्थ मेरे द्वारा संक्षेप से कहा जाता है । यहाँ श्लोक में "मया" नहि कहा होने पर भी अर्थ से जाना जाता है । इसके द्वारा साक्षात् अभिधेय (ग्रंथ का विषय) कहा।
सम्बन्ध तथा प्रयोजन (प्रथम गाथा में न कहे होने पर भी) सामर्थ्य से जानना, वह इस प्रकार हैसर्वदर्शन में वक्तव्य (कहने योग्य) देव-तत्त्व - प्रमाणादि है। उसका ज्ञान वह उपेय (साध्य) है और वह ज्ञान का उपाय (साधन) यह शास्त्र है। (अर्थात् शास्त्र के शब्द उपाय है और उससे प्राप्त होनेवाला देवादि का ज्ञान वह उपेय है।) इस अनुसार सम्बन्ध सूचित हुआ जानना ।
प्रयोजन दो प्रकार के है । (१) कर्ता का प्रयोजन, (२) श्रोता का प्रयोजन। दोनो के भी दो प्रकार है (१) अनंतर (२) परंपर. (अनंतर अर्थात् नजदिकका तथा परंपर अर्थात् दूरका)
कर्ता का अनन्तर प्रयोजन जीवो के ऊपर उपकार करना वह है । श्रोता का अनन्तर प्रयोजन सर्वदर्शन को मान्य देव, तत्त्व, प्रमाणादि का ज्ञान करना वह है । कर्ता तथा श्रोता, दोनो का भी परम्पर प्रयोजन हेय-उपादेय दर्शनो को जानकर हेयदर्शन का त्याग तथा उपादेय दर्शन का स्वीकार करके परम्परा से (अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र, अनंतवीर्य स्वरुप) अनंतचतुष्टयात्मिका सिद्धि है । अर्थात् केवलज्ञानकी प्राप्ति है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org