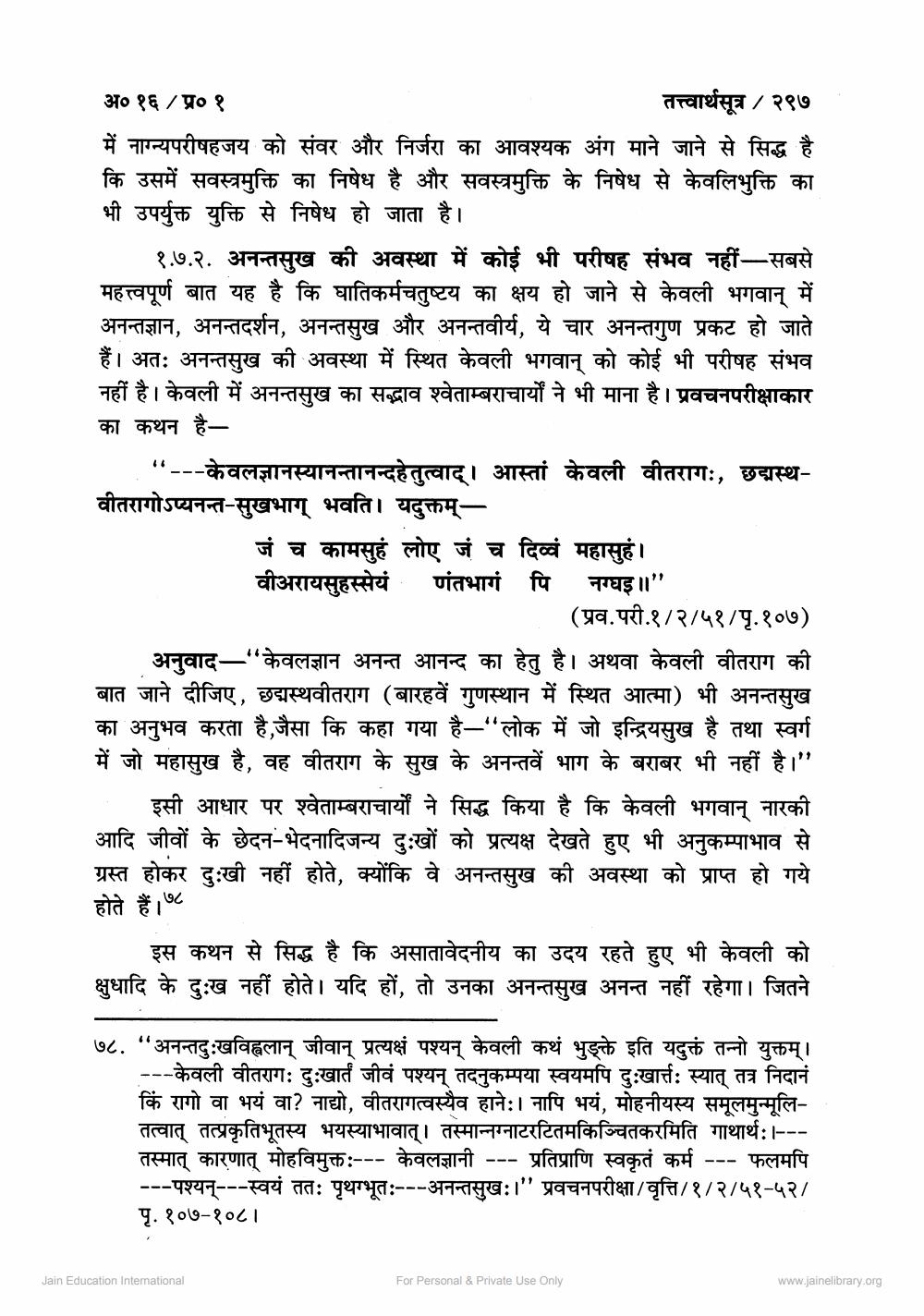________________
अ०१६ / प्र०१
तत्त्वार्थसूत्र / २९७ में नाग्न्यपरीषहजय को संवर और निर्जरा का आवश्यक अंग माने जाने से सिद्ध है कि उसमें सवस्त्रमुक्ति का निषेध है और सवस्त्रमुक्ति के निषेध से केवलिभुक्ति का भी उपर्युक्त युक्ति से निषेध हो जाता है।
१.७.२. अनन्तसुख की अवस्था में कोई भी परीषह संभव नहीं-सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि घातिकर्मचतुष्टय का क्षय हो जाने से केवली भगवान् में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य, ये चार अनन्तगुण प्रकट हो जाते हैं। अतः अनन्तसुख की अवस्था में स्थित केवली भगवान् को कोई भी परीषह संभव नहीं है। केवली में अनन्तसुख का सद्भाव श्वेताम्बराचार्यों ने भी माना है। प्रवचनपरीक्षाकार का कथन है
"---केवलज्ञानस्यानन्तानन्दहेतुत्वाद्। आस्तां केवली वीतरागः, छद्मस्थवीतरागोऽप्यनन्त-सुखभाग् भवति। यदुक्तम्
जं च कामसुहं लोए जं च दिव्वं महासुहं। वीअरायसुहस्सेयं णंतभागं पि नग्घइ॥"
(प्रव.परी.१/२/५१/पृ.१०७) अनुवाद-"केवलज्ञान अनन्त आनन्द का हेतु है। अथवा केवली वीतराग की बात जाने दीजिए, छद्मस्थवीतराग (बारहवें गुणस्थान में स्थित आत्मा) भी अनन्तसुख का अनुभव करता है,जैसा कि कहा गया है-"लोक में जो इन्द्रियसुख है तथा स्वर्ग में जो महासुख है, वह वीतराग के सुख के अनन्तवें भाग के बराबर भी नहीं है।"
इसी आधार पर श्वेताम्बराचार्यों ने सिद्ध किया है कि केवली भगवान् नारकी आदि जीवों के छेदन-भेदनादिजन्य दुःखों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी अनुकम्पाभाव से ग्रस्त होकर दुःखी नहीं होते, क्योंकि वे अनन्तसुख की अवस्था को प्राप्त हो गये होते हैं।७८
इस कथन से सिद्ध है कि असातावेदनीय का उदय रहते हुए भी केवली को क्षुधादि के दुःख नहीं होते। यदि हों, तो उनका अनन्तसुख अनन्त नहीं रहेगा। जितने
७८. "अनन्तदुःखविह्वलान् जीवान् प्रत्यक्षं पश्यन् केवली कथं भुङ्क्ते इति यदुक्तं तन्नो युक्तम्।
---केवली वीतरागः दुःखार्तं जीवं पश्यन् तदनुकम्पया स्वयमपि दुःखातः स्यात् तत्र निदानं किं रागो वा भयं वा? नाद्यो, वीतरागत्वस्यैव हानेः। नापि भयं, मोहनीयस्य समूलमुन्मूलितत्वात् तत्प्रकृतिभूतस्य भयस्याभावात्। तस्मान्नग्नाटरटितमकिञ्चितकरमिति गाथार्थः।--- तस्मात् कारणात् मोहविमुक्त:--- केवलज्ञानी --- प्रतिप्राणि स्वकृतं कर्म --- फलमपि ---पश्यन्---स्वयं ततः पृथग्भूतः---अनन्तसुखः।" प्रवचनपरीक्षा/वृत्ति/१/२/५१-५२/ पृ.१०७-१०८।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org