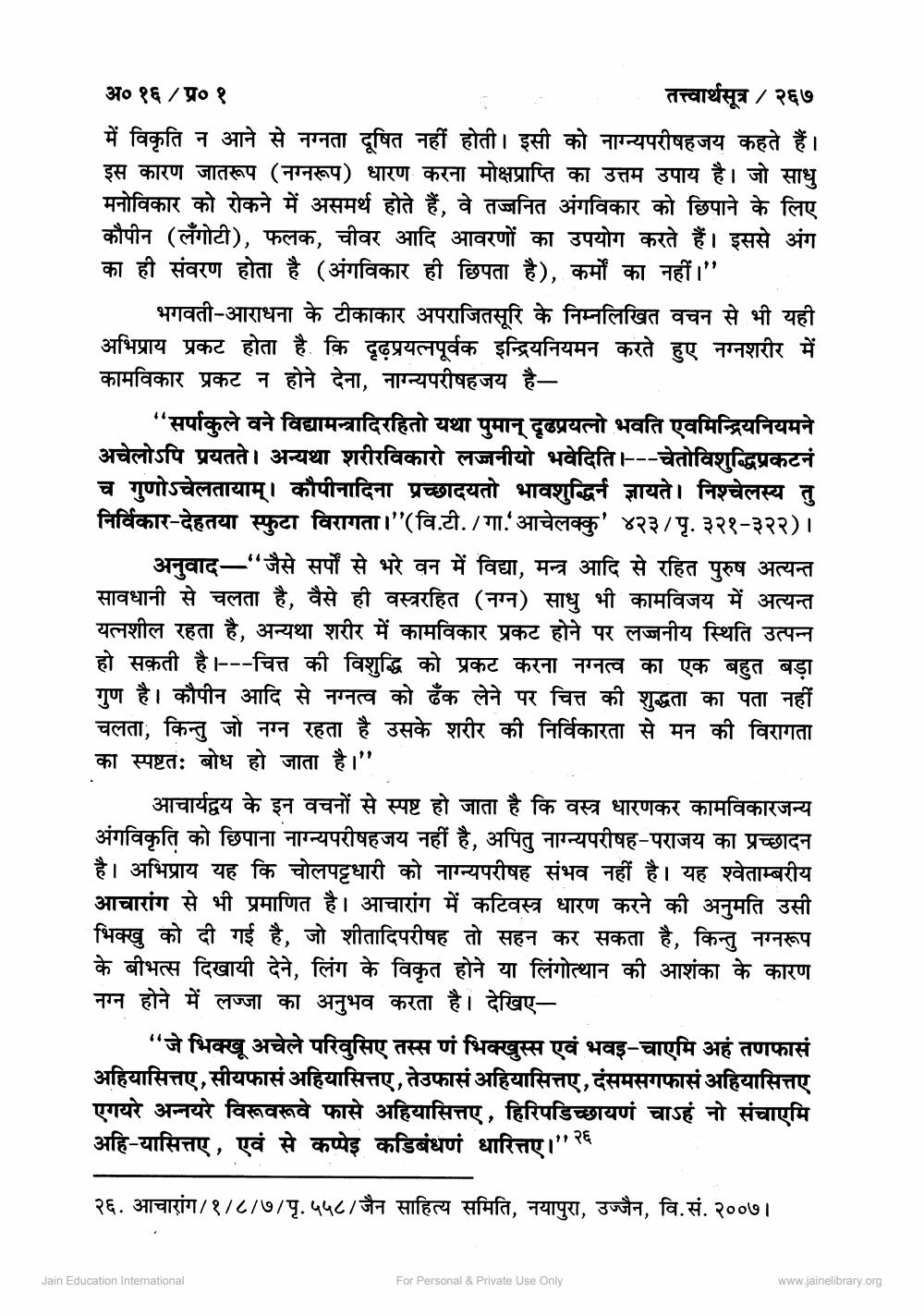________________
अ०१६ / प्र०१
तत्त्वार्थसूत्र / २६७ में विकृति न आने से नग्नता दूषित नहीं होती। इसी को नाग्न्यपरीषहजय कहते हैं। इस कारण जातरूप (नग्नरूप) धारण करना मोक्षप्राप्ति का उत्तम उपाय है। जो साधु मनोविकार को रोकने में असमर्थ होते हैं, वे तजनित अंगविकार को छिपाने के लिए कौपीन (लँगोटी), फलक, चीवर आदि आवरणों का उपयोग करते हैं। इससे अंग का ही संवरण होता है (अंगविकार ही छिपता है), कर्मों का नहीं।" __भगवती-आराधना के टीकाकार अपराजितसूरि के निम्नलिखित वचन से भी यही अभिप्राय प्रकट होता है कि दृढ़प्रयत्नपूर्वक इन्द्रियनियमन करते हुए नग्नशरीर में कामविकार प्रकट न होने देना, नाग्न्यपरीषहजय है
"सर्पाकुले वने विद्यामन्त्रादिरहितो यथा पुमान् दृढप्रयत्नो भवति एवमिन्द्रियनियमने अचेलोऽपि प्रयतते। अन्यथा शरीरविकारो लजनीयो भवेदिति।---चेतोविशुद्धिप्रकटनं च गुणोऽचेलतायाम्। कौपीनादिना प्रच्छादयतो भावशुद्धिर्न ज्ञायते। निश्चेलस्य तु निर्विकार-देहतया स्फुटा विरागता।"(वि.टी./गा. आचेलक्कु' ४२३ / पृ. ३२१-३२२)।
अनुवाद-"जैसे सर्यों से भरे वन में विद्या, मन्त्र आदि से रहित पुरुष अत्यन्त सावधानी से चलता है, वैसे ही वस्त्ररहित (नग्न) साधु भी कामविजय में अत्यन्त यत्नशील रहता है, अन्यथा शरीर में कामविकार प्रकट होने पर लज्जनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है।---चित्त की विशुद्धि को प्रकट करना नग्नत्व का एक बहुत बड़ा गुण है। कौपीन आदि से नग्नत्व को ढंक लेने पर चित्त की शुद्धता का पता नहीं चलता, किन्तु जो नग्न रहता है उसके शरीर की निर्विकारता से मन की विरागता का स्पष्टतः बोध हो जाता है।"
आचार्यद्वय के इन वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि वस्त्र धारणकर कामविकारजन्य अंगविकृति को छिपाना नाग्न्यपरीषहजय नहीं है, अपितु नाग्न्यपरीषह-पराजय का प्रच्छादन है। अभिप्राय यह कि चोलपट्टधारी को नाग्न्यपरीषह संभव नहीं है। यह श्वेताम्बरीय आचारांग से भी प्रमाणित है। आचारांग में कटिवस्त्र धारण करने की अनुमति उसी भिक्खु को दी गई है, जो शीतादिपरीषह तो सहन कर सकता है, किन्तु नग्नरूप के बीभत्स दिखायी देने, लिंग के विकृत होने या लिंगोत्थान की आशंका के कारण नग्न होने में लज्जा का अनुभव करता है। देखिए
"जे भिक्खू अचेले परिवुसिए तस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ-चाएमि अहं तणफासं अहियासित्तए, सीयफासं अहियासित्तए, तेउफासं अहियासित्तए, दंसमसगफासंअहियासित्तए एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहियासित्तए, हिरिपडिच्छायणं चाऽहं नो संचाएमि अहि-यासित्तए , एवं से कप्पेइ कडिबंधणं धारित्तए।" २६
२६. आचारांग/१/८/७/पृ. ५५८/ जैन साहित्य समिति, नयापुरा, उज्जैन, वि.सं. २००७ ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org