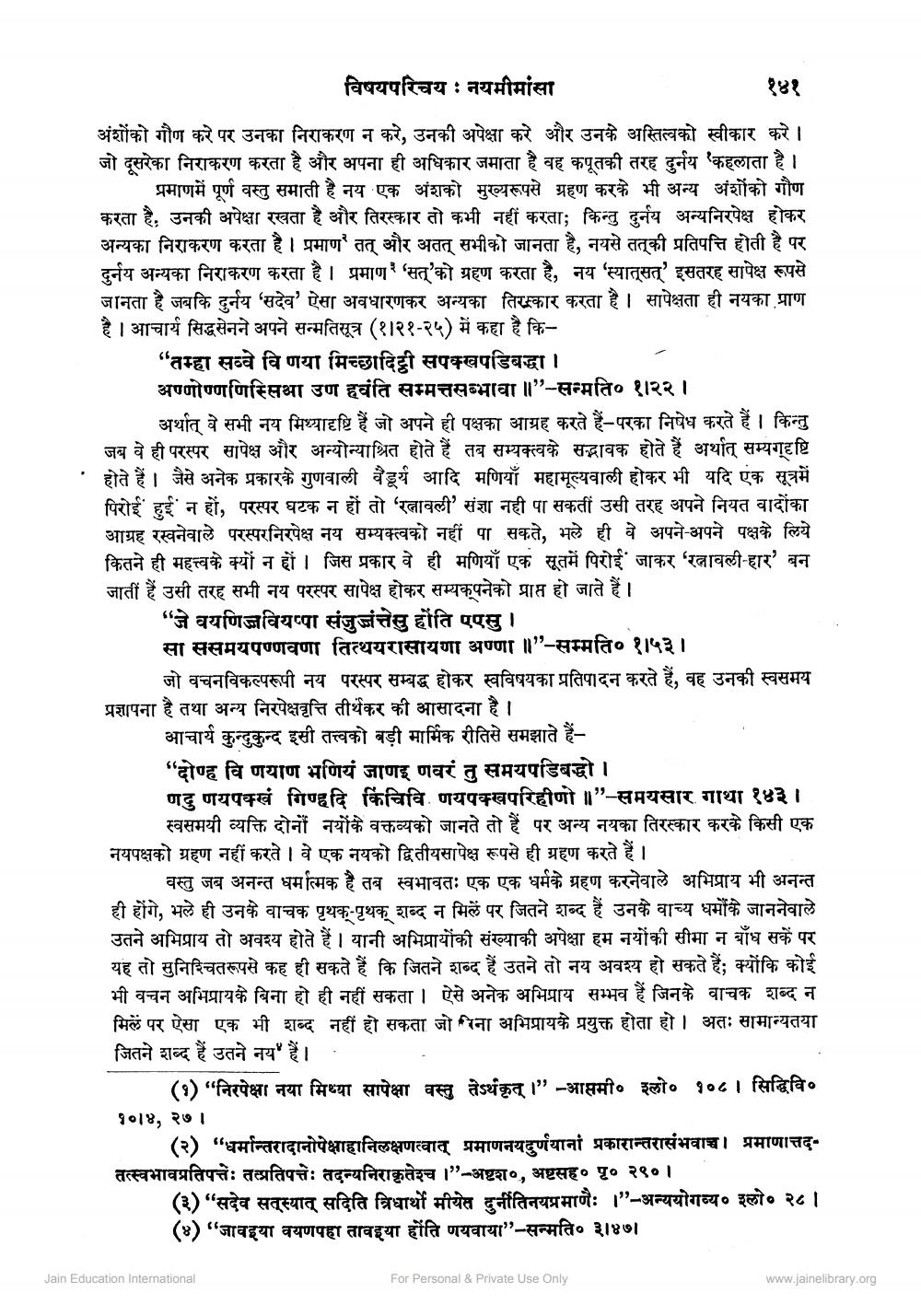________________
विषयपरिचय: नयमीमांसा
१४१
अंशोंको गौण करे पर उनका निराकरण न करे, उनकी अपेक्षा करे और उनके अस्तित्वको स्वीकार करे । जो दूसरेका निराकरण करता है और अपना ही अधिकार जमाता है वह कपूतकी तरह दुर्नय ' कहलाता है । प्रमाण में पूर्ण वस्तु समाती है नय एक अंशको मुख्यरूपसे ग्रहण करके भी अन्य अंशोंको गौण करता है, उनकी अपेक्षा रखता है और तिरस्कार तो कभी नहीं करता; किन्तु दुर्नय अन्यनिरपेक्ष होकर अन्यका निराकरण करता है । प्रमाण' तत् और अतत् सभी को जानता है, नयसे तत्की प्रतिपत्ति होती है पर दुर्नय अन्यका निराकरण करता है । प्रमाण' 'सत्' को ग्रहण करता है, नय 'स्यात्सत्' इसतरह सापेक्ष रूपसे जानता है जबकि दुर्न 'सदेव' ऐसा अवधारणकर अन्यका तिरस्कार करता है । सापेक्षता ही नयका प्राण है । आचार्य सिद्धसेनने अपने सन्मतिसूत्र (१।२१-२५) में कहा है कि
I
" तम्हा सव्वे विणया मिच्छादिट्ठी सपक्खपडिबद्धा । अण्णोण्णणिस्तिभा उण हवंति सम्मत्तसन्भावा ॥" - सन्मति० १।२२ ।
अर्थात् वे सभी नय मिध्यादृष्टि हैं जो अपने ही पक्षका आग्रह करते हैं- परका निषेध करते हैं । किन्तु जब वे ही परस्पर सापेक्ष और अन्योन्याश्रित होते हैं तब सम्यक्त्वके सद्भावक होते हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि होते हैं । जैसे अनेक प्रकारके गुणवाली वैडूर्य आदि मणियाँ महामूल्यवाली होकर भी यदि एक सूत्रमें पिरोई हुई न हों, परस्पर घटक न हों तो 'रत्नावली' संज्ञा नही पा सकतीं उसी तरह अपने नियत वादोंका आग्रह रखनेवाले परस्पर निरपेक्ष नय सम्यक्त्वको नहीं पा सकते, भले ही वे अपने-अपने पक्ष के लिये कितने ही महत्त्व के क्यों न हों । जिस प्रकार वे ही मणियाँ एक सूतमें पिरोई' जाकर 'रत्नावली - हार' बन जातीं हैं उसी तरह सभी नय परस्पर सापेक्ष होकर सम्यक्पनेको प्राप्त हो जाते हैं ।
"जे वयणिज्जवियप्पा संजुजंत्तेसु होंति एएसु ।
सा ससमय पण्णवणा तित्थयरासायणा अण्णा ॥ " - सम्मति० १।५३ ।
जो वचनविकल्परूपी नय परस्पर सम्बद्ध होकर स्वविषयका प्रतिपादन करते हैं, वह उनकी स्वसमय प्रज्ञापना है तथा अन्य निरपेक्षवृत्ति तीर्थंकर की आसादना है ।
आचार्य कुन्दुकुन्द इसी तत्त्वको बड़ी मार्मिक रीति से समझाते हैं
" दोह वि णयाण भणियं जाणइ णवरं तु समयपडिबद्धो ।
दु
पक्खं गिदि किंचिवि णयपक्खपरिहीणो ॥ " - समयसार गाथा १४३ । स्वमयी व्यक्ति दोनों नयोंके वक्तव्यको जानते तो हैं पर अन्य नयका तिरस्कार करके किसी एक नयपक्षको ग्रहण नहीं करते । वे एक नयको द्वितीयसापेक्ष रूपसे ही ग्रहण करते हैं ।
वस्तु जब अनन्त धर्मात्मक है तब स्वभावतः एक एक धर्मके ग्रहण करनेवाले अभिप्राय भी अनन्त ही होंगे, भले ही उनके वाचक पृथक-पृथक शब्द न मिलें पर जितने शब्द हैं उनके वाच्य धर्मोके जाननेवाले उतने अभिप्राय तो अवश्य होते हैं। यानी अभिप्रायोंकी संख्याकी अपेक्षा हम नयोंकी सीमा न बाँध सकें पर यह तो सुनिश्चित रूपसे कह ही सकते हैं कि जितने शब्द हैं उतने तो नय अवश्य हो सकते हैं; क्योंकि कोई भी वचन अभिप्राय के बिना ही नहीं सकता । ऐसे अनेक अभिप्राय सम्भव हैं जिनके वाचक शब्द न मिलें पर ऐसा एक भी शब्द नहीं हो सकता जो बिना अभिप्रायके प्रयुक्त होता हो । अतः सामान्यतया जितने शब्द हैं उतने नय" हैं ।
(१) "निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ।" - आप्तमी० इलो० १०८ । सिद्धिवि० १०१४, २७ ।
(२) "धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात् प्रमाणनयदुर्णयानां प्रकारान्तरासंभवाञ्च । प्रमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च ।” - अष्टश०, अष्टसह० पृ० २९० ।
(३) “सदेव सत्स्यात् सदिति विधार्थी मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणैः |” - अन्ययोगव्य० श्लो० २८ । ( ४ ) " जावइया वयण पहा तावइया होंति णयवाया " - सन्मति ० ३।४७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org