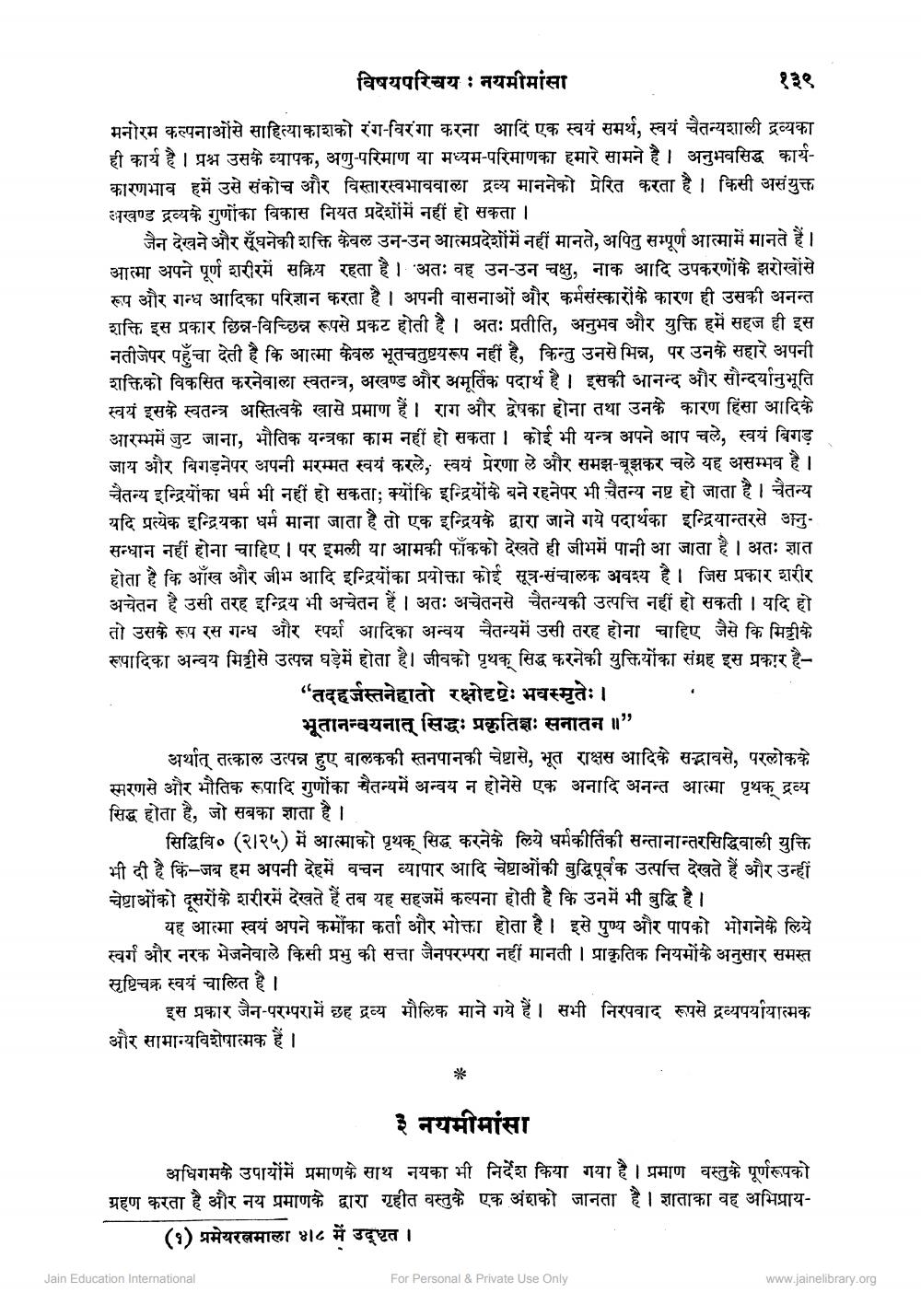________________
विषयपरिचय : नयमीमांसा मनोरम कल्पनाओंसे साहित्याकाशको रंग-विरंगा करना आदि एक स्वयं समर्थ, स्वयं चैतन्यशाली द्रव्यका ही कार्य है । प्रश्न उसके व्यापक, अणु-परिमाण या मध्यम-परिमाणका हमारे सामने है। अनुभवसिद्ध कार्यकारणभाव हमें उसे संकोच और विस्तारस्वभाववाला द्रव्य माननेको प्रेरित करता है। किसी असंयुक्त अखण्ड द्रव्यके गुणोंका विकास नियत प्रदेशों में नहीं हो सकता।
जैन देखने और सूंघनेकी शक्ति केवल उन-उन आत्मप्रदेशोंमें नहीं मानते, अपितु सम्पूर्ण आत्मामें मानते हैं। आत्मा अपने पूर्ण शरीरमें सक्रिय रहता है। अतः वह उन-उन चक्षु, नाक आदि उपकरणों के झरोखोंसे रूप और गन्ध आदिका परिज्ञान करता है। अपनी वासनाओं और कर्मसंस्कारों के कारण ही उसकी अनन्त शक्ति इस प्रकार छिन्न-विच्छिन्न रूपसे प्रकट होती है। अतः प्रतीति, अनुभव और युक्ति हमें सहज ही इस नतीजेपर पहुँचा देती है कि आत्मा केवल भूतचतुष्टयरूप नहीं है, किन्तु उनसे भिन्न, पर उनके सहारे अपनी शक्तिको विकसित करनेवाला स्वतन्त्र, अखण्ड और अमूर्तिक पदार्थ है । इसकी आनन्द और सौन्दर्यानुभूति स्वयं इसके स्वतन्त्र अस्तित्वके खासे प्रमाण हैं। राग और द्वेषका होना तथा उनके कारण हिंसा आदिके आरम्भमें जुट जाना, भौतिक यन्त्रका काम नहीं हो सकता । कोई भी यन्त्र अपने आप चले, स्वयं बिगड़ जाय और बिगड़नेपर अपनी मरम्मत स्वयं करले, स्वयं प्रेरणा ले और समझ-बूझकर चले यह असम्भव है। चैतन्य इन्द्रियोंका धर्म भी नहीं हो सकता; क्योंकि इन्द्रियों के बने रहनेपर भी चैतन्य नष्ट हो जाता है। चैतन्य यदि प्रत्येक इन्द्रियका धर्म माना जाता है तो एक इन्द्रियके द्वारा जाने गये पदार्थका इन्द्रियान्तरसे अनुसन्धान नहीं होना चाहिए । पर इमली या आमकी फाँकको देखते ही जीभमें पानी आ जाता है । अतः ज्ञात होता है कि आँख और जीभ आदि इन्द्रियोंका प्रयोक्ता कोई सूत्र-संचालक अवश्य है। जिस प्रकार शरीर अचेतन है उसी तरह इन्द्रिय भी अचेतन हैं । अतः अचेतनसे चैतन्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि हो तो उसके रूप रस गन्ध और स्पर्श आदिका अन्वय चैतन्यमें उसी तरह होना चाहिए जैसे कि मिट्टीके रूपादिका अन्वय मिट्टीसे उत्पन्न घड़ेमें होता है। जीवको पृथक् सिद्ध करनेकी युक्तियोंका संग्रह इस प्रकार है
"तदहर्जस्तनेहातो रक्षोदृष्टेः भवस्मृतेः।
भूतानन्वयनात् सिद्धः प्रकृतिज्ञः सनातन ॥" अर्थात् तत्काल उत्पन्न हुए बालककी स्तनपानकी चेष्टासे, भूत राक्षस आदिके सद्भावसे, परलोकके स्मरणसे और भौतिक रूपादि गुणोंका चैतन्यमें अन्वय न होनेसे एक अनादि अनन्त आत्मा पृथक् द्रव्य सिद्ध होता है, जो सबका ज्ञाता है।
सिद्धिवि० (२।२५) में आत्माको पृथक सिद्ध करनेके लिये धर्मकीर्तिकी सन्तानान्तरसिद्धिवाली युक्ति भी दी है किं-जब हम अपनी देहमें वचन व्यापार आदि चेष्टाओंकी बुद्धिपूर्वक उत्पत्ति देखते हैं और उन्हीं चेष्टाओंको दूसरोंके शरीरमें देखते हैं तब यह सहजमें कल्पना होती है कि उनमें भी बुद्धि है।
यह आत्मा स्वयं अपने कर्मोंका कर्ता और भोक्ता होता है। इसे पुण्य और पापको भोगनेके लिये स्वर्ग और नरक भेजनेवाले किसी प्रभु की सत्ता जैनपरम्परा नहीं मानती । प्राकृतिक नियमों के अनुसार समस्त सृष्टिचक्र स्वयं चालित है।
___ इस प्रकार जैन-परम्परामें छह द्रव्य मौलिक माने गये हैं। सभी निरपवाद रूपसे द्रव्यपर्यायात्मक और सामान्यविशेषात्मक हैं।
३ नयमीमांसा अधिगमके उपायोंमें प्रमाणके साथ नयका भी निर्देश किया गया है । प्रमाण वस्तुके पूर्णरूपको ग्रहण करता है और नय प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुके एक अंशको जानता है। ज्ञाताका वह अभिप्राय
(१) प्रमेयरत्नमाला ४।८ में उद्धृत ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org