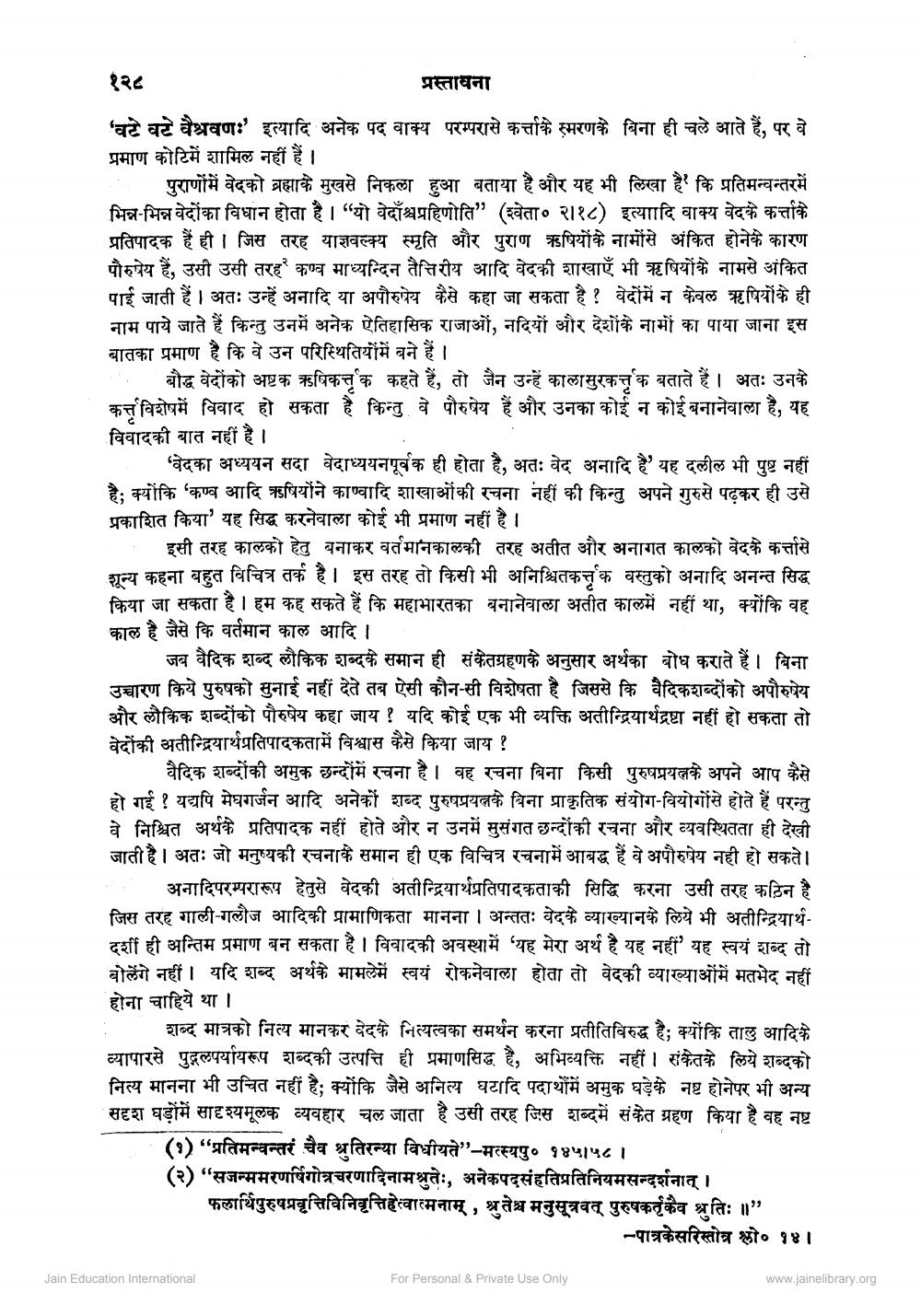________________
१२८
प्रस्तावना
'वटे वटे वैश्रवणः' इत्यादि अनेक पद वाक्य परम्परासे कर्त्ताके स्मरणके बिना ही चले आते हैं, पर वे प्रमाण कोटि में शामिल नहीं हैं ।
पुराणोंमें वेदको ब्रह्माके मुखसे निकला हुआ बताया है और यह भी लिखा है कि प्रतिमन्वन्तर में भिन्न-भिन्न वेदों का विधान होता है । “यो वेदाँश्चप्रहिणोति” (श्वेता ० २।१८) इत्यादि वाक्य वेदके कर्त्ता के प्रतिपादक हैं ही । जिस तरह याज्ञवल्क्य स्मृति और पुराण ऋषियोंके नामोंसे अंकित होनेके कारण पौरुषेय हैं, उसी उसी तरह कण्व माध्यन्दिन तैत्तिरीय आदि वेदकी शाखाएँ भी ऋषियोंके नामसे अंकि पाई जाती हैं । अतः उन्हें अनादि या अपौरुषेय कैसे कहा जा सकता है ? वेदोंमें न केवल ऋषियों के ही नाम पाये जाते हैं किन्तु उनमें अनेक ऐतिहासिक राजाओं, नदियों और देशों के नामों का पाया जाना इस बातका प्रमाण है कि वे उन परिस्थितियों में बने हैं ।
बौद्ध वेदोंको अष्टक ऋषिकर्तृक कहते हैं, तो जैन उन्हें कालासुरकर्त्तृक बताते हैं । अतः उनके कर्त्तृविशेष में विवाद हो सकता है किन्तु वे पौरुषेय हैं और उनका कोई न कोई बनानेवाला है, यह विवादकी बात नहीं है ।
'वेदका अध्ययन सदा वेदाध्ययनपूर्वक ही होता है, अतः वेद अनादि है' यह दलील भी पुष्ट नहीं है; क्योंकि 'कण्व आदि ऋषियोंने काण्वादि शाखाओं की रचना नहीं की किन्तु अपने गुरुसे पढ़कर ही उसे प्रकाशित किया' यह सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है ।
इसी तरह कालको हेतु बनाकर वर्तमानकालकी तरह अतीत और अनागत कालको वेदके कर्त्तासे शून्य कहना बहुत विचित्र तर्क है । इस तरह तो किसी भी अनिश्चितकर्त्तृक वस्तुको अनादि अनन्त सिद्ध किया जा सकता है | हम कह सकते हैं कि महाभारतका बनानेवाला अतीत कालमें नहीं था, क्योंकि वह काल है जैसे कि वर्तमान काल आदि ।
जब वैदिक शब्द लौकिक शब्दके समान ही संकेतग्रहणके अनुसार अर्थका बोध कराते हैं। बिना उच्चारण किये पुरुषको सुनाई नहीं देते तब ऐसी कौन-सी विशेषता है जिससे कि वैदिकशब्दों को अपौरुषेय और लौकिक शब्दोंको पौरुषेय कहा जाय ? यदि कोई एक भी व्यक्ति अतीन्द्रियार्थद्रष्टा नहीं हो सकता तो वेदोंकी अतीन्द्रियार्थप्रतिपादकता में विश्वास कैसे किया जाय ?
वैदिक शब्दोंकी अमुक छन्दोंमें रचना है । वह रचना बिना किसी पुरुषप्रयत्नके अपने आप कैसे हो गई ? यद्यपि मेघगर्जन आदि अनेकों शब्द पुरुषप्रयत्नके बिना प्राकृतिक संयोग-वियोगोंसे होते हैं परन्तु वे निश्चित अर्थ प्रतिपादक नहीं होते और न उनमें सुसंगत छन्दोंकी रचना और व्यवस्थितता ही देखी जाती है । अतः जो मनुष्यकी रचनाके समान ही एक विचित्र रचना में आबद्ध हैं वे अपौरुषेय नही हो सकते । अनादिपरम्परारूप हेतुसे वेदकी अतीन्द्रियार्थप्रतिपादकताकी सिद्धि करना उसी तरह कठिन है जिस तरह गाली-गलौज आदिकी प्रामाणिकता मानना । अन्ततः वेदके व्याख्यान के लिये भी अतीन्द्रियार्थदर्शी ही अन्तिम प्रमाण बन सकता है । विवादकी अवस्था में 'यह मेरा अर्थ है यह नहीं यह स्वयं शब्द तो बोलेंगे नहीं । यदि शब्द अर्थके मामले में स्वयं रोकनेवाला होता तो वेदकी व्याख्याओं में मतभेद नहीं होना चाहिये था ।
शब्द मात्रको नित्य मानकर वेदके नित्यत्वका समर्थन करना प्रतीतिविरुद्ध है; क्योंकि तालु आदिके व्यापार से पुद्गलपर्यायरूप शब्दकी उत्पत्ति ही प्रमाणसिद्ध है, अभिव्यक्ति नहीं । संकेतके लिये शब्दको नित्य मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि जैसे अनित्य घटादि पदार्थोंमें अमुक घड़ेके नष्ट होनेपर भी अन्य सदृश घड़ोंमें सादृश्यमूलक व्यवहार चल जाता है उसी तरह जिस शब्दमें संकेत ग्रहण किया है वह नष्ट (१) “प्रतिमन्वन्तरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते" - मत्स्यपु० १४५।५८ । (२) "सजन्ममरणर्षि गोत्रचरणादिनामश्रुतेः, अनेकपदसंहतिप्रतिनियमसन्दर्शनात् । फलार्थिपुरुषप्रवृत्तिविनिवृत्तिहेत्वात्मनाम् श्रुतेश्च मनुसूत्रवत् पुरुषकर्तृकैव श्रुतिः ॥"
- पात्रकेसरिस्तोत्र श्लो० १४ ।
Jain Education International
"
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org