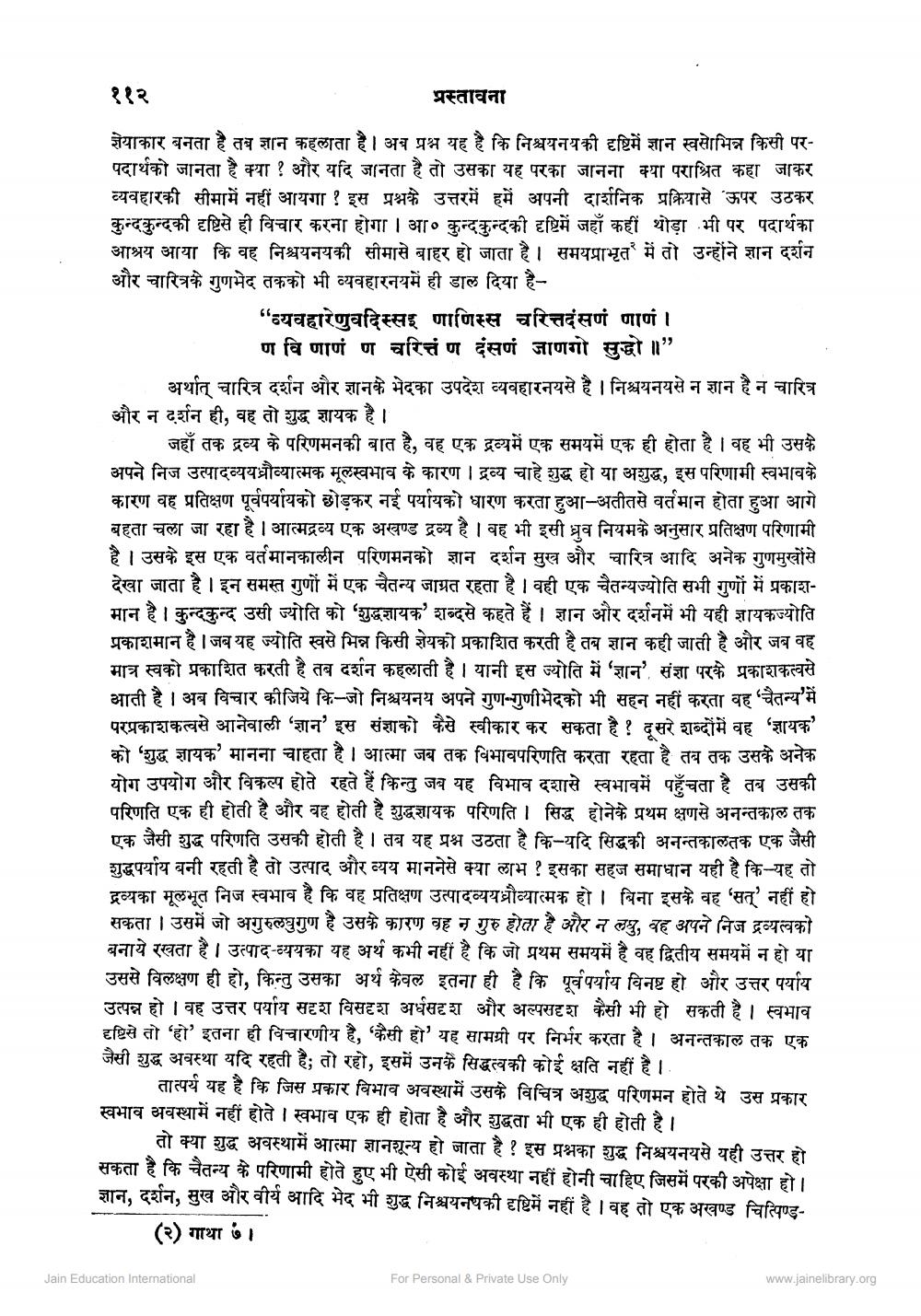________________
११२
प्रस्तावना
ज्ञेयाकार बनता है तब ज्ञान कहलाता है । अब प्रश्न यह है कि निश्चयनयकी दृष्टि में ज्ञान स्वसोभिन्न किसी परपदार्थको जानता है क्या ? और यदि जानता है तो उसका यह परका जानना क्या पराश्रित कहा जाकर व्यवहारकी सीमा में नहीं आयगा? इस प्रश्न उत्तरमें हमें अपनी दार्शनिक प्रक्रियासे ऊपर उठकर कुन्दकुन्दकी दृष्टिसे ही विचार करना होगा । आ० कुन्दकुन्दकी दृष्टिमें जहाँ कहीं थोड़ा भी पर पदार्थका आश्रय आया कि वह निश्चयनयकी सीमासे बाहर हो जाता है। समयप्राभृत में तो उन्होंने ज्ञान दर्शन और चारित्रके गुणभेद तकको भी व्यवहारनयमें ही डाल दिया है
"व्यवहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स चरित्तदसणं गाणं ।
ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥" अर्थात् चारित्र दर्शन और ज्ञानके भेदका उपदेश व्यवहारनयसे है । निश्चयनयसे न ज्ञान है न चारित्र और न दर्शन ही, वह तो शुद्ध ज्ञायक है ।
जहाँ तक द्रव्य के परिणमनकी बात है, वह एक द्रव्यमें एक समयमें एक ही होता है । वह भी उसके अपने निज उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक मूलस्वभाव के कारण । द्रव्य चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, इस परिणामी स्वभावके कारण वह प्रतिक्षण पूर्वपर्यायको छोड़कर नई पर्यायको धारण करता हुआ-अतीतसे वर्तमान होता हुआ आगे बहता चला जा रहा है । आत्मद्रव्य एक अखण्ड द्रव्य है । वह भी इसी ध्रव नियमके अनुसार प्रतिक्षण परिणामी है । उसके इस एक वर्तमानकालीन परिणमनको ज्ञान दर्शन सुख और चारित्र आदि अनेक गुणमुखोंसे देखा जाता है । इन समस्त गुणों में एक चैतन्य जाग्रत रहता है । वही एक चैतन्यज्योति सभी गुणों में प्रकाशमान है । कुन्दकुन्द उसी ज्योति को 'शुद्धज्ञायक' शब्दसे कहते हैं । ज्ञान और दर्शनमें भी यही ज्ञायकज्योति प्रकाशमान है । जब यह ज्योति स्वसे भिन्न किसी ज्ञेयको प्रकाशित करती है तब ज्ञान कही जाती है और जब वह मात्र स्वको प्रकाशित करती है तब दर्शन कहलाती है। यानी इस ज्योति में 'ज्ञान' संज्ञा परके प्रकाशकत्वसे आती है। अब विचार कीजिये कि-जो निश्चयनय अपने गुण-गुणीभेदको भी सहन नहीं करता वह 'चैतन्य में परप्रकाशकत्वसे आनेवाली 'ज्ञान' इस संज्ञाको कैसे स्वीकार कर सकता है ? दूसरे शब्दोंमें वह 'ज्ञायक' को 'शुद्ध ज्ञायक' मानना चाहता है । आत्मा जब तक विभावपरिणति करता रहता है तब तक उसके अनेक योग उपयोग और विकल्प होते रहते हैं किन्तु जब यह विभाव दशासे स्वभावमें पहुँचता है तब उसकी परिणति एक ही होती है और वह होती है शुद्धज्ञायक परिणति । सिद्ध होनेके प्रथम क्षणसे अनन्तकाल तक एक जैसी शुद्ध परिणति उसकी होती है । तब यह प्रश्न उठता है कि-यदि सिद्धकी अनन्तकालतक एक जैसी शुद्धपर्याय बनी रहती है तो उत्पाद और व्यय माननेसे क्या लाभ ? इसका सहज समाधान यही है कि-यह तो द्रव्यका मूलभूत निज स्वभाव है कि वह प्रतिक्षण उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक हो। बिना इसके वह 'सत्' नहीं हो सकता । उसमें जो अगुरुलघुगुण है उसके कारण वह न गुरु होता है और न लघु, वह अपने निज द्रव्यत्वको बनाये रखता है । उत्पाद-व्ययका यह अर्थ कभी नहीं है कि जो प्रथम समयमें है वह द्वितीय समयमें न हो या उससे विलक्षण ही हो, किन्तु उसका अर्थ केवल इतना ही है कि पूर्वपर्याय विनष्ट हो और उत्तर पर्याय उत्पन्न हो । वह उत्तर पर्याय सदृश विसदृश अर्धसदृश और अल्पसदृश कैसी भी हो सकती है। स्वभाव दृष्टिसे तो 'हो' इतना ही विचारणीय है, 'कैसी हो' यह सामग्री पर निर्भर करता है। अनन्तकाल तक एक जैसी शुद्ध अवस्था यदि रहती है तो रहो, इसमें उनके सिद्धत्वकी कोई क्षति नहीं है।
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विभाव अवस्थामें उसके विचित्र अशुद्ध परिणमन होते थे उस प्रकार स्वभाव अवस्थामें नहीं होते । खभाव एक ही होता है और शुद्धता भी एक ही होती है।
तो क्या शुद्ध अवस्थामें आत्मा ज्ञानशून्य हो जाता है ? इस प्रश्नका शुद्ध निश्चयनयसे यही उत्तर हो सकता है कि चैतन्य के परिणामी होते हुए भी ऐसी कोई अवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें परकी अपेक्षा हो। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि भेद भी शुद्ध निश्चयनथकी दृष्टिमें नहीं है । वह तो एक अखण्ड चित्पिण्ड
(२) गाथा ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org