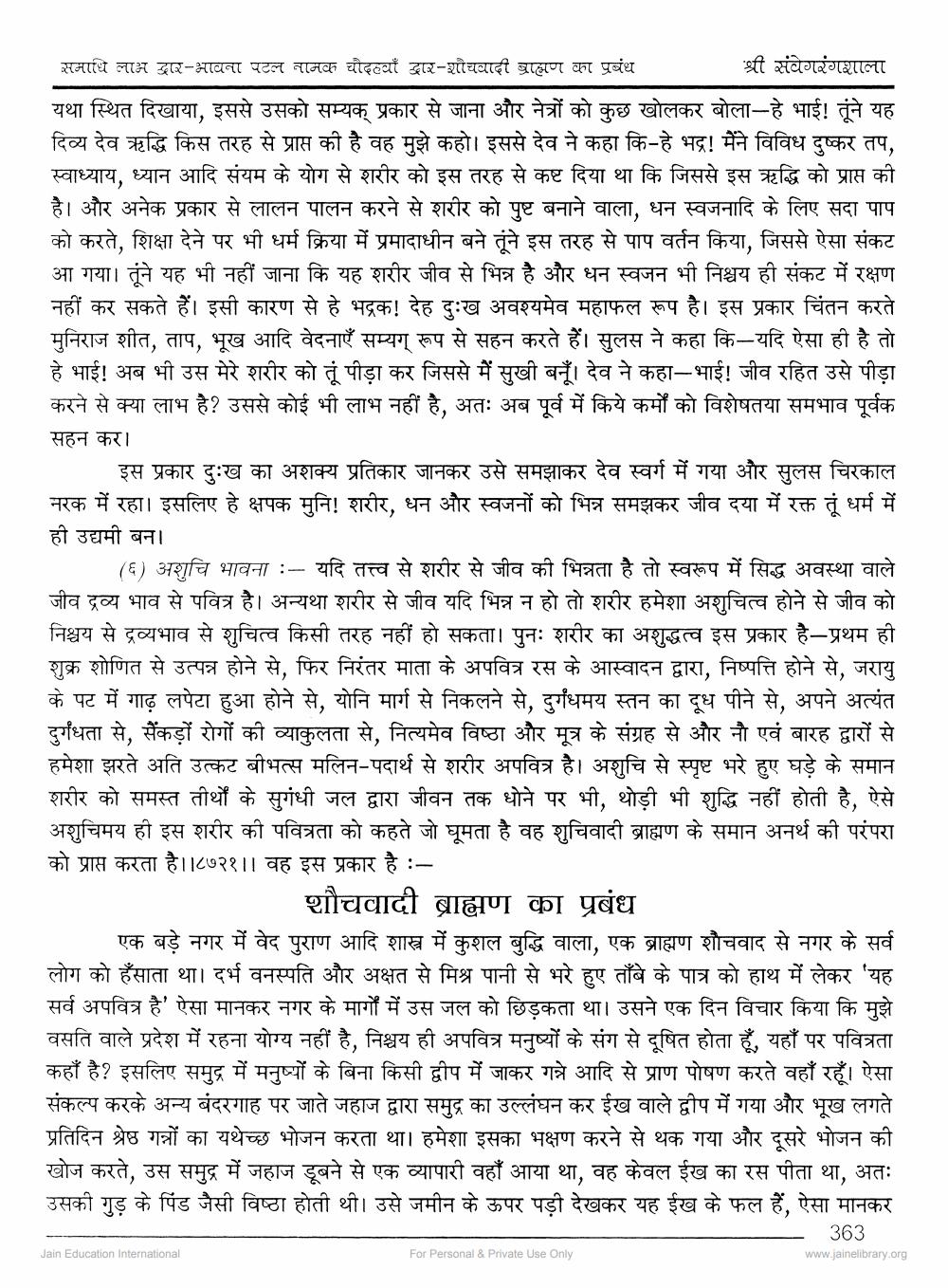________________
समाधि लाभ द्वार-भावना पटल नामक चौदहवाँ द्वार-शौचवादी ब्राह्मण का प्रबंध
श्री संवेगरंगशाला यथा स्थित दिखाया, इससे उसको सम्यक् प्रकार से जाना और नेत्रों को कुछ खोलकर बोला-हे भाई! तूंने यह दिव्य देव ऋद्धि किस तरह से प्राप्त की है वह मुझे कहो। इससे देव ने कहा कि-हे भद्र! मैंने विविध दुष्कर तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि संयम के योग से शरीर को इस तरह से कष्ट दिया था कि जिससे इस ऋद्धि को प्राप्त की है। और अनेक प्रकार से लालन पालन करने से शरीर को पुष्ट बनाने वाला, धन स्वजनादि के लिए सदा पाप को करते, शिक्षा देने पर भी धर्म क्रिया में प्रमादाधीन बने तूंने इस तरह से पाप वर्तन किया, जिससे ऐसा संकट आ गया। तूंने यह भी नहीं जाना कि यह शरीर जीव से भिन्न है और धन स्वजन भी निश्चय ही संकट में रक्षण नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हे भद्रक! देह दुःख अवश्यमेव महाफल रूप है। इस प्रकार चिंतन करते मुनिराज शीत, ताप, भूख आदि वेदनाएँ सम्यग् रूप से सहन करते हैं। सुलस ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो हे भाई! अब भी उस मेरे शरीर को तूं पीड़ा कर जिससे मैं सुखी बनूँ। देव ने कहा-भाई! जीव रहित उसे पीड़ा करने से क्या लाभ है? उससे कोई भी लाभ नहीं है, अतः अब पूर्व में किये कर्मों को विशेषतया समभाव पूर्वक सहन कर।
इस प्रकार दुःख का अशक्य प्रतिकार जानकर उसे समझाकर देव स्वर्ग में गया और सुलस चिरकाल नरक में रहा। इसलिए हे क्षपक मुनि! शरीर, धन और स्वजनों को भिन्न समझकर जीव दया में रक्त तूं धर्म में ही उद्यमी बन।
(६) अशुचि भावना :- यदि तत्त्व से शरीर से जीव की भिन्नता है तो स्वरूप में सिद्ध अवस्था वाले जीव द्रव्य भाव से पवित्र है। अन्यथा शरीर से जीव यदि भिन्न न हो तो शरीर हमेशा अशुचित्व होने से जीव को निश्चय से द्रव्यभाव से शुचित्व किसी तरह नहीं हो सकता। पुनः शरीर का अशुद्धत्व इस प्रकार है-प्रथम ही शक्र शोणित से उत्पन्न होने से. फिर निरंतर माता के अपवित्र रस के आस्वादन द्वारा. निष्पत्ति होने से. जराय के पट में गाढ़ लपेटा हुआ होने से, योनि मार्ग से निकलने से, दुर्गंधमय स्तन का दूध पीने से, अपने अत्यंत दुर्गंधता से, सैंकड़ों रोगों की व्याकुलता से, नित्यमेव विष्ठा और मूत्र के संग्रह से और नौ एवं बारह द्वारों से हमेशा झरते अति उत्कट बीभत्स मलिन-पदार्थ से शरीर अपवित्र है। अशुचि से स्पृष्ट भरे हुए घड़े के समान शरीर को समस्त तीर्थों के सुगंधी जल द्वारा जीवन तक धोने पर भी, थोड़ी भी शुद्धि नहीं होती है, ऐसे अशुचिमय ही इस शरीर की पवित्रता को कहते जो घूमता है वह शुचिवादी ब्राह्मण के समान अनर्थ की परंपरा को प्राप्त करता है।।८७२१ ।। वह इस प्रकार है :
शौचवादी ब्राह्मण का प्रबंध एक बड़े नगर में वेद पुराण आदि शास्त्र में कुशल बुद्धि वाला, एक ब्राह्मण शौचवाद से नगर के सर्व लोग को हँसाता था। दर्भ वनस्पति और अक्षत से मिश्र पानी से भरे हुए ताँबे के पात्र को हाथ में लेकर 'यह सर्व अपवित्र है' ऐसा मानकर नगर के मार्गों में उस जल को छिड़कता था। उसने एक दिन विचार किया कि मुझे वसति वाले प्रदेश में रहना योग्य नहीं है, निश्चय ही अपवित्र मनुष्यों के संग से दूषित होता हूँ, यहाँ पर पवित्रता कहाँ है? इसलिए समुद्र में मनुष्यों के बिना किसी द्वीप में जाकर गन्ने आदि से प्राण पोषण करते वहाँ रहूँ। ऐसा संकल्प करके अन्य बंदरगाह पर जाते जहाज द्वारा समुद्र का उल्लंघन कर ईख वाले द्वीप में गया और भूख लगते प्रतिदिन श्रेष्ठ गन्नों का यथेच्छ भोजन करता था। हमेशा इसका भक्षण करने से थक गया और दूसरे भोजन की खोज करते, उस समुद्र में जहाज डूबने से एक व्यापारी वहाँ आया था, वह केवल ईख का रस पीता था, अतः उसकी गुड़ के पिंड जैसी विष्ठा होती थी। उसे जमीन के ऊपर पड़ी देखकर यह ईख के फल हैं, ऐसा मानकर
363
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org