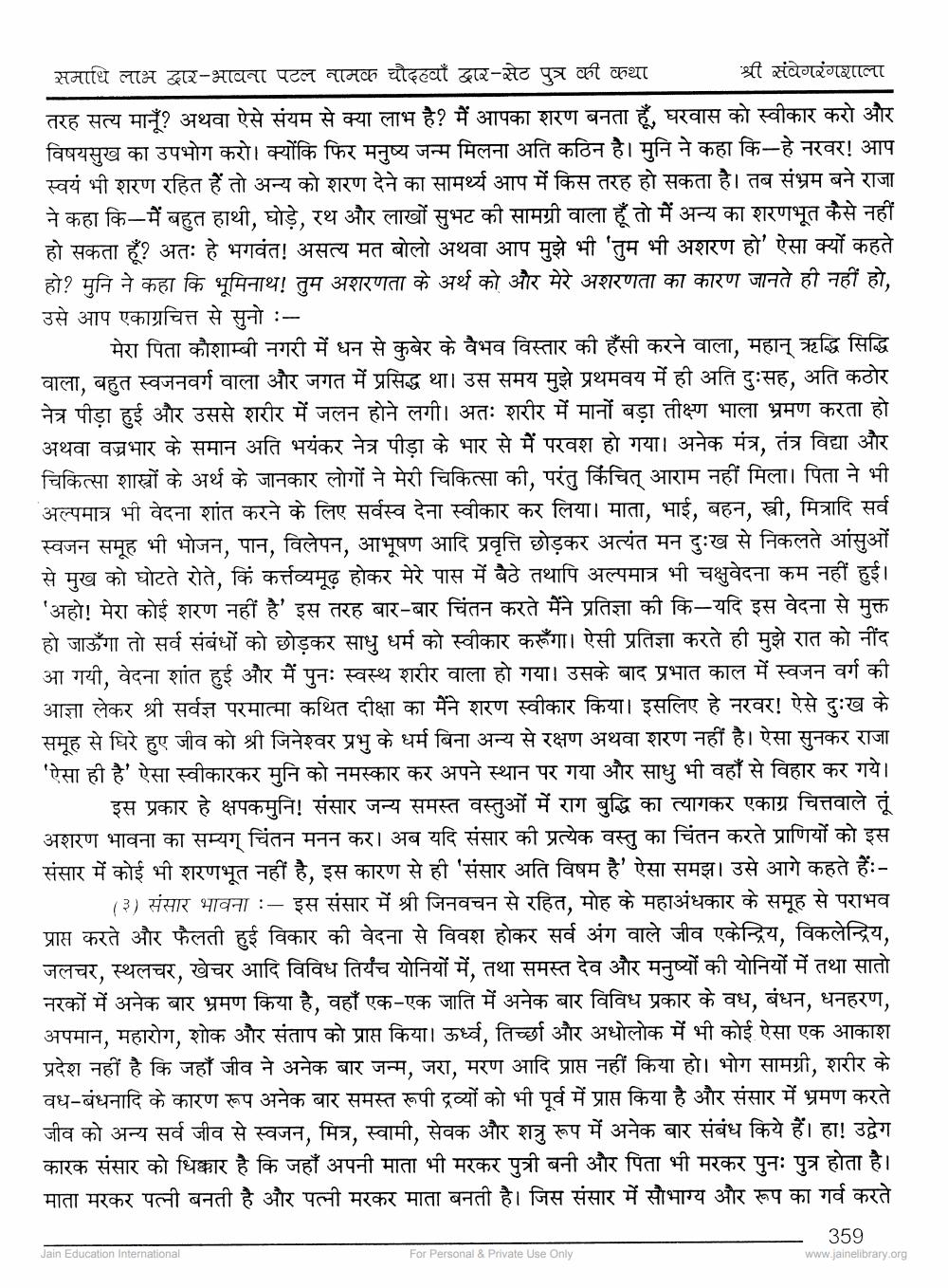________________
समाधि लाभ द्वार-भावना पटल नामक चौदहवाँ द्वार-सेट पुत्र की कथा
श्री संवेगरंगशाला तरह सत्य मानूँ? अथवा ऐसे संयम से क्या लाभ है? मैं आपका शरण बनता हूँ, घरवास को स्वीकार करो और विषयसुख का उपभोग करो। क्योंकि फिर मनुष्य जन्म मिलना अति कठिन है। मुनि ने कहा कि - हे नरवर ! आप स्वयं भी शरण रहित हैं तो अन्य को शरण देने का सामर्थ्य आप में किस तरह हो सकता है। तब संभ्रम बने राजा ने कहा कि- मैं बहुत हाथी, घोड़े, रथ और लाखों सुभट की सामग्री वाला हूँ तो मैं अन्य का शरणभूत कैसे नहीं हो सकता हूँ? अतः हे भगवंत ! असत्य मत बोलो अथवा आप मुझे भी 'तुम भी अशरण हो' ऐसा क्यों कहते हो ? मुनि ने कहा कि भूमिनाथ! तुम अशरणता के अर्थ को और मेरे अशरणता का कारण जानते ही नहीं हो, उसे आप एकाग्रचित्त से सुनो :
मेरा पिता कौशाम्बी नगरी में धन से कुबेर के वैभव विस्तार की हँसी करने वाला, महान् ऋद्धि सिद्धि वाला, बहुत स्वजनवर्ग वाला और जगत में प्रसिद्ध था । उस समय मुझे प्रथमवय में ही अति दुःसह, अति कठोर नेत्र पीड़ा हुई और उससे शरीर में जलन होने लगी। अतः शरीर में मानों बड़ा तीक्ष्ण भाला भ्रमण करता हो अथवा वज्रभार के समान अति भयंकर नेत्र पीड़ा के भार से मैं परवश हो गया। अनेक मंत्र, तंत्र विद्या और चिकित्सा शास्त्रों के अर्थ के जानकार लोगों ने मेरी चिकित्सा की, परंतु किंचित् आराम नहीं मिला। पिता ने भी अल्पमात्र भी वेदना शांत करने के लिए सर्वस्व देना स्वीकार कर लिया। माता, भाई, बहन, स्त्री, मित्रादि सर्व स्वजन समूह भी भोजन, पान, विलेपन, आभूषण आदि प्रवृत्ति छोड़कर अत्यंत मन दुःख निकलते आंसुओं से मुख को घोटते रोते, किं कर्त्तव्यमूढ़ होकर मेरे पास में बैठे तथापि अल्पमात्र भी चक्षुवेदना कम नहीं हुई। 'अहो ! मेरा कोई शरण नहीं है' इस तरह बार-बार चिंतन करते मैंने प्रतिज्ञा की कि - यदि इस वेदना से मुक्त हो जाऊँगा तो सर्व संबंधों को छोड़कर साधु धर्म को स्वीकार करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करते ही मुझे रात को नींद आ गयी, वेदना शांत हुई और मैं पुनः स्वस्थ शरीर वाला हो गया। उसके बाद प्रभात काल में स्वजन वर्ग की आज्ञा लेकर श्री सर्वज्ञ परमात्मा कथित दीक्षा का मैंने शरण स्वीकार किया । इसलिए हे नरवर ! ऐसे दुःख के समूह से घिरे हुए जीव को श्री जिनेश्वर प्रभु के धर्म बिना अन्य से रक्षण अथवा शरण नहीं है। ऐसा सुनकर राजा 'ऐसा ही है' ऐसा स्वीकारकर मुनि को नमस्कार कर अपने स्थान पर गया और साधु भी वहाँ से विहार कर गये । इस प्रकार हे क्षपकमुनि ! संसार जन्य समस्त वस्तुओं में राग बुद्धि का त्यागकर एकाग्र चित्तवाले तूं अशरण भावना का सम्यग् चिंतन मनन कर । अब यदि संसार प्रत्येक वस्तु का चिंतन करते प्राणियों को इस संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, इस कारण से ही 'संसार अति विषम है' ऐसा समझ। उसे आगे कहते हैं:( ३ ) संसार भावना :- इस संसार में श्री जिनवचन से रहित, मोह के महाअंधकार के समूह से पराभव प्राप्त करते और फैलती हुई विकार की वेदना से विवश होकर सर्व अंग वाले जीव एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, जलचर, स्थलचर, खेचर आदि विविध तिर्यंच योनियों में, तथा समस्त देव और मनुष्यों की योनियों में तथा सातो नरकों में अनेक बार भ्रमण किया है, वहाँ एक-एक जाति में अनेक बार विविध प्रकार के वध, बंधन, धनहरण, अपमान, महारोग, शोक और संताप प्राप्त किया। ऊर्ध्व, तिर्च्छा और अधोलोक में भी कोई ऐसा एक आकाश प्रदेश नहीं है कि जहाँ जीव ने अनेक बार जन्म, जरा, मरण आदि प्राप्त नहीं किया हो। भोग सामग्री, शरीर के वध-बंधनादि के कारण रूप अनेक बार समस्त रूपी द्रव्यों को भी पूर्व में प्राप्त किया है और संसार में भ्रमण करते जीव को अन्य सर्व जीव से स्वजन, मित्र, स्वामी, सेवक और शत्रु रूप में अनेक बार संबंध किये हैं। हा ! उद्वेग कारक संसार को धिक्कार है कि जहाँ अपनी माता भी मरकर पुत्री बनी और पिता भी मरकर पुनः पुत्र होता है। माता मरकर पत्नी बनती है और पत्नी मरकर माता बनती है। जिस संसार में सौभाग्य और रूप का गर्व करते
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
359 www.jainelibrary.org