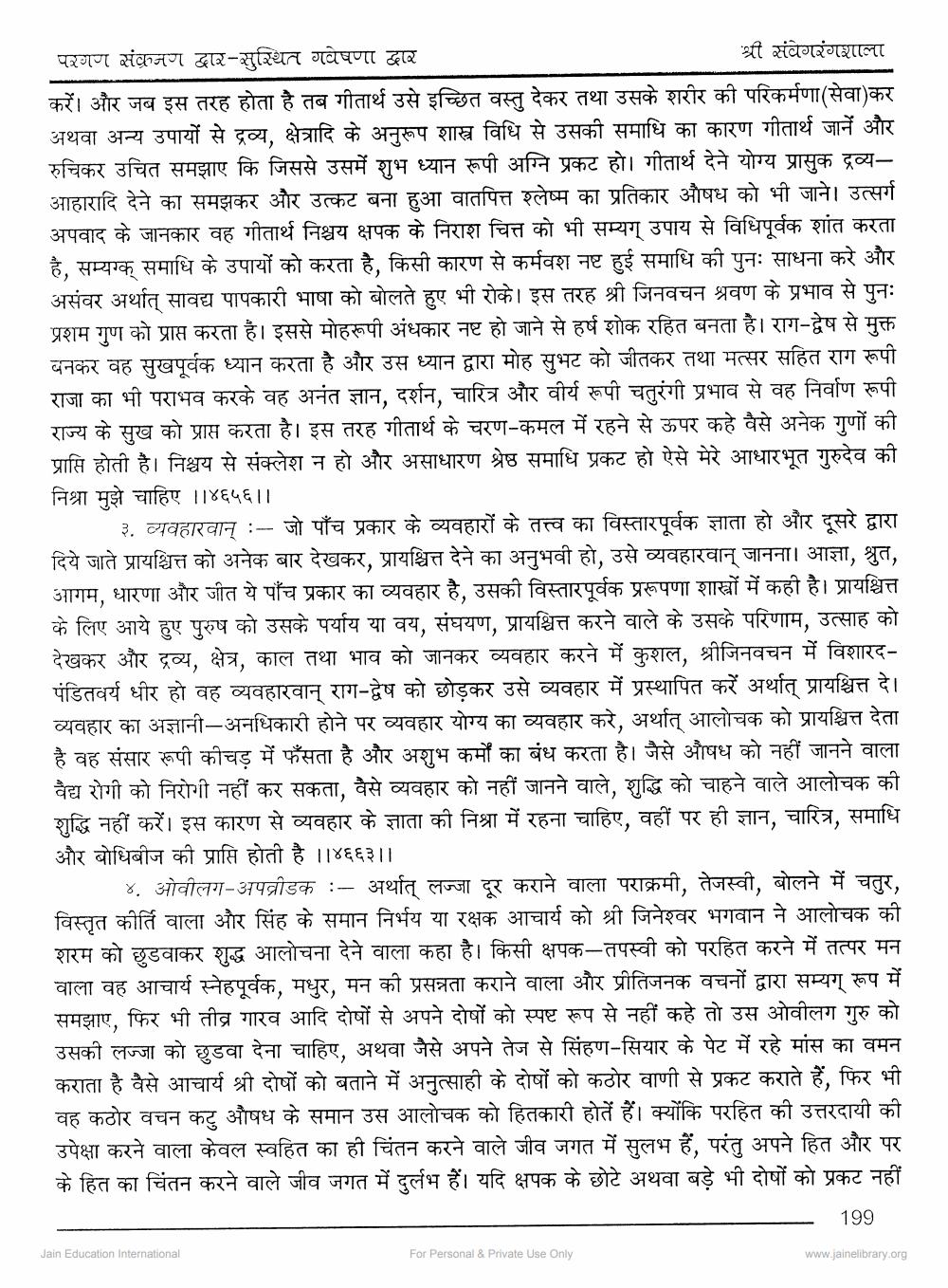________________
परगग संक्रजग द्वार-सुस्थित गवेषणा द्वार
श्री संवेगरंगशाला करें। और जब इस तरह होता है तब गीतार्थ उसे इच्छित वस्तु देकर तथा उसके शरीर की परिकर्मणा(सेवा)कर अथवा अन्य उपायों से द्रव्य, क्षेत्रादि के अनुरूप शास्त्र विधि से उसकी समाधि का कारण गीतार्थ जानें और रुचिकर उचित समझाए कि जिससे उसमें शुभ ध्यान रूपी अग्नि प्रकट हो। गीतार्थ देने योग्य प्रासुक द्रव्यआहारादि देने का समझकर और उत्कट बना हुआ वातपित्त श्लेष्म का प्रतिकार औषध को भी जाने। उत्सर्ग अपवाद के जानकार वह गीतार्थ निश्चय क्षपक के निराश चित्त को भी सम्यग् उपाय से विधिपूर्वक शांत करता है, सम्यग्क् समाधि के उपायों को करता है, किसी कारण से कर्मवश नष्ट हुई समाधि की पुनः साधना करे और असंवर अर्थात् सावध पापकारी भाषा को बोलते हुए भी रोके। इस तरह श्री जिनवचन श्रवण के प्रभाव से पुनः प्रशम गुण को प्राप्त करता है। इससे मोहरूपी अंधकार नष्ट हो जाने से हर्ष शोक रहित बनता है। राग-द्वेष से मुक्त बनकर वह सुखपूर्वक ध्यान करता है और उस ध्यान द्वारा मोह सुभट को जीतकर तथा मत्सर सहित राग रूपी राजा का भी पराभव करके वह अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य रूपी चतुरंगी प्रभाव से वह निर्वाण रूपी राज्य के सुख को प्राप्त करता है। इस तरह गीतार्थ के चरण-कमल में रहने से ऊपर कहे वैसे अनेक गुणों की प्राप्ति होती है। निश्चय से संक्लेश न हो और असाधारण श्रेष्ठ समाधि प्रकट हो ऐसे मेरे आधारभूत गुरुदेव की निश्रा मुझे चाहिए ।।४६५६।।
३. व्यवहारवान् :- जो पाँच प्रकार के व्यवहारों के तत्त्व का विस्तारपूर्वक ज्ञाता हो और दूसरे द्वारा दिये जाते प्रायश्चित्त को अनेक बार देखकर, प्रायश्चित्त देने का अनुभवी हो, उसे व्यवहारवान् जानना। आज्ञा, श्रुत, आगम, धारणा और जीत ये पाँच प्रकार का व्यवहार है, उसकी विस्तारपूर्वक प्ररूपणा शास्त्रों में कही है। प्रायश्चित्त के लिए आये हुए पुरुष को उसके पर्याय या वय, संघयण, प्रायश्चित्त करने वाले के उसके परिणाम, उत्साह को देखकर और द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव को जानकर व्यवहार करने में कशल. श्रीजिनवचन में विशारदपंडितवर्य धीर हो वह व्यवहारवान् राग-द्वेष को छोड़कर उसे व्यवहार में प्रस्थापित करें अर्थात् प्रायश्चित्त दे। व्यवहार का अज्ञानी-अनधिकारी होने पर व्यवहार योग्य का व्यवहार करे, अर्थात् आलोचक को प्रायश्चित्त देता है वह संसार रूपी कीचड़ में फंसता है और अशुभ कर्मों का बंध करता है। जैसे औषध को नहीं जानने वाला वैद्य रोगी को निरोगी नहीं कर सकता, वैसे व्यवहार को नहीं जानने वाले, शुद्धि को चाहने वाले आलोचक की शुद्धि नहीं करें। इस कारण से व्यवहार के ज्ञाता की निश्रा में रहना चाहिए, वहीं पर ही ज्ञान, चारित्र, समाधि और बोधिबीज की प्राप्ति होती है ।।४६६३।।
___४. ओवीलग-अपव्रीडक :- अर्थात् लज्जा दूर कराने वाला पराक्रमी, तेजस्वी, बोलने में चतुर, विस्तृत कीर्ति वाला और सिंह के समान निर्भय या रक्षक आचार्य को श्री जिनेश्वर भगवान ने आलोचक की शरम को छुडवाकर शुद्ध आलोचना देने वाला कहा है। किसी क्षपक-तपस्वी को परहित करने में तत्पर मन वाला वह आचार्य स्नेहपूर्वक, मधुर, मन की प्रसन्नता कराने वाला और प्रीतिजनक वचनों द्वारा सम्यग् रूप में समझाए, फिर भी तीव्र गारव आदि दोषों से अपने दोषों को स्पष्ट रूप से नहीं कहे तो उस ओवीलग गुरु को उसकी लज्जा को छुडवा देना चाहिए, अथवा जैसे अपने तेज से सिंहण-सियार के पेट में रहे मांस का वमन कराता है वैसे आचार्य श्री दोषों को बताने में अनुत्साही के दोषों को कठोर वाणी से प्रकट कराते हैं, फिर भी वह कठोर वचन कटु औषध के समान उस आलोचक को हितकारी होते हैं। क्योंकि परहित की उत्तरदायी की उपेक्षा करने वाला केवल स्वहित का ही चिंतन करने वाले जीव जगत में सुलभ हैं, परंतु अपने हित और पर के हित का चिंतन करने वाले जीव जगत में दुर्लभ हैं। यदि क्षपक के छोटे अथवा बड़े भी दोषों को प्रकट नहीं
- 199
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org