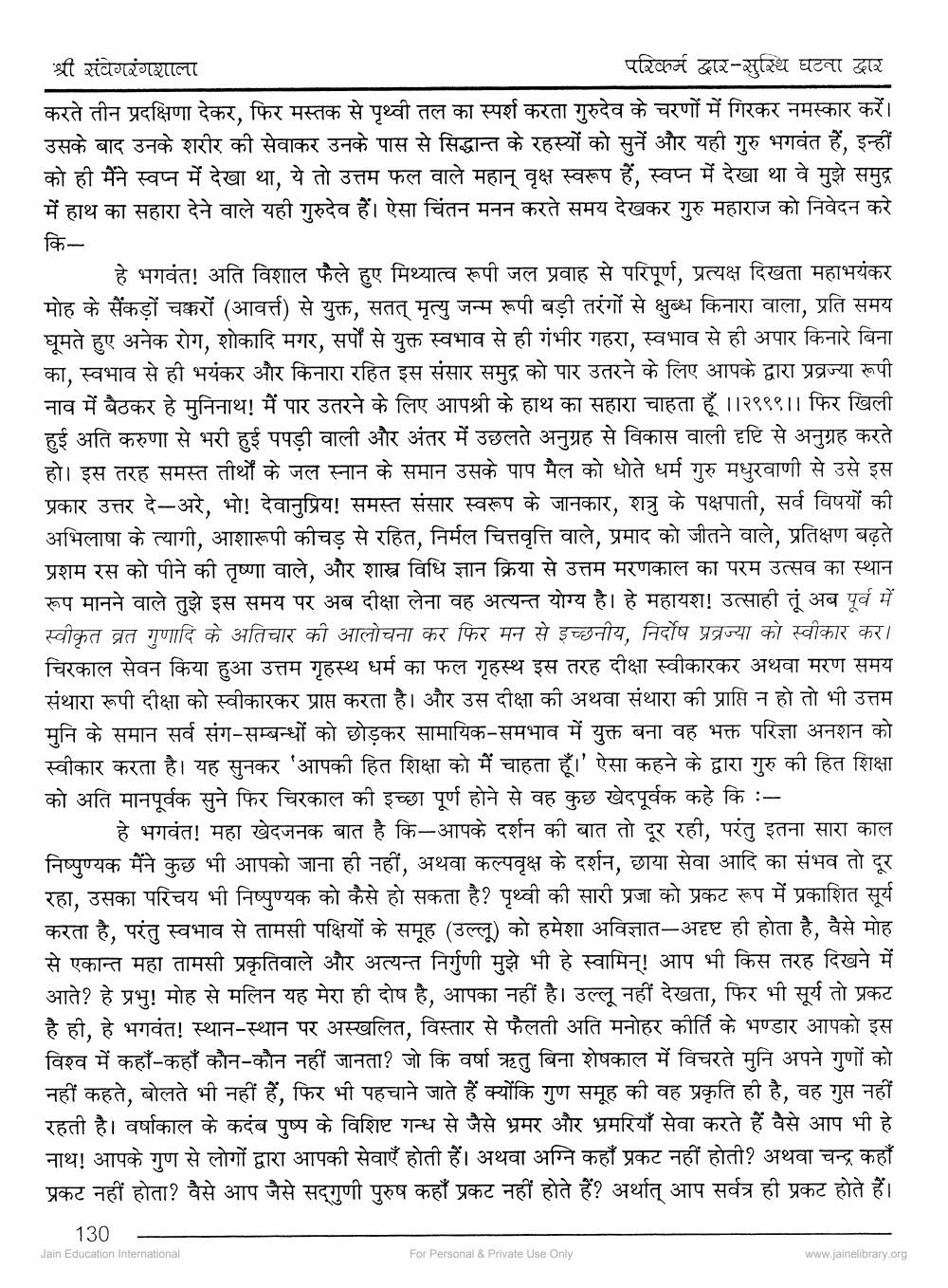________________
'श्री संवेगरंगशाला
परिकर्म द्वार-सुस्थि घटना द्वार करते तीन प्रदक्षिणा देकर, फिर मस्तक से पृथ्वी तल का स्पर्श करता गुरुदेव के चरणों में गिरकर नमस्कार करें। उसके बाद उनके शरीर की सेवाकर उनके पास से सिद्धान्त के रहस्यों को सुनें और यही गुरु भगवंत हैं, इन्हीं को ही मैंने स्वप्न में देखा था, ये तो उत्तम फल वाले महान् वृक्ष स्वरूप हैं, स्वप्न में देखा था वे मुझे समुद्र में हाथ का सहारा देने वाले यही गुरुदेव हैं। ऐसा चिंतन मनन करते समय देखकर गुरु महाराज को निवेदन करे कि
हे भगवंत! अति विशाल फैले हुए मिथ्यात्व रूपी जल प्रवाह से परिपूर्ण, प्रत्यक्ष दिखता महाभयंकर मोह के सैंकड़ों चक्करों (आवर्त) से युक्त, सतत् मृत्यु जन्म रूपी बड़ी तरंगों से क्षुब्ध किनारा वाला, प्रति समय घूमते हुए अनेक रोग, शोकादि मगर, सों से युक्त स्वभाव से ही गंभीर गहरा, स्वभाव से ही अपार किनारे बिना का, स्वभाव से ही भयंकर और किनारा रहित इस संसार समुद्र को पार उतरने के लिए आपके द्वारा प्रव्रज्या रूपी नाव में बैठकर हे मुनिनाथ! मैं पार उतरने के लिए आपश्री के हाथ का सहारा चाहता हूँ ।।२९९९।। फिर खिली हुई अति करुणा से भरी हुई पपड़ी वाली और अंतर में उछलते अनुग्रह से विकास वाली दृष्टि से अनुग्रह करते हो। इस तरह समस्त तीर्थों के जल स्नान के समान उसके पाप मैल को धोते धर्म गुरु मधुरवाणी से उसे इस प्रकार उत्तर दे-अरे, भो! देवानुप्रिय! समस्त संसार स्वरूप के जानकार, शत्रु के पक्षपाती, सर्व विषयों की अभिलाषा के त्यागी, आशारूपी कीचड़ से रहित, निर्मल चित्तवृत्ति वाले, प्रमाद को जीतने वाले, प्रतिक्षण बढ़ते प्रशम रस को पीने की तष्णा वाले. और शास्त्र विधि ज्ञान क्रिया से उत्तम मरणकाल का परम उत्सव का स्थान रूप मानने वाले तुझे इस समय पर अब दीक्षा लेना वह अत्यन्त योग्य है। हे महायश! उत्साही तूं अब पूर्व में स्वीकृत व्रत गुणादि के अतिचार की आलोचना कर फिर मन से इच्छनीय, निर्दोष प्रव्रज्या को स्वीकार कर। चिरकाल सेवन किया हुआ उत्तम गृहस्थ धर्म का फल गृहस्थ इस तरह दीक्षा स्वीकारकर अथवा मरण समय संथारा रूपी दीक्षा को स्वीकारकर प्राप्त करता है। और उस दीक्षा की अथवा संथारा की प्राप्ति न हो तो भी उत्तम मुनि के समान सर्व संग-सम्बन्धों को छोड़कर सामायिक-समभाव में युक्त बना वह भक्त परिज्ञा अनशन को स्वीकार करता है। यह सुनकर 'आपकी हित शिक्षा को मैं चाहता हूँ।' ऐसा कहने के द्वारा गुरु की हित शिक्षा को अति मानपूर्वक सुने फिर चिरकाल की इच्छा पूर्ण होने से वह कुछ खेदपूर्वक कहे कि :
हे भगवंत! महा खेदजनक बात है कि आपके दर्शन की बात तो दूर रही, परंतु इतना सारा काल निष्पुण्यक मैंने कुछ भी आपको जाना ही नहीं, अथवा कल्पवृक्ष के दर्शन, छाया सेवा आदि का संभव तो दूर रहा, उसका परिचय भी निष्पुण्यक को कैसे हो सकता है? पृथ्वी की सारी प्रजा को प्रकट रूप में प्रकाशित सूर्य करता है, परंतु स्वभाव से तामसी पक्षियों के समूह (उल्लू) को हमेशा अविज्ञात-अदृष्ट ही होता है, वैसे मोह से एकान्त महा तामसी प्रकृतिवाले और अत्यन्त निर्गुणी मुझे भी हे स्वामिन्! आप भी किस तरह दिखने में आते? हे प्रभु! मोह से मलिन यह मेरा ही दोष है, आपका नहीं है। उल्लू नहीं देखता, फिर भी सूर्य तो प्रकट है ही, हे भगवंत! स्थान-स्थान पर अस्खलित, विस्तार से फैलती अति मनोहर कीर्ति के भण्डार आपको इस विश्व में कहाँ-कहाँ कौन-कौन नहीं जानता? जो कि वर्षा ऋतु बिना शेषकाल में विचरते मुनि अपने गुणों को नहीं कहते, बोलते भी नहीं हैं, फिर भी पहचाने जाते हैं क्योंकि गुण समूह की वह प्रकृति ही है, वह गुप्त नहीं रहती है। वर्षाकाल के कदंब पुष्प के विशिष्ट गन्ध से जैसे भ्रमर और भ्रमरियाँ सेवा करते हैं वैसे आप भी हे नाथ! आपके गुण से लोगों द्वारा आपकी सेवाएँ होती हैं। अथवा अग्नि कहाँ प्रकट नहीं होती? अथवा चन्द्र कहाँ प्रकट नहीं होता? वैसे आप जैसे सद्गुणी पुरुष कहाँ प्रकट नहीं होते हैं? अर्थात् आप सर्वत्र ही प्रकट होते हैं।
130 Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org