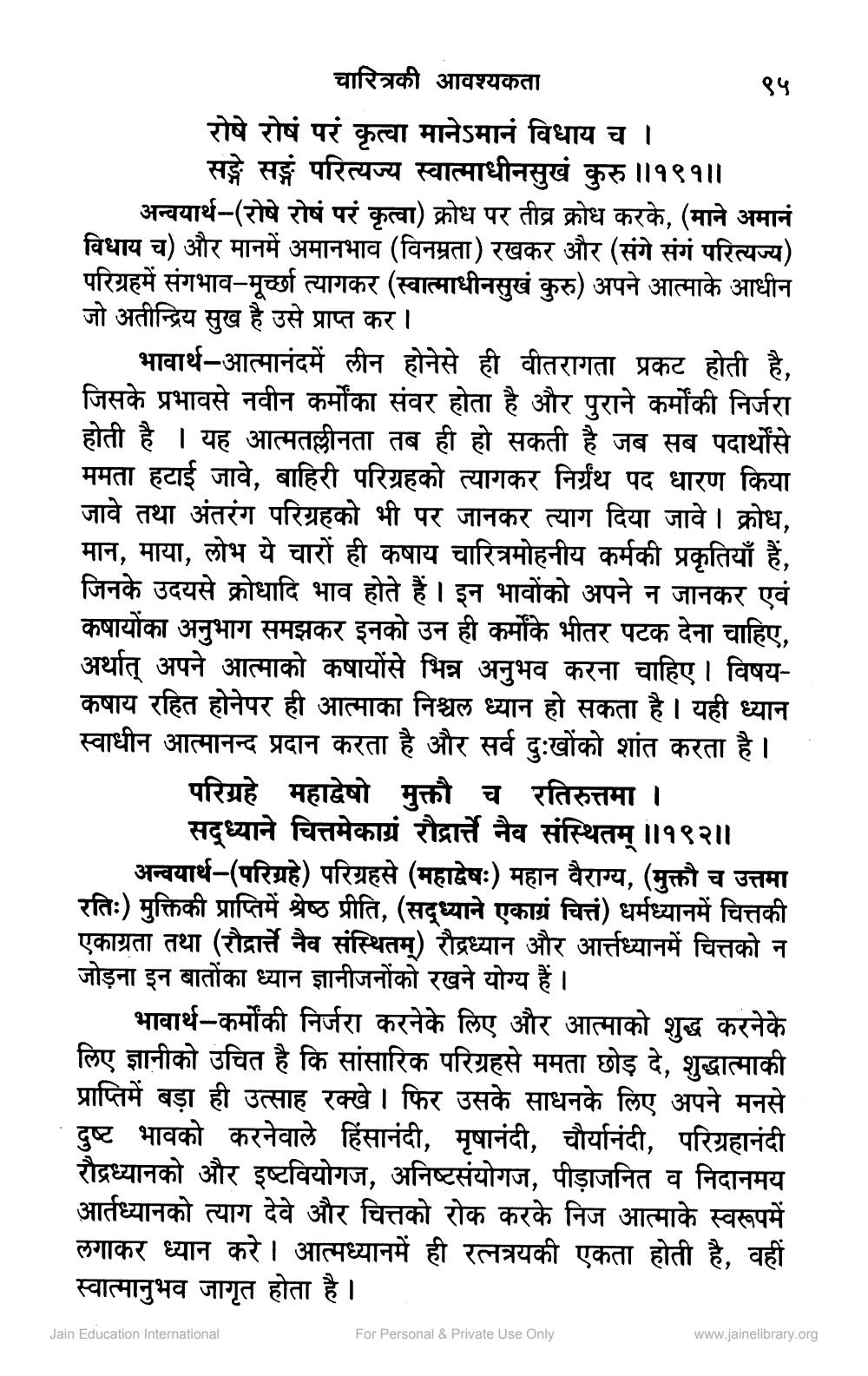________________
चारित्रकी आवश्यकता रोषे रोषं परं कृत्वा मानेऽमानं विधाय च ।
सङ्गे सङ्गं परित्यज्य स्वात्माधीनसुखं कुरु ॥१९१॥ अन्वयार्थ-(रोषे रोषं परं कृत्वा) क्रोध पर तीव्र क्रोध करके, (माने अमानं विधाय च) और मानमें अमानभाव (विनम्रता) रखकर और (संगे संगं परित्यज्य) परिग्रहमें संगभाव-मूर्छा त्यागकर (स्वात्माधीनसुखं कुरु) अपने आत्माके आधीन जो अतीन्द्रिय सुख है उसे प्राप्त कर ।
भावार्थ-आत्मानंदमें लीन होनेसे ही वीतरागता प्रकट होती है, जिसके प्रभावसे नवीन कर्मोंका संवर होता है और पुराने कर्मोंकी निर्जरा होती है । यह आत्मतल्लीनता तब ही हो सकती है जब सब पदार्थोंसे ममता हटाई जावे, बाहिरी परिग्रहको त्यागकर निग्रंथ पद धारण किया जावे तथा अंतरंग परिग्रहको भी पर जानकर त्याग दिया जावे । क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों ही कषाय चारित्रमोहनीय कर्मकी प्रकृतियाँ हैं, जिनके उदयसे क्रोधादि भाव होते हैं। इन भावोंको अपने न जानकर एवं कषायोंका अनुभाग समझकर इनको उन ही कर्मोंके भीतर पटक देना चाहिए, अर्थात् अपने आत्माको कषायोंसे भिन्न अनुभव करना चाहिए। विषयकषाय रहित होनेपर ही आत्माका निश्चल ध्यान हो सकता है। यही ध्यान स्वाधीन आत्मानन्द प्रदान करता है और सर्व दुःखोंको शांत करता है।
परिग्रहे महाद्वेषो मुक्तौ च रतिरुत्तमा ।
सद्ध्याने चित्तमेकाग्रं रौद्रार्ते नैव संस्थितम् ॥१९२॥ अन्वयार्थ-(परिग्रहे) परिग्रहसे (महाद्वेषः) महान वैराग्य, (मुक्तौ च उत्तमा रतिः) मुक्तिकी प्राप्तिमें श्रेष्ठ प्रीति, (सध्याने एकाग्रं चित्तं) धर्मध्यानमें चित्तकी एकाग्रता तथा (रौद्रार्ते नैव संस्थितम्) रौद्रध्यान और आर्त्तध्यानमें चित्तको न जोड़ना इन बातोंका ध्यान ज्ञानीजनोंको रखने योग्य हैं।
भावार्थ-कर्मोंकी निर्जरा करनेके लिए और आत्माको शुद्ध करनेके लिए ज्ञानीको उचित है कि सांसारिक परिग्रहसे ममता छोड़ दे, शुद्धात्माकी प्राप्तिमें बड़ा ही उत्साह रक्खे । फिर उसके साधनके लिए अपने मनसे दुष्ट भावको करनेवाले हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी रौद्रध्यानको और इष्टवियोगज, अनिष्टसंयोगज, पीड़ाजनित व निदानमय आर्तध्यानको त्याग देवे और चित्तको रोक करके निज आत्माके स्वरूपमें लगाकर ध्यान करे। आत्मध्यानमें ही रत्नत्रयकी एकता होती है, वहीं स्वात्मानुभव जागृत होता है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org