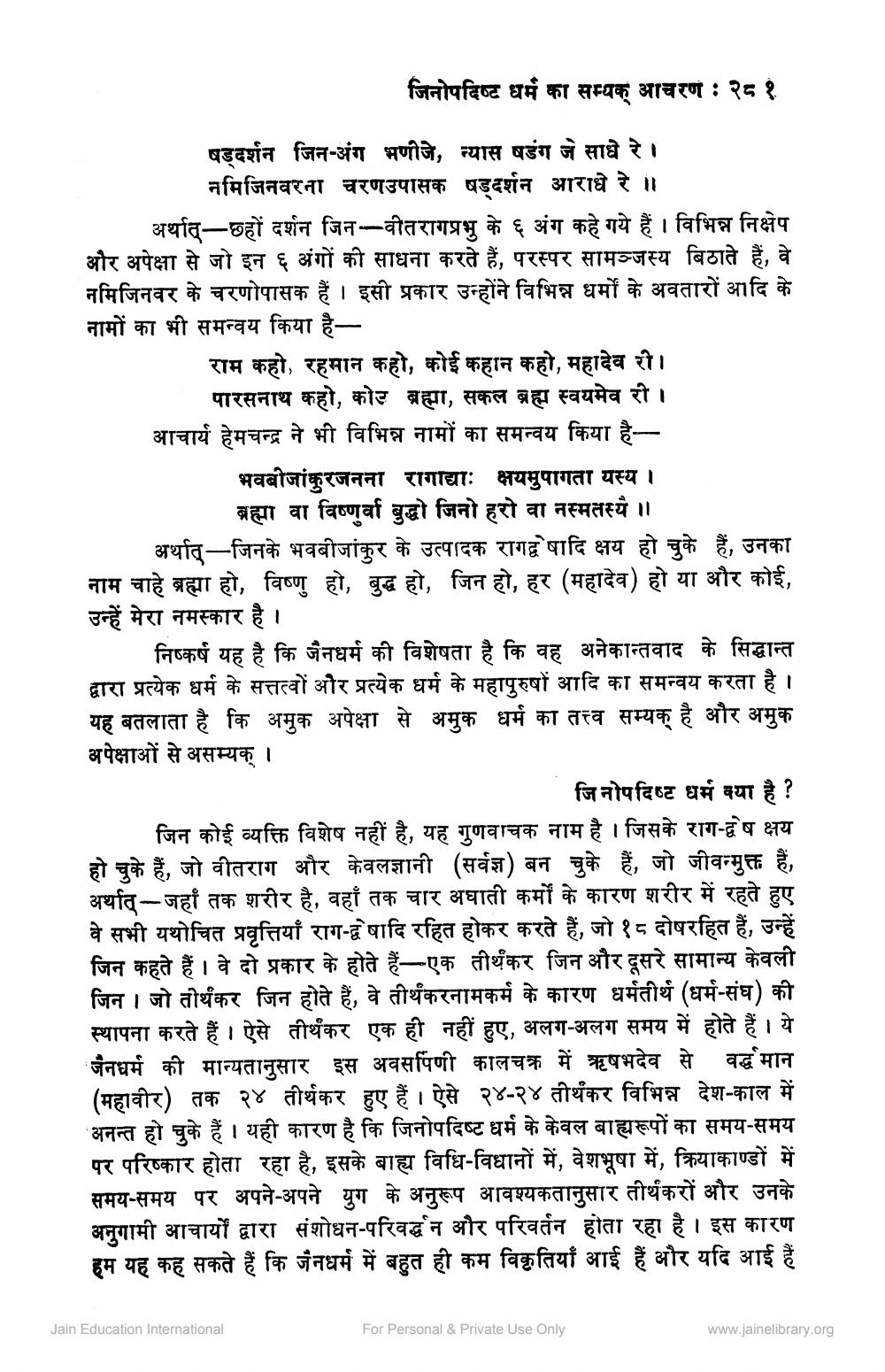________________
जिनोपदिष्ट धर्म का सम्यक् आचरण : २८१
षड्दर्शन जिन-अंग भणीजे, न्यास षडंग जे साधे रे ।
नमिजिनवरना चरणउपासक षड्दर्शन आराधे रे ॥ अर्थात्-छहों दर्शन जिन-वीतरागप्रभु के ६ अंग कहे गये हैं । विभिन्न निक्षेप और अपेक्षा से जो इन ६ अंगों की साधना करते हैं, परस्पर सामञ्जस्य बिठाते हैं, वे नमिजिनवर के चरणोपासक हैं । इसी प्रकार उन्होंने विभिन्न धर्मों के अवतारों आदि के नामों का भी समन्वय किया है
राम कहो, रहमान कहो, कोई कहान कहो, महादेव री।
पारसनाथ कहो, कोर ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री। आचार्य हेमचन्द्र ने भी विभिन्न नामों का समन्वय किया है
भवबीजांकुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा बुद्धो जिनो हरो वा नस्मतस्यै ॥ अर्थात्-जिनके भवबीजांकुर के उत्पादक रागद्वेषादि क्षय हो चुके हैं, उनका नाम चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, बुद्ध हो, जिन हो, हर (महादेव) हो या और कोई, उन्हें मेरा नमस्कार है।
निष्कर्ष यह है कि जैनधर्म की विशेषता है कि वह अनेकान्तवाद के सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक धर्म के सत्तत्वों और प्रत्येक धर्म के महापुरुषों आदि का समन्वय करता है । यह बतलाता है कि अमुक अपेक्षा से अमुक धर्म का तत्त्व सम्यक् है और अमुक अपेक्षाओं से असम्यक् ।
जिनोपदिष्ट धर्म क्या है ? जिन कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यह गुणवाचक नाम है । जिसके राग-द्वेष क्षय हो चुके हैं, जो वीतराग और केवलज्ञानी (सर्वज्ञ) बन चुके हैं, जो जीवन्मुक्त हैं, अर्थात्-जहाँ तक शरीर है, वहाँ तक चार अघाती कर्मों के कारण शरीर में रहते हुए वे सभी यथोचित प्रवृत्तियाँ राग-द्वेषादि रहित होकर करते हैं, जो १८ दोषरहित हैं, उन्हें जिन कहते हैं । वे दो प्रकार के होते हैं-एक तीर्थंकर जिन और दूसरे सामान्य केवली जिन । जो तीर्थंकर जिन होते हैं, वे तीर्थंकरनामकर्म के कारण धर्मतीर्थ (धर्म-संघ) की स्थापना करते हैं। ऐसे तीर्थंकर एक ही नहीं हुए, अलग-अलग समय में होते हैं। ये जैनधर्म की मान्यतानुसार इस अवसर्पिणी कालचक्र में ऋषभदेव से वर्द्धमान (महावीर) तक २४ तीर्थकर हुए हैं । ऐसे २४-२४ तीर्थंकर विभिन्न देश-काल में अनन्त हो चुके हैं । यही कारण है कि जिनोपदिष्ट धर्म के केवल बाह्यरूपों का समय-समय पर परिष्कार होता रहा है, इसके बाह्य विधि-विधानों में, वेशभूषा में, क्रियाकाण्डों में समय-समय पर अपने-अपने युग के अनुरूप आवश्यकतानुसार तीर्थंकरों और उनके अनुगामी आचार्यों द्वारा संशोधन-परिवर्द्धन और परिवर्तन होता रहा है । इस कारण हम यह कह सकते हैं कि जैनधर्म में बहुत ही कम विकृतियाँ आई हैं और यदि आई हैं
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org