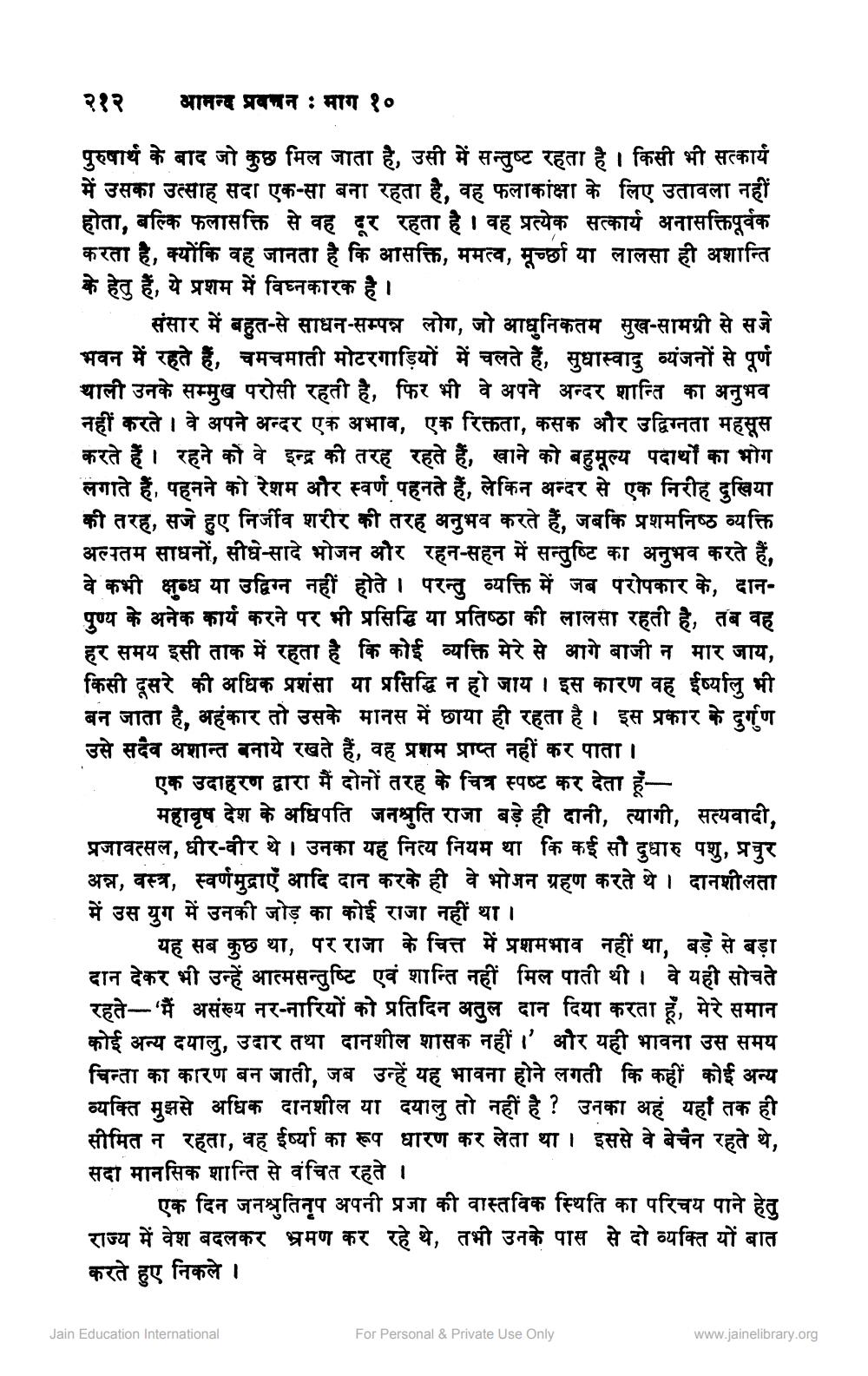________________
२१२
आनन्द प्रवचन : माग १०
पुरुषार्थ के बाद जो कुछ मिल जाता है, उसी में सन्तुष्ट रहता है । किसी भी सत्कार्य में उसका उत्साह सदा एक-सा बना रहता है, वह फलाकांक्षा के लिए उतावला नहीं होता, बल्कि फलासक्ति से वह दूर रहता है । वह प्रत्येक सत्कार्य अनासक्तिपूर्वक करता है, क्योंकि वह जानता है कि आसक्ति, ममत्व, मूर्छा या लालसा ही अशान्ति के हेतु हैं, ये प्रशम में विघ्नकारक है।
संसार में बहुत-से साधन-सम्पन्न लोग, जो आधुनिकतम सुख-सामग्री से सजे भवन में रहते हैं, चमचमाती मोटरगाड़ियों में चलते हैं, सुधास्वादु व्यंजनों से पूर्ण थाली उनके सम्मुख परोसी रहती है, फिर भी वे अपने अन्दर शान्ति का अनुभव नहीं करते। वे अपने अन्दर एक अभाव, एक रिक्तता, कसक और उद्विग्नता महसूस करते हैं। रहने को वे इन्द्र की तरह रहते हैं, खाने को बहुमूल्य पदार्थों का भोग लगाते हैं, पहनने को रेशम और स्वर्ण पहनते हैं, लेकिन अन्दर से एक निरीह दुखिया की तरह, सजे हुए निर्जीव शरीर की तरह अनुभव करते हैं, जबकि प्रशमनिष्ठ व्यक्ति अल्पतम साधनों, सीधे-सादे भोजन और रहन-सहन में सन्तुष्टि का अनुभव करते हैं, वे कभी क्षुब्ध या उद्विग्न नहीं होते। परन्तु व्यक्ति में जब परोपकार के, दानपुण्य के अनेक कार्य करने पर भी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा की लालसा रहती है, तब वह हर समय इसी ताक में रहता है कि कोई व्यक्ति मेरे से आगे बाजी न मार जाय, किसी दूसरे की अधिक प्रशंसा या प्रसिद्धि न हो जाय । इस कारण वह ईर्ष्यालु भी बन जाता है, अहंकार तो उसके मानस में छाया ही रहता है। इस प्रकार के दुर्गुण उसे सदैव अशान्त बनाये रखते हैं, वह प्रशम प्राप्त नहीं कर पाता।
एक उदाहरण द्वारा मैं दोनों तरह के चित्र स्पष्ट कर देता हूँ
महावृष देश के अधिपति जनश्रुति राजा बड़े ही दानी, त्यागी, सत्यवादी, प्रजावत्सल, धीर-वीर थे। उनका यह नित्य नियम था कि कई सौ दुधारु पशु, प्रचुर अन्न, वस्त्र, स्वर्णमुद्राएँ आदि दान करके ही वे भोजन ग्रहण करते थे। दानशीलता में उस युग में उनकी जोड़ का कोई राजा नहीं था।
यह सब कुछ था, पर राजा के चित्त में प्रशमभाव नहीं था, बड़े से बड़ा दान देकर भी उन्हें आत्मसन्तुष्टि एवं शान्ति नहीं मिल पाती थी। वे यही सोचते रहते- 'मैं असंख्य नर-नारियों को प्रतिदिन अतुल दान दिया करता हूँ, मेरे समान कोई अन्य दयालु, उदार तथा दानशील शासक नहीं।' और यही भावना उस समय चिन्ता का कारण बन जाती, जब उन्हें यह भावना होने लगती कि कहीं कोई अन्य व्यक्ति मुझसे अधिक दानशील या दयालु तो नहीं है ? उनका अहं यहां तक ही सीमित न रहता, वह ईर्ष्या का रूप धारण कर लेता था। इससे वे बेचैन रहते थे, सदा मानसिक शान्ति से वंचित रहते ।
एक दिन जनश्रुतिनप अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का परिचय पाने हेतु राज्य में वेश बदलकर भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके पास से दो व्यक्ति यों बात करते हुए निकले।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org