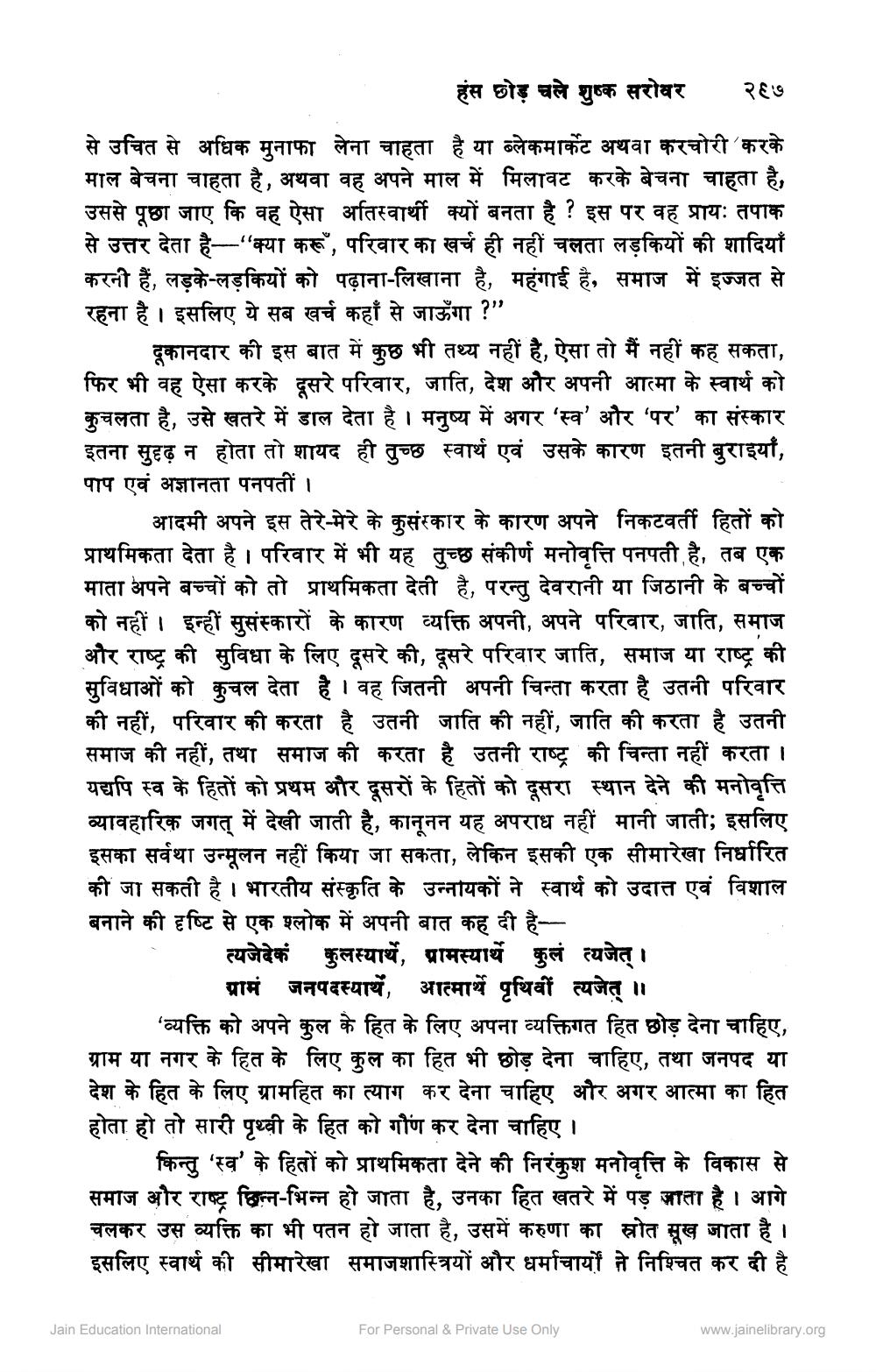________________
हंस छोड़ चले शुष्क सरोवर
२६७
से उचित से अधिक मुनाफा लेना चाहता है या ब्लेकमार्केट अथवा करचोरी करके माल बेचना चाहता है, अथवा वह अपने माल में मिलावट करके बेचना चाहता है, उससे पूछा जाए कि वह ऐसा अतिस्वार्थी क्यों बनता है ? इस पर वह प्रायः तपाक से उत्तर देता है- "क्या करूँ, परिवार का खर्च ही नहीं चलता लड़कियों की शादियाँ करनी हैं, लड़के-लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना है, महंगाई है, समाज में इज्जत से रहना है। इसलिए ये सब खर्च कहाँ से जाऊँगा ?"
__ दूकानदार की इस बात में कुछ भी तथ्य नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी वह ऐसा करके दूसरे परिवार, जाति, देश और अपनी आत्मा के स्वार्थ को कुचलता है, उसे खतरे में डाल देता है। मनुष्य में अगर 'स्व' और 'पर' का संस्कार इतना सुदृढ़ न होता तो शायद ही तुच्छ स्वार्थ एवं उसके कारण इतनी बुराइयाँ, पाप एवं अज्ञानता पनपतीं।
आदमी अपने इस तेरे-मेरे के कुसंस्कार के कारण अपने निकटवर्ती हितों को प्राथमिकता देता है। परिवार में भी यह तुच्छ संकीर्ण मनोवृत्ति पनपती है, तब एक माता अपने बच्चों को तो प्राथमिकता देती है, परन्तु देवरानी या जिठानी के बच्चों को नहीं। इन्हीं सुसंस्कारों के कारण व्यक्ति अपनी, अपने परिवार, जाति, समाज और राष्ट्र की सुविधा के लिए दूसरे की, दूसरे परिवार जाति, समाज या राष्ट्र की सुविधाओं को कुचल देता है । वह जितनी अपनी चिन्ता करता है उतनी परिवार की नहीं, परिवार की करता है उतनी जाति की नहीं, जाति की करता है उतनी समाज की नहीं, तथा समाज की करता है उतनी राष्ट्र की चिन्ता नहीं करता । यद्यपि स्व के हितों को प्रथम और दूसरों के हितों को दूसरा स्थान देने की मनोवृत्ति व्यावहारिक जगत् में देखी जाती है, कानूनन यह अपराध नहीं मानी जाती; इसलिए इसका सर्वथा उन्मूलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी एक सीमारेखा निर्धारित की जा सकती है। भारतीय संस्कृति के उन्नायकों ने स्वार्थ को उदात्त एवं विशाल बनाने की दृष्टि से एक श्लोक में अपनी बात कह दी है
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।
ग्रामं जनपदस्यायें, आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ 'व्यक्ति को अपने कुल के हित के लिए अपना व्यक्तिगत हित छोड़ देना चाहिए, ग्राम या नगर के हित के लिए कुल का हित भी छोड़ देना चाहिए, तथा जनपद या देश के हित के लिए ग्रामहित का त्याग कर देना चाहिए और अगर आत्मा का हित होता हो तो सारी पृथ्वी के हित को गौण कर देना चाहिए।
किन्तु 'स्व' के हितों को प्राथमिकता देने की निरंकुश मनोवृत्ति के विकास से समाज और राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जाता है, उनका हित खतरे में पड़ जाता है। आगे चलकर उस व्यक्ति का भी पतन हो जाता है, उसमें करुणा का स्रोत सूख जाता है। इसलिए स्वार्थ की सीमारेखा समाजशास्त्रियों और धर्माचार्यों ने निश्चित कर दी है
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org