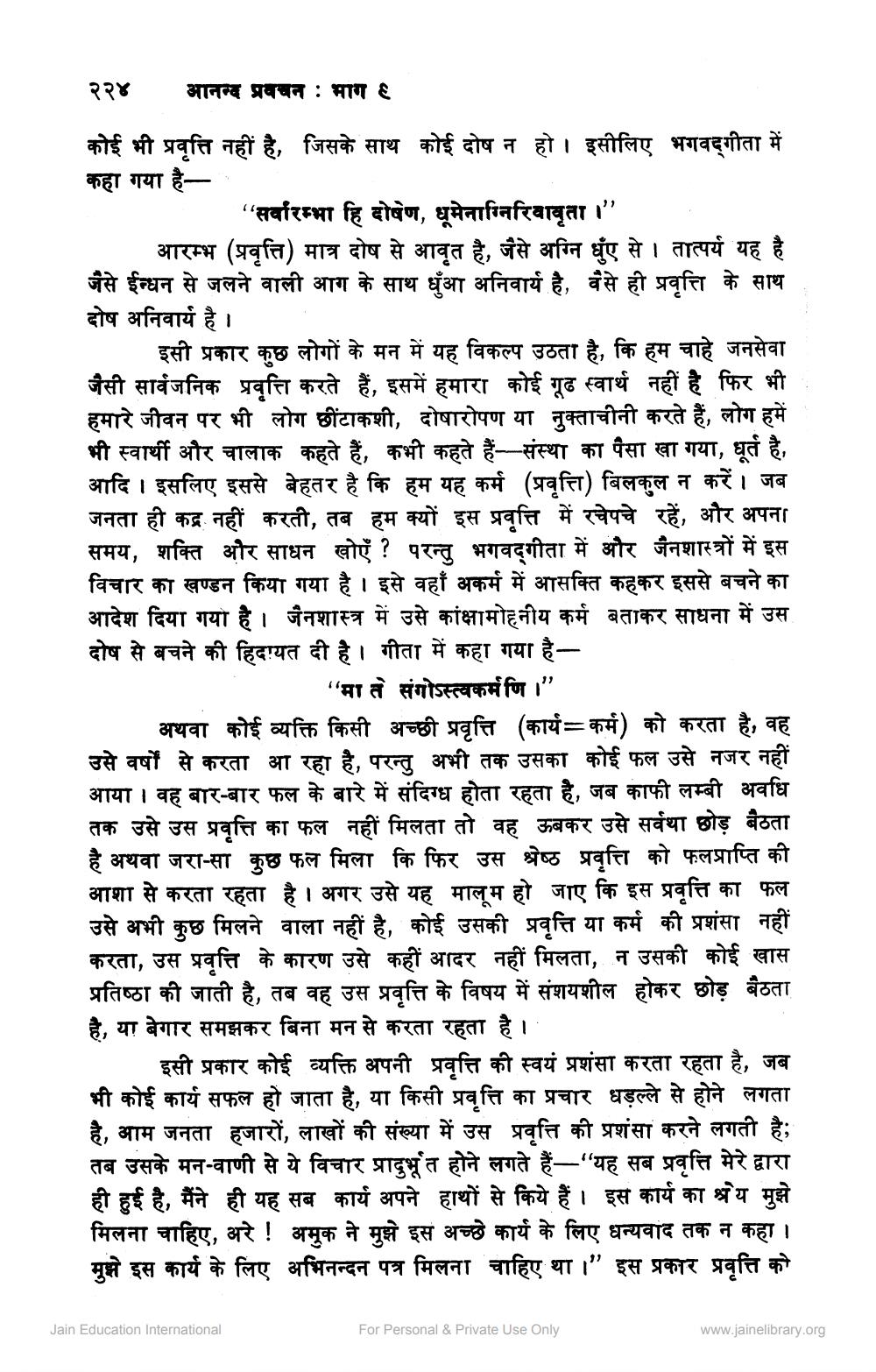________________
२२४ आनन्द प्रवचन : भाग ६
कोई भी प्रवृत्ति नहीं है, जिसके साथ कोई दोष न हो। इसीलिए भगवद्गीता में कहा गया है
"सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृता ।"
आरम्भ ( प्रवृत्ति) मात्र दोष से आवृत है, जैसे अग्नि धुंए से । तात्पर्य यह है जैसे ईन्धन से जलने वाली आग के साथ धुँआ अनिवार्य है, वैसे ही प्रवृत्ति के साथ दोष अनिवार्य है ।
इसी प्रकार कुछ लोगों के मन में यह विकल्प उठता है, कि हम चाहे जनसेवा जैसी सार्वजनिक प्रवृत्ति करते हैं, इसमें हमारा कोई गूढ स्वार्थ नहीं है फिर भी हमारे जीवन पर भी लोग छींटाकशी, दोषारोपण या नुक्ताचीनी करते हैं, लोग हमें भी स्वार्थी और चालाक कहते हैं, कभी कहते हैं -- संस्था का पैसा खा गया, धूर्त है, आदि । इसलिए इससे बेहतर है कि हम यह कर्म ( प्रवृत्ति) बिलकुल न करें । जब जनता ही कद्र नहीं करती, तब हम क्यों इस प्रवृत्ति में रचेपचे रहें, और अपना समय, शक्ति और साधन खोएँ ? परन्तु भगवद्गीता में और जैनशास्त्रों में इस विचार का खण्डन किया गया है । इसे वहाँ अकर्म में आसक्ति कहकर इससे बचने का आदेश दिया गया है । जैनशास्त्र में उसे कांक्षामोहनीय कर्म बताकर साधना में उस दोष से बचने की हिदायत दी है। गीता में कहा गया है
" मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।”
अथवा कोई व्यक्ति किसी अच्छी प्रवृत्ति ( कार्य = कर्म) को करता है, वह उसे वर्षों से करता आ रहा है, परन्तु अभी तक उसका कोई फल उसे नजर नहीं आया । वह बार-बार फल के बारे में संदिग्ध होता रहता है, जब काफी लम्बी अवधि तक उसे उस प्रवृत्ति का फल नहीं मिलता तो वह ऊबकर उसे सर्वथा छोड़ बैठता है अथवा जरा-सा कुछ फल मिला कि फिर उस श्रेष्ठ प्रवृत्ति को फलप्राप्ति की आशा से करता रहता है । अगर उसे यह मालूम हो जाए कि इस प्रवृत्ति का फल उसे अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई उसकी प्रवृत्ति या कर्म की प्रशंसा नहीं करता, उस प्रवृत्ति के कारण उसे कहीं आदर नहीं मिलता, न उसकी कोई खास प्रतिष्ठा की जाती है, तब वह उस प्रवृत्ति के विषय में संशयशील होकर छोड़ बैठता है, या बेगार समझकर बिना मन से करता रहता है ।
इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति की स्वयं प्रशंसा करता रहता है, जब भी कोई कार्य सफल हो जाता है, या किसी प्रवृत्ति का प्रचार धड़ल्ले से होने लगता है, आम जनता हजारों, लाखों की संख्या में उस प्रवृत्ति की प्रशंसा करने लगती है; तब उसके मन-वाणी से ये विचार प्रादुर्भूत होने लगते हैं - " यह सब प्रवृत्ति मेरे द्वारा ही हुई है, मैंने ही यह सब कार्य अपने हाथों से किये हैं । इस कार्य का श्रेय मुझे मिलना चाहिए, अरे ! अमुक ने मुझे इस अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद तक न कहा । मुझे इस कार्य के लिए अभिनन्दन पत्र मिलना चाहिए था ।" इस प्रकार प्रवृत्ति को
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org