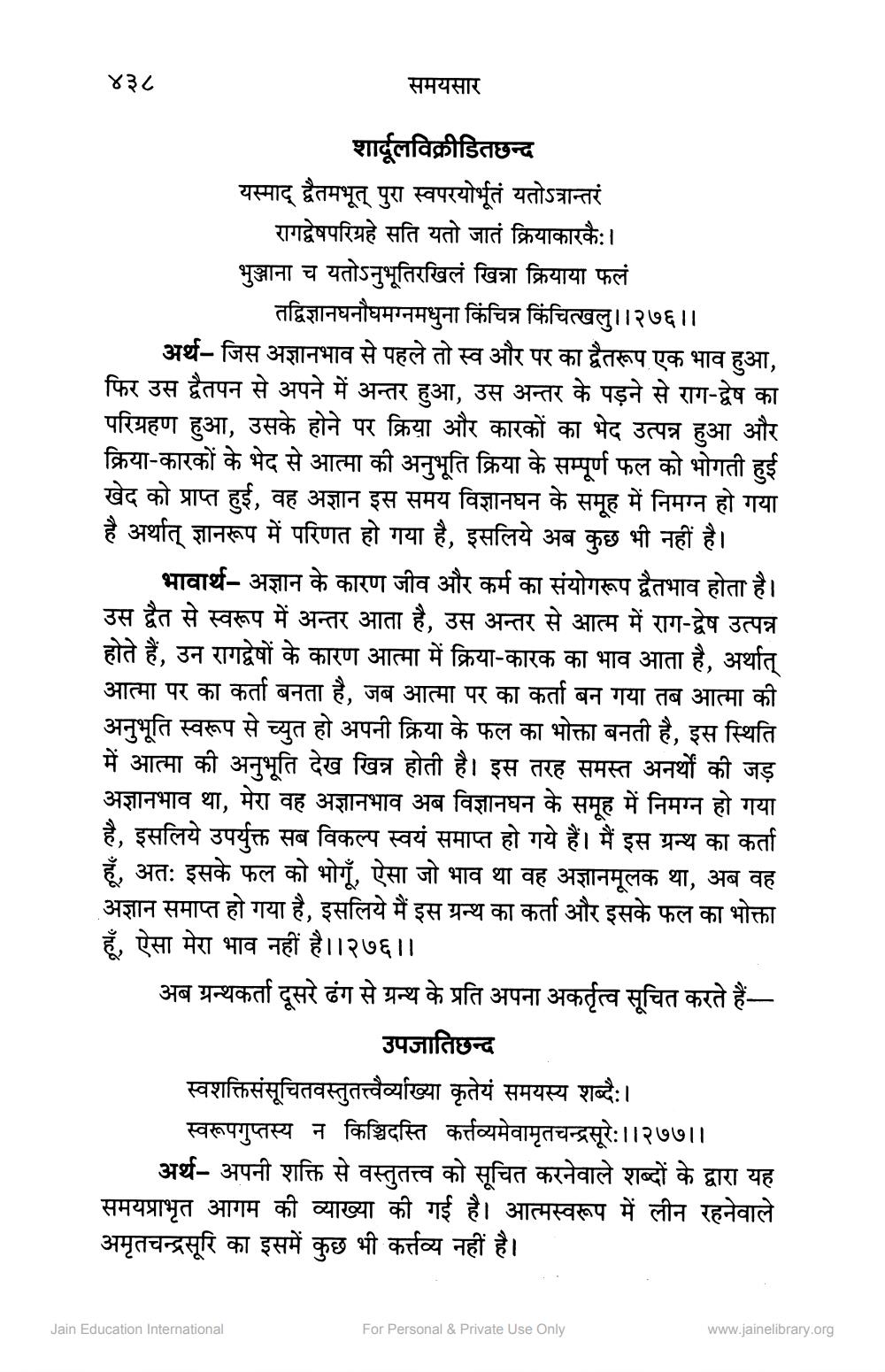________________
४३८
समयसार
शार्दूलविक्रीडितछन्द यस्माद् द्वैतमभूत् पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रान्तरं
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः। भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियाया फलं
तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किंचिन किंचित्खलु।।२७६।। अर्थ- जिस अज्ञानभाव से पहले तो स्व और पर का द्वैतरूप एक भाव हुआ, फिर उस द्वैतपन से अपने में अन्तर हुआ, उस अन्तर के पड़ने से राग-द्वेष का परिग्रहण हुआ, उसके होने पर क्रिया और कारकों का भेद उत्पन्न हुआ और क्रिया-कारकों के भेद से आत्मा की अनुभूति क्रिया के सम्पूर्ण फल को भोगती हुई
खेद को प्राप्त हुई, वह अज्ञान इस समय विज्ञानघन के समूह में निमग्न हो गया है अर्थात् ज्ञानरूप में परिणत हो गया है, इसलिये अब कुछ भी नहीं है।
भावार्थ- अज्ञान के कारण जीव और कर्म का संयोगरूप द्वैतभाव होता है। उस द्वैत से स्वरूप में अन्तर आता है, उस अन्तर से आत्म में राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं, उन रागद्वेषों के कारण आत्मा में क्रिया-कारक का भाव आता है, अर्थात् आत्मा पर का कर्ता बनता है, जब आत्मा पर का कर्ता बन गया तब आत्मा की अनुभूति स्वरूप से च्युत हो अपनी क्रिया के फल का भोक्ता बनती है, इस स्थिति में आत्मा की अनुभूति देख खिन्न होती है। इस तरह समस्त अनर्थों की जड़ अज्ञानभाव था, मेरा वह अज्ञानभाव अब विज्ञानघन के समूह में निमग्न हो गया है, इसलिये उपर्युक्त सब विकल्प स्वयं समाप्त हो गये हैं। मैं इस ग्रन्थ का कर्ता हूँ, अत: इसके फल को भोगूं, ऐसा जो भाव था वह अज्ञानमूलक था, अब वह अज्ञान समाप्त हो गया है, इसलिये मैं इस ग्रन्थ का कर्ता और इसके फल का भोक्ता हूँ, ऐसा मेरा भाव नहीं है।।२७६।। अब ग्रन्थकर्ता दूसरे ढंग से ग्रन्थ के प्रति अपना अकर्तृत्व सूचित करते हैं
उपजातिछन्द स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः। स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति कर्त्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः।।२७७।।
अर्थ- अपनी शक्ति से वस्तुतत्त्व को सूचित करनेवाले शब्दों के द्वारा यह समयप्राभृत आगम की व्याख्या की गई है। आत्मस्वरूप में लीन रहनेवाले अमृतचन्द्रसूरि का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org