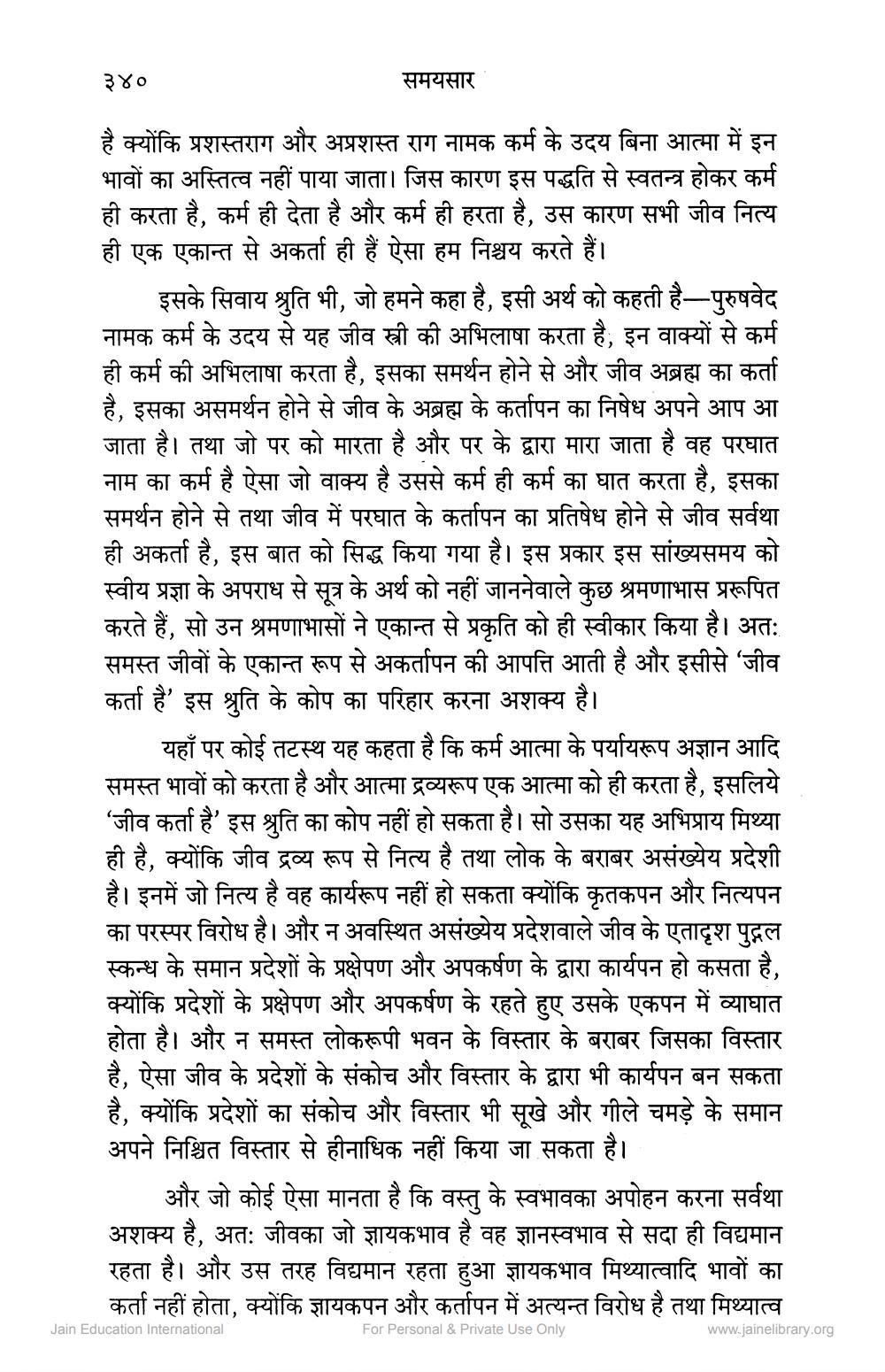________________
३४०
समयसार
है क्योंकि प्रशस्तराग और अप्रशस्त राग नामक कर्म के उदय बिना आत्मा में इन भावों का अस्तित्व नहीं पाया जाता। जिस कारण इस पद्धति से स्वतन्त्र होकर कर्म ही करता है, कर्म ही देता है और कर्म ही हरता है, उस कारण सभी जीव नित्य ही एक एकान्त से अकर्ता ही हैं ऐसा हम निश्चय करते हैं।
इसके सिवाय श्रुति भी, जो हमने कहा है, इसी अर्थ को कहती है—पुरुषवेद नामक कर्म के उदय से यह जीव स्त्री की अभिलाषा करता है, इन वाक्यों से कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है, इसका समर्थन होने से और जीव अब्रह्म का कर्ता है, इसका असमर्थन होने से जीव के अब्रह्म के कर्तापन का निषेध अपने आप आ जाता है। तथा जो पर को मारता है और पर के द्वारा मारा जाता है वह परघात नाम का कर्म है ऐसा जो वाक्य है उससे कर्म ही कर्म का घात करता है, इसका समर्थन होने से तथा जीव में परघात के कर्तापन का प्रतिषेध होने से जीव सर्वथा ही अकर्ता है, इस बात को सिद्ध किया गया है। इस प्रकार इस सांख्यसमय को स्वीय प्रज्ञा के अपराध से सूत्र के अर्थ को नहीं जाननेवाले कुछ श्रमणाभास प्ररूपित करते हैं, सो उन श्रमणाभासों ने एकान्त से प्रकृति को ही स्वीकार किया है। अत: समस्त जीवों के एकान्त रूप से अकर्तापन की आपत्ति आती है और इसीसे 'जीव कर्ता है' इस श्रृति के कोप का परिहार करना अशक्य है।
यहाँ पर कोई तटस्थ यह कहता है कि कर्म आत्मा के पर्यायरूप अज्ञान आदि समस्त भावों को करता है और आत्मा द्रव्यरूप एक आत्मा को ही करता है, इसलिये ‘जीव कर्ता है' इस श्रुति का कोप नहीं हो सकता है। सो उसका यह अभिप्राय मिथ्या ही है, क्योंकि जीव द्रव्य रूप से नित्य है तथा लोक के बराबर असंख्येय प्रदेशी है। इनमें जो नित्य है वह कार्यरूप नहीं हो सकता क्योंकि कृतकपन और नित्यपन का परस्पर विरोध है। और न अवस्थित असंख्येय प्रदेशवाले जीव के एतादृश पुद्गल स्कन्ध के समान प्रदेशों के प्रक्षेपण और अपकर्षण के द्वारा कार्यपन हो कसता है, क्योंकि प्रदेशों के प्रक्षेपण और अपकर्षण के रहते हुए उसके एकपन में व्याघात होता है। और न समस्त लोकरूपी भवन के विस्तार के बराबर जिसका विस्तार है, ऐसा जीव के प्रदेशों के संकोच और विस्तार के द्वारा भी कार्यपन बन सकता है, क्योंकि प्रदेशों का संकोच और विस्तार भी सूखे और गीले चमड़े के समान अपने निश्चित विस्तार से हीनाधिक नहीं किया जा सकता है।
और जो कोई ऐसा मानता है कि वस्तु के स्वभावका अपोहन करना सर्वथा अशक्य है, अत: जीवका जो ज्ञायकभाव है वह ज्ञानस्वभाव से सदा ही विद्यमान रहता है। और उस तरह विद्यमान रहता हुआ ज्ञायकभाव मिथ्यात्वादि भावों का कर्ता नहीं होता, क्योंकि ज्ञायकपन और कर्तापन में अत्यन्त विरोध है तथा मिथ्यात्व
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org