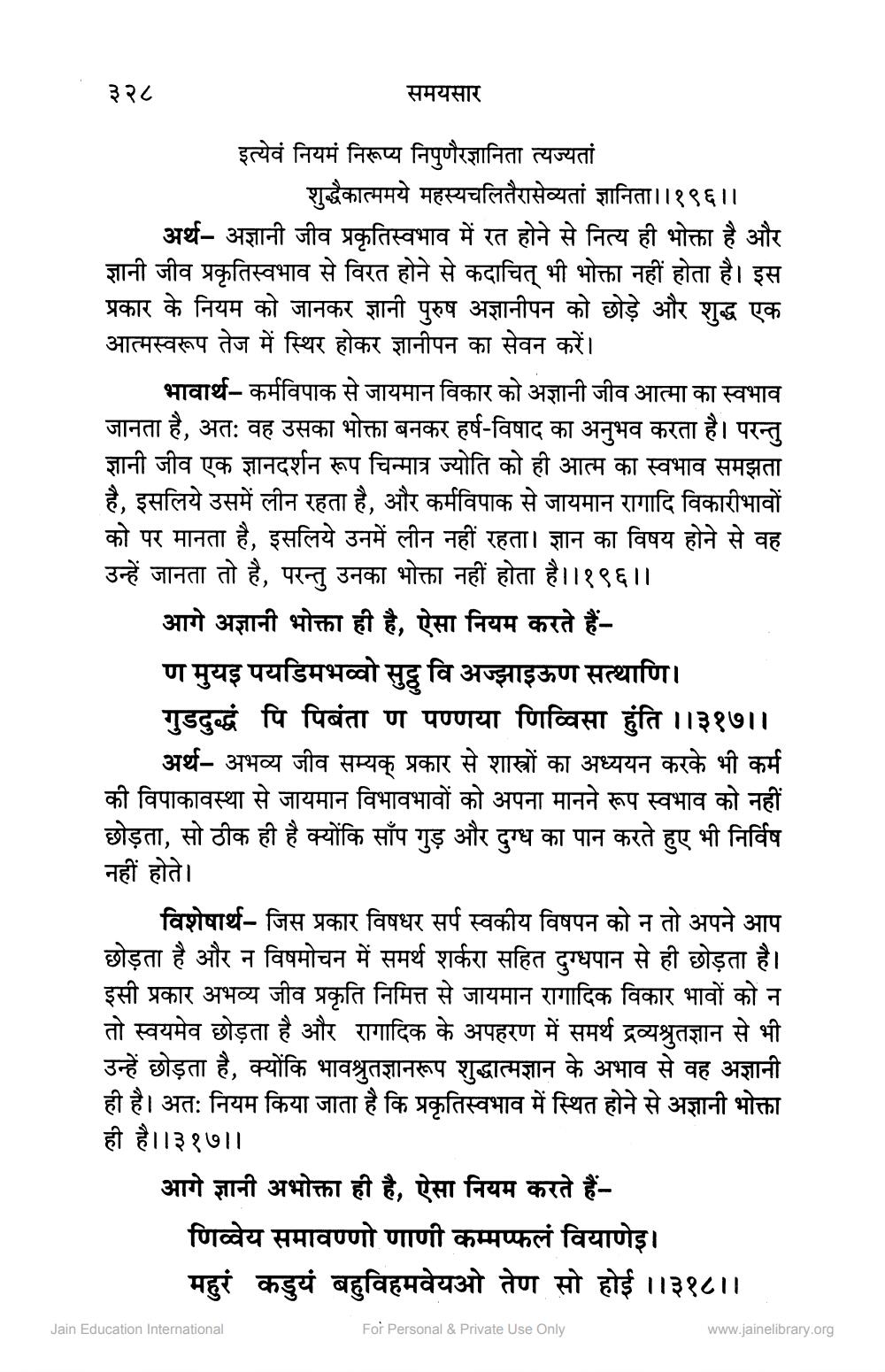________________
३२८
समयसार
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां
शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता।।१९६।। अर्थ- अज्ञानी जीव प्रकृतिस्वभाव में रत होने से नित्य ही भोक्ता है और ज्ञानी जीव प्रकृतिस्वभाव से विरत होने से कदाचित् भी भोक्ता नहीं होता है। इस प्रकार के नियम को जानकर ज्ञानी पुरुष अज्ञानीपन को छोड़े और शुद्ध एक आत्मस्वरूप तेज में स्थिर होकर ज्ञानीपन का सेवन करें।
भावार्थ- कर्मविपाक से जायमान विकार को अज्ञानी जीव आत्मा का स्वभाव जानता है, अत: वह उसका भोक्ता बनकर हर्ष-विषाद का अनुभव करता है। परन्तु ज्ञानी जीव एक ज्ञानदर्शन रूप चिन्मात्र ज्योति को ही आत्म का स्वभाव समझता है, इसलिये उसमें लीन रहता है, और कर्मविपाक से जायमान रागादि विकारीभावों को पर मानता है, इसलिये उनमें लीन नहीं रहता। ज्ञान का विषय होने से वह उन्हें जानता तो है, परन्तु उनका भोक्ता नहीं होता है।।१९६।।
आगे अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम करते हैंण मुयइ पयडिमभव्वो सुट्ठ वि अज्झाइऊण सत्थाणि। गुडदुद्धं पि पिबंता ण पण्णया णिव्विसा हुंति ।।३१७।।
अर्थ- अभव्य जीव सम्यक् प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करके भी कर्म की विपाकावस्था से जायमान विभावभावों को अपना मानने रूप स्वभाव को नहीं छोड़ता, सो ठीक ही है क्योंकि साँप गुड़ और दुग्ध का पान करते हुए भी निर्विष नहीं होते।
विशेषार्थ- जिस प्रकार विषधर सर्प स्वकीय विषपन को न तो अपने आप छोड़ता है और न विषमोचन में समर्थ शर्करा सहित दुग्धपान से ही छोड़ता है। इसी प्रकार अभव्य जीव प्रकृति निमित्त से जायमान रागादिक विकार भावों को न तो स्वयमेव छोड़ता है और रागादिक के अपहरण में समर्थ द्रव्यश्रुतज्ञान से भी उन्हें छोड़ता है, क्योंकि भावश्रुतज्ञानरूप शुद्धात्मज्ञान के अभाव से वह अज्ञानी ही है। अत: नियम किया जाता है कि प्रकृतिस्वभाव में स्थित होने से अज्ञानी भोक्ता ही है।।३१७।।
आगे ज्ञानी अभोक्ता ही है, ऐसा नियम करते हैंणिव्वेय समावण्णो णाणी कम्पप्फलं वियाणेइ। महुरं कडुयं बहुविहमवेयओ तेण सो होई ।।३१८।।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org