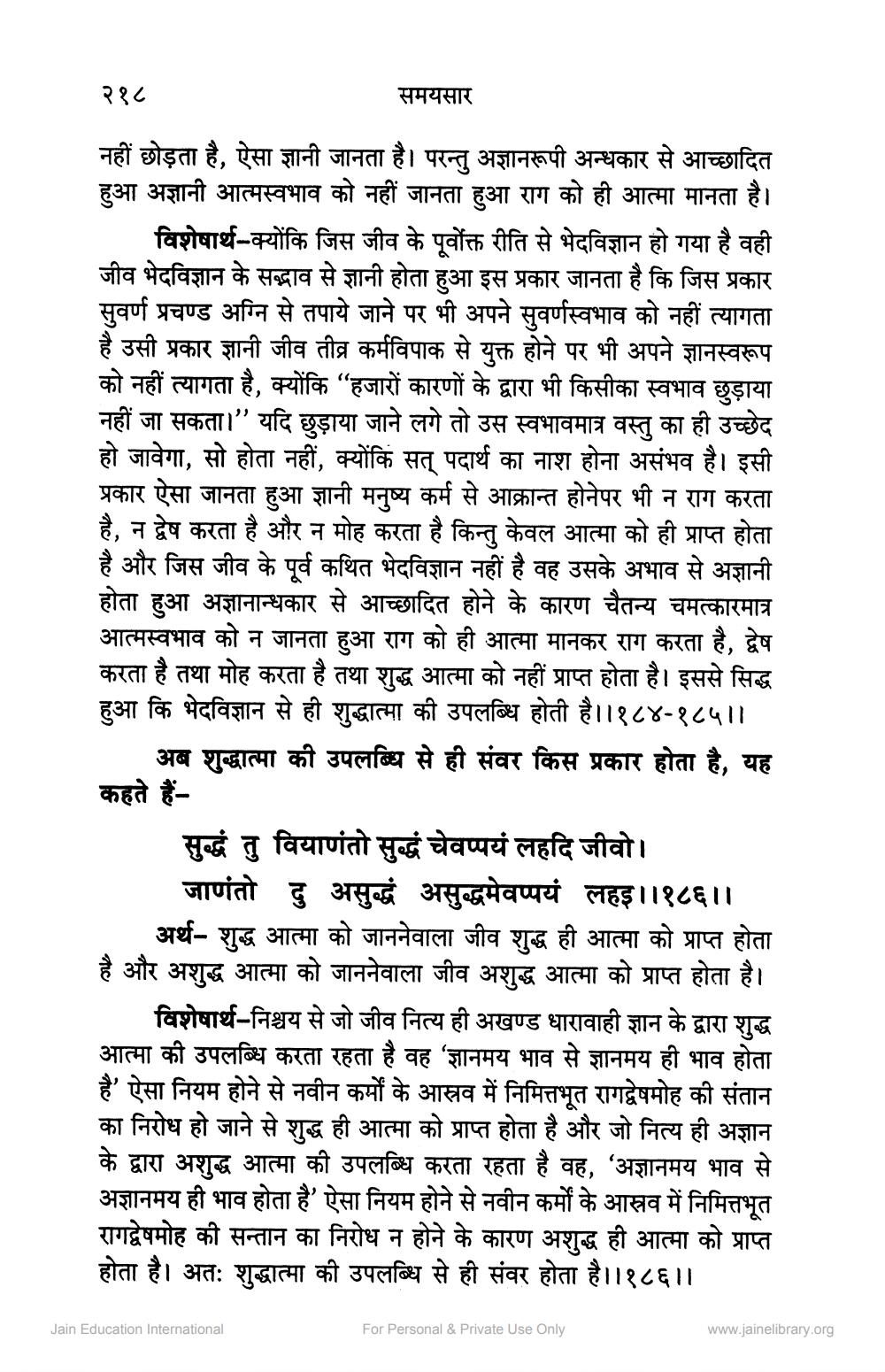________________
२१८
समयसार
नहीं छोड़ता है, ऐसा ज्ञानी जानता है। परन्तु अज्ञानरूपी अन्धकार से आच्छादित हुआ अज्ञानी आत्मस्वभाव को नहीं जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है।
विशेषार्थ-क्योंकि जिस जीव के पूर्वोक्त रीति से भेदविज्ञान हो गया है वही जीव भेदविज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार सुवर्ण प्रचण्ड अग्नि से तपाये जाने पर भी अपने सुवर्णस्वभाव को नहीं त्यागता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव तीव्र कर्मविपाक से युक्त होने पर भी अपने ज्ञानस्वरूप को नहीं त्यागता है, क्योंकि “हजारों कारणों के द्वारा भी किसीका स्वभाव छुड़ाया नहीं जा सकता।" यदि छुड़ाया जाने लगे तो उस स्वभावमात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जावेगा, सो होता नहीं, क्योंकि सत् पदार्थ का नाश होना असंभव है। इसी प्रकार ऐसा जानता हुआ ज्ञानी मनुष्य कर्म से आक्रान्त होनेपर भी न राग करता है, न द्वेष करता है और न मोह करता है किन्तु केवल आत्मा को ही प्राप्त होता है और जिस जीव के पूर्व कथित भेदविज्ञान नहीं है वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ अज्ञानान्धकार से आच्छादित होने के कारण चैतन्य चमत्कारमात्र आत्मस्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानकर राग करता है, द्वेष करता है तथा मोह करता है तथा शुद्ध आत्मा को नहीं प्राप्त होता है। इससे सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है।।१८४-१८५।।
अब शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर किस प्रकार होता है, यह कहते हैं
सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धं चेवप्पयं लहदि जीवो। जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहइ।।१८६।।
अर्थ- शुद्ध आत्मा को जाननेवाला जीव शुद्ध ही आत्मा को प्राप्त होता है और अशुद्ध आत्मा को जाननेवाला जीव अशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है।
विशेषार्थ-निश्चय से जो जीव नित्य ही अखण्ड धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करता रहता है वह 'ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय ही भाव होता है' ऐसा नियम होने से नवीन कर्मों के आस्रव में निमित्तभूत रागद्वेषमोह की संतान का निरोध हो जाने से शुद्ध ही आत्मा को प्राप्त होता है और जो नित्य ही अज्ञान के द्वारा अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि करता रहता है वह, 'अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय ही भाव होता है' ऐसा नियम होने से नवीन कर्मों के आस्रव में निमित्तभत रागद्वेषमोह की सन्तान का निरोध न होने के कारण अशुद्ध ही आत्मा को प्राप्त होता है। अत: शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है।।१८६।।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org