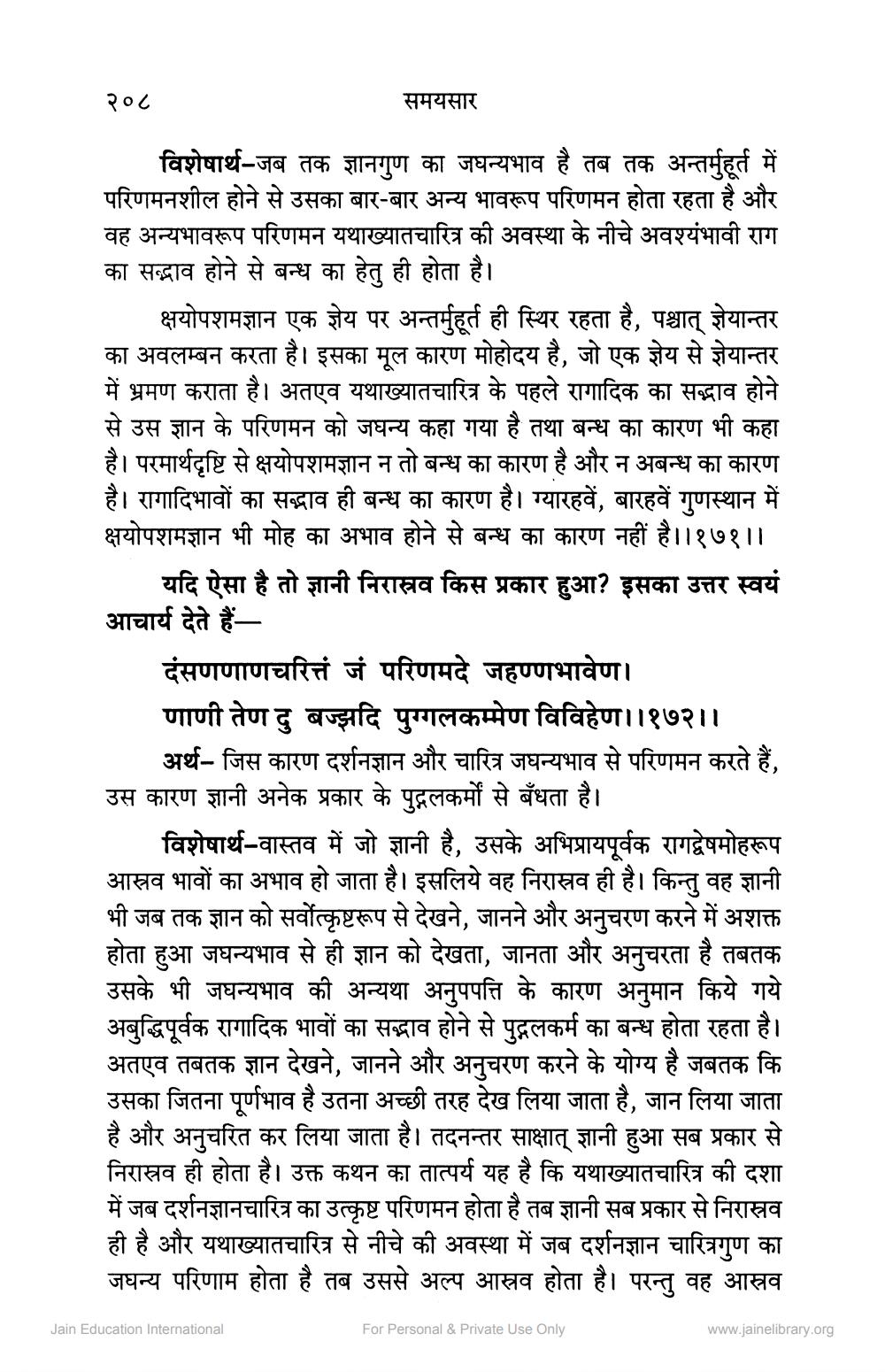________________
२०८
समयसार
विशेषार्थ-जब तक ज्ञानगुण का जघन्यभाव है तब तक अन्तर्मुहूर्त में परिणमनशील होने से उसका बार-बार अन्य भावरूप परिणमन होता रहता है और वह अन्यभावरूप परिणमन यथाख्यातचारित्र की अवस्था के नीचे अवश्यंभावी राग का सद्भाव होने से बन्ध का हेतु ही होता है।
क्षयोपशमज्ञान एक ज्ञेय पर अन्तर्मुहूर्त ही स्थिर रहता है, पश्चात् ज्ञेयान्तर का अवलम्बन करता है। इसका मूल कारण मोहोदय है, जो एक ज्ञेय से ज्ञेयान्तर में भ्रमण कराता है। अतएव यथाख्यातचारित्र के पहले रागादिक का सद्भाव होने से उस ज्ञान के परिणमन को जघन्य कहा गया है तथा बन्ध का कारण भी कहा है। परमार्थदृष्टि से क्षयोपशमज्ञान न तो बन्ध का कारण है और न अबन्ध का कारण है। रागादिभावों का सद्भाव ही बन्ध का कारण है। ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थान में क्षयोपशमज्ञान भी मोह का अभाव होने से बन्ध का कारण नहीं है।।१७१।।
यदि ऐसा है तो ज्ञानी निरास्रव किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर स्वयं आचार्य देते हैं
दसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णभावेण। णाणी तेण दु बज्झदि पुग्गलकम्मेण विविहेण।।१७२।।
अर्थ- जिस कारण दर्शनज्ञान और चारित्र जघन्यभाव से परिणमन करते हैं, उस कारण ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गलकर्मों से बँधता है।
विशेषार्थ-वास्तव में जो ज्ञानी है, उसके अभिप्रायपूर्वक रागद्वेषमोहरूप आस्रव भावों का अभाव हो जाता है। इसलिये वह निरास्रव ही है। किन्तु वह ज्ञानी भी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्टरूप से देखने, जानने और अनुचरण करने में अशक्त होता हुआ जघन्यभाव से ही ज्ञान को देखता, जानता और अनुचरता है तबतक उसके भी जघन्यभाव की अन्यथा अनुपपत्ति के कारण अनुमान किये गये अबुद्धिपूर्वक रागादिक भावों का सद्भाव होने से पुद्गलकर्म का बन्ध होता रहता है। अतएव तबतक ज्ञान देखने, जानने और अनुचरण करने के योग्य है जबतक कि उसका जितना पूर्णभाव है उतना अच्छी तरह देख लिया जाता है, जान लिया जाता है और अनुचरित कर लिया जाता है। तदनन्तर साक्षात् ज्ञानी हुआ सब प्रकार से निरास्रव ही होता है। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यथाख्यातचारित्र की दशा में जब दर्शनज्ञानचारित्र का उत्कृष्ट परिणमन होता है तब ज्ञानी सब प्रकार से निरास्रव ही है और यथाख्यातचारित्र से नीचे की अवस्था में जब दर्शनज्ञान चारित्रगुण का जघन्य परिणाम होता है तब उससे अल्प आस्रव होता है। परन्तु वह आस्रव
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org