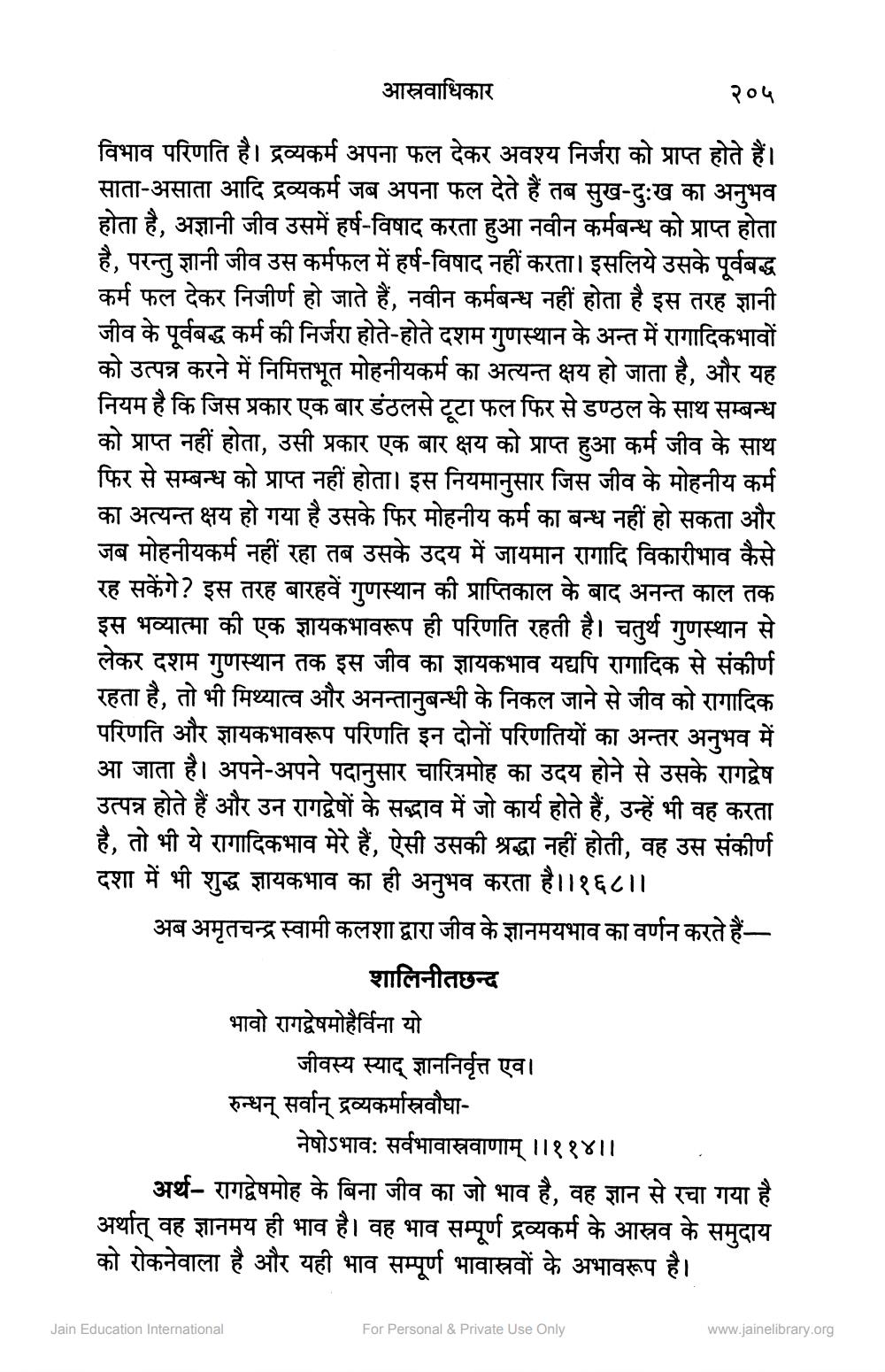________________
आस्रवाधिकार
विभाव परिणति है । द्रव्यकर्म अपना फल देकर अवश्य निर्जरा को प्राप्त होते हैं। साता-असाता आदि द्रव्यकर्म जब अपना फल देते हैं तब सुख-दुःख का अनुभव होता है, अज्ञानी जीव उसमें हर्ष-विषाद करता हुआ नवीन कर्मबन्ध को प्राप्त होता है, परन्तु ज्ञानी जीव उस कर्मफल में हर्ष-विषाद नहीं करता। इसलिये उसके पूर्वबद्ध कर्म फल देकर निजीर्ण हो जाते हैं, नवीन कर्मबन्ध नहीं होता है इस तरह ज्ञानी जीव के पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होते-होते दशम गुणस्थान के अन्त में रागादिकभावों को उत्पन्न करने में निमित्तभूत मोहनीयकर्म का अत्यन्त क्षय हो जाता है, और यह नियम है कि जिस प्रकार एक बार डंठलसे टूटा फल फिर से डण्ठल के साथ सम्बन्ध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार एक बार क्षय को प्राप्त हुआ कर्म जीव के साथ फिर से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं होता। इस नियमानुसार जिस जीव के मोहनीय कर्म का अत्यन्त क्षय हो गया है उसके फिर मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं हो सकता और जब मोहनीयकर्म नहीं रहा तब उसके उदय में जायमान रागादि विकारीभाव कैसे रह सकेंगे? इस तरह बारहवें गुणस्थान की प्राप्तिकाल के बाद अनन्त काल तक इस भव्यात्मा की एक ज्ञायकभावरूप ही परिणति रहती है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक इस जीव का ज्ञायकभाव यद्यपि रागादिक से संकीर्ण रहता है, तो भी मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी के निकल जाने से जीव को रागादिक परिणति और ज्ञायकभावरूप परिणति इन दोनों परिणतियों का अन्तर अनुभव में आ जाता है। अपने-अपने पदानुसार चारित्रमोह का उदय होने से उसके रागद्वेष उत्पन्न होते हैं और उन रागद्वेषों के सद्भाव में जो कार्य होते हैं, उन्हें भी वह करता है, तो भी ये रागादिकभाव मेरे हैं, ऐसी उसकी श्रद्धा नहीं होती, वह उस संकीर्ण दशा में भी शुद्ध ज्ञायकभाव का ही अनुभव करता है । । १६८ ।।
अब अमृतचन्द्र स्वामी कलशा द्वारा जीव के ज्ञानमयभाव का वर्णन करते हैं
शालिनीतछन्द
भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो
Jain Education International
जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्वृत्त एव ।
रुन्धन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्रवौघा
नेषोऽभावः सर्वभावास्रवाणाम् ।। ११४।।
अर्थ- रागद्वेषमोह के बिना जीव का जो भाव है, वह ज्ञान से रचा गया है अर्थात् वह ज्ञानमय ही भाव है । वह भाव सम्पूर्ण द्रव्यकर्म के आस्रव के को रोकनेवाला है और यही भाव सम्पूर्ण भावास्रवों के अभावरूप है।
समुदाय
२०५
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org