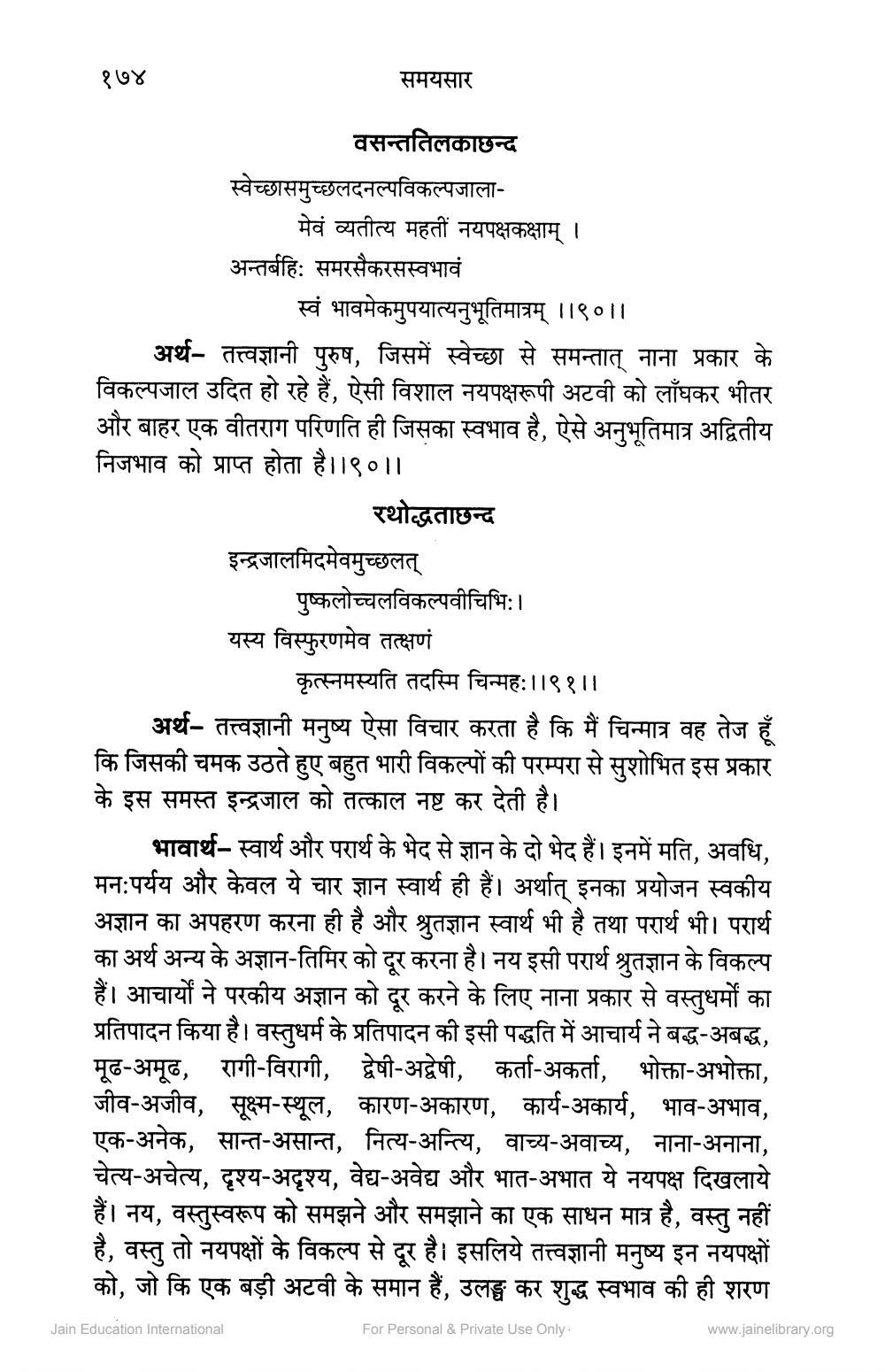________________
१७४
समयसार
वसन्ततिलकाछन्द स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला
मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् । अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभावं
स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ।।९० ।। अर्थ- तत्त्वज्ञानी पुरुष, जिसमें स्वेच्छा से समन्तात् नाना प्रकार के विकल्पजाल उदित हो रहे हैं, ऐसी विशाल नयपक्षरूपी अटवी को लाँघकर भीतर
और बाहर एक वीतराग परिणति ही जिसका स्वभाव है, ऐसे अनुभूतिमात्र अद्वितीय निजभाव को प्राप्त होता है।।९०।।
रथोद्धताछन्द इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्
पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः। यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं
कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः।।९१ ।। अर्थ- तत्त्वज्ञानी मनुष्य ऐसा विचार करता है कि मैं चिन्मात्र वह तेज हूँ कि जिसकी चमक उठते हुए बहुत भारी विकल्पों की परम्परा से सुशोभित इस प्रकार के इस समस्त इन्द्रजाल को तत्काल नष्ट कर देती है।
भावार्थ- स्वार्थ और परार्थ के भेद से ज्ञान के दो भेद हैं। इनमें मति, अवधि, मन:पर्यय और केवल ये चार ज्ञान स्वार्थ ही हैं। अर्थात् इनका प्रयोजन स्वकीय अज्ञान का अपहरण करना ही है और श्रुतज्ञान स्वार्थ भी है तथा परार्थ भी। परार्थ का अर्थ अन्य के अज्ञान-तिमिर को दूर करना है। नय इसी परार्थ श्रुतज्ञान के विकल्प हैं। आचार्यों ने परकीय अज्ञान को दूर करने के लिए नाना प्रकार से वस्तुधर्मों का प्रतिपादन किया है। वस्तुधर्म के प्रतिपादन की इसी पद्धति में आचार्य ने बद्ध-अबद्ध, मूढ-अमूढ, रागी-विरागी, द्वेषी-अद्वेषी, कर्ता-अकर्ता, भोक्ता-अभोक्ता, जीव-अजीव, सूक्ष्म-स्थूल, कारण-अकारण, कार्य-अकार्य, भाव-अभाव, एक-अनेक, सान्त-असान्त, नित्य-अन्त्यि, वाच्य-अवाच्य, नाना-अनाना,
चेत्य-अचेत्य, दृश्य-अदृश्य, वेद्य-अवेद्य और भात-अभात ये नयपक्ष दिखलाये हैं। नय, वस्तुस्वरूप को समझने और समझाने का एक साधन मात्र है, वस्तु नहीं है, वस्तु तो नयपक्षों के विकल्प से दूर है। इसलिये तत्त्वज्ञानी मनुष्य इन नयपक्षों को, जो कि एक बड़ी अटवी के समान हैं, उलङ्घ कर शुद्ध स्वभाव की ही शरण
Jain Education International
For Personal & Private Use Only.
www.jainelibrary.org