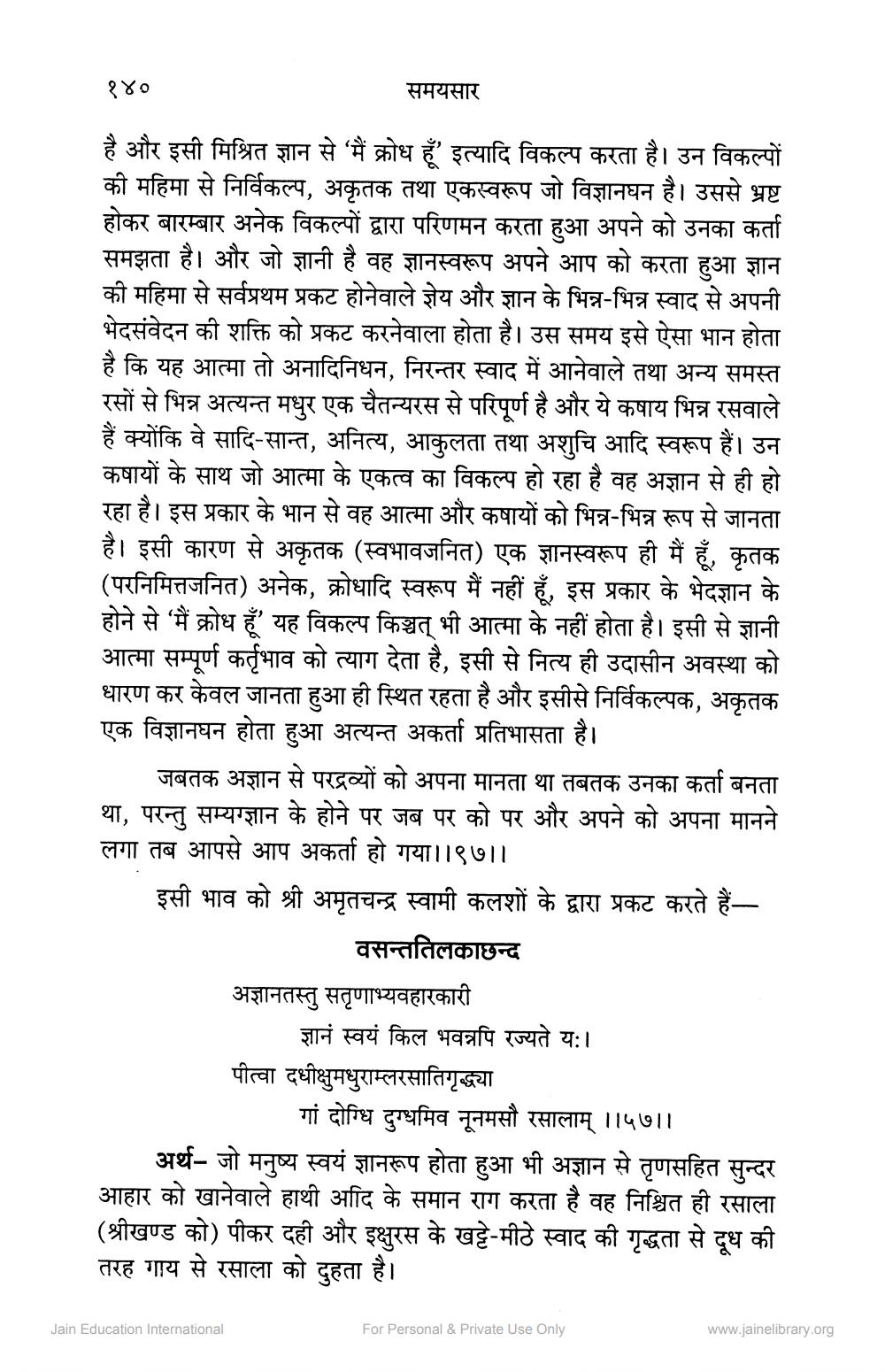________________
१४०
समयसार
है और इसी मिश्रित ज्ञान से 'मैं क्रोध हूँ' इत्यादि विकल्प करता है। उन विकल्पों की महिमा से निर्विकल्प, अकृतक तथा एकस्वरूप जो विज्ञानघन है। उससे भ्रष्ट होकर बारम्बार अनेक विकल्पों द्वारा परिणमन करता हुआ अपने को उनका कर्ता समझता है। और जो ज्ञानी है वह ज्ञानस्वरूप अपने आप को करता हुआ ज्ञान की महिमा से सर्वप्रथम प्रकट होनेवाले ज्ञेय और ज्ञान के भिन्न-भिन्न स्वाद से अपनी भेदसंवेदन की शक्ति को प्रकट करनेवाला होता है। उस समय इसे ऐसा भान होता है कि यह आत्मा तो अनादिनिधन, निरन्तर स्वाद में आनेवाले तथा अन्य समस्त रसों से भिन्न अत्यन्त मधुर एक चैतन्यरस से परिपूर्ण है और ये कषाय भिन्न रसवाले हैं क्योंकि वे सादि-सान्त, अनित्य, आकुलता तथा अशुचि आदि स्वरूप हैं। उन कषायों के साथ जो आत्मा के एकत्व का विकल्प हो रहा है वह अज्ञान से ही हो रहा है। इस प्रकार के भान से वह आत्मा और कषायों को भिन्न-भिन्न रूप से जानता है। इसी कारण से अकृतक (स्वभावजनित) एक ज्ञानस्वरूप ही मैं हूँ, कृतक (परनिमित्तजनित) अनेक, क्रोधादि स्वरूप में नहीं हूँ, इस प्रकार के भेदज्ञान के होने से 'मैं क्रोध हूँ' यह विकल्प किञ्चत् भी आत्मा के नहीं होता है। इसी से ज्ञानी आत्मा सम्पूर्ण कर्तृभाव को त्याग देता है, इसी से नित्य ही उदासीन अवस्था को धारण कर केवल जानता हुआ ही स्थित रहता है और इसीसे निर्विकल्पक, अकृतक एक विज्ञानघन होता हुआ अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासता है।
__ जबतक अज्ञान से परद्रव्यों को अपना मानता था तबतक उनका कर्ता बनता था, परन्तु सम्यग्ज्ञान के होने पर जब पर को पर और अपने को अपना मानने लगा तब आपसे आप अकर्ता हो गया।।९७।। इसी भाव को श्री अमृतचन्द्र स्वामी कलशों के द्वारा प्रकट करते हैं
वसन्ततिलकाछन्द अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी
ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः। पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्ध्या
___गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालाम् ।।५७।। अर्थ- जो मनुष्य स्वयं ज्ञानरूप होता हुआ भी अज्ञान से तृणसहित सुन्दर आहार को खानेवाले हाथी आदि के समान राग करता है वह निश्चित ही रसाला (श्रीखण्ड को) पीकर दही और इक्षुरस के खट्टे-मीठे स्वाद की गृद्धता से दूध की तरह गाय से रसाला को दुहता है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org