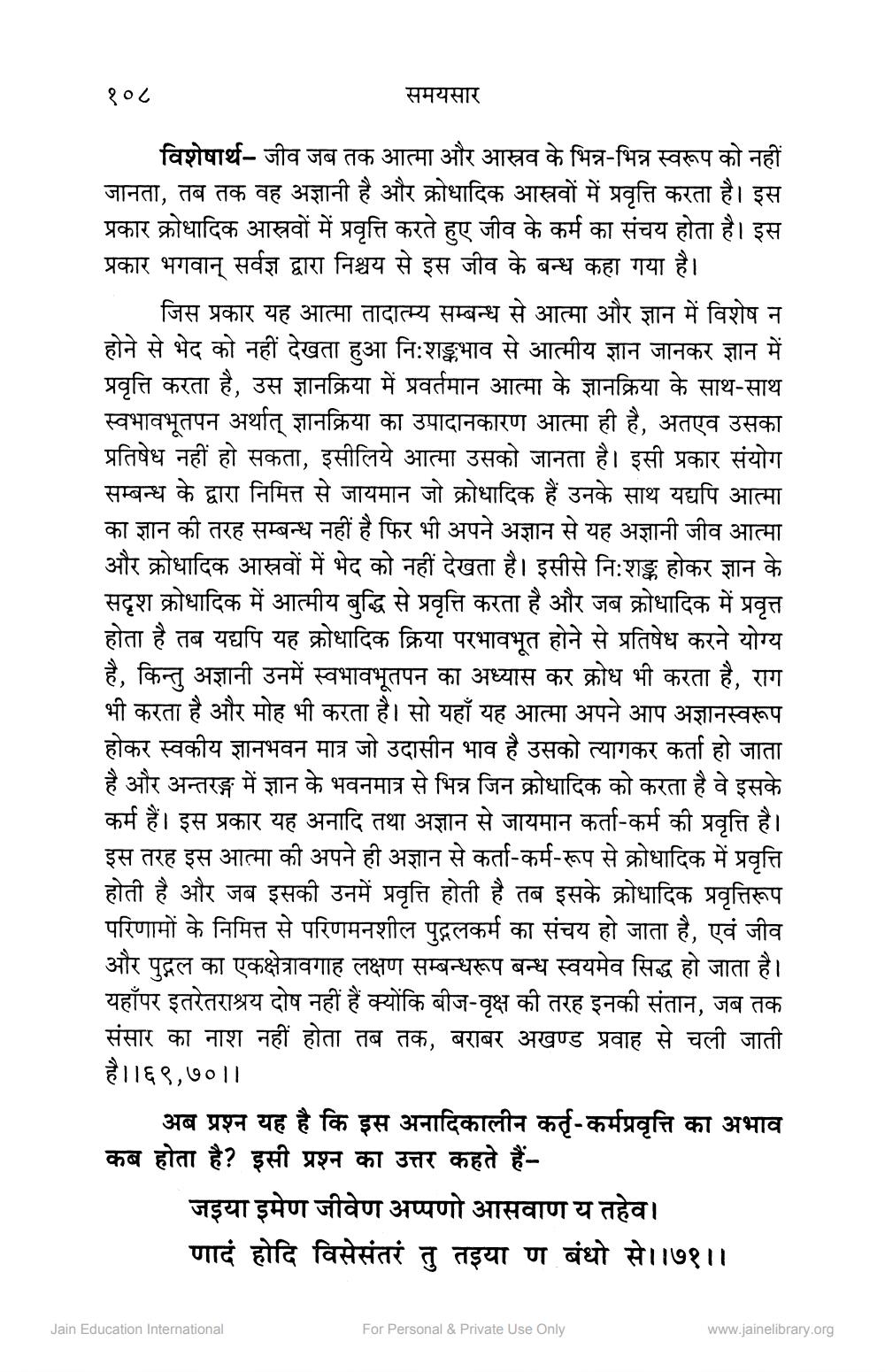________________
१०८
समयसार
विशेषार्थ- जीव जब तक आत्मा और आस्रव के भिन्न-भिन्न स्वरूप को नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी है और क्रोधादिक आस्रवों में प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार क्रोधादिक आस्रवों में प्रवृत्ति करते हुए जीव के कर्म का संचय होता है। इस प्रकार भगवान् सर्वज्ञ द्वारा निश्चय से इस जीव के बन्ध कहा गया है।
जिस प्रकार यह आत्मा तादात्म्य सम्बन्ध से आत्मा और ज्ञान में विशेष न होने से भेद को नहीं देखता हुआ निःशङ्कभाव से आत्मीय ज्ञान जानकर ज्ञान में प्रवृत्ति करता है, उस ज्ञानक्रिया में प्रवर्तमान आत्मा के ज्ञानक्रिया के साथ-साथ स्वभावभूतपन अर्थात् ज्ञानक्रिया का उपादानकारण आत्मा ही है, अतएव उसका प्रतिषेध नहीं हो सकता, इसीलिये आत्मा उसको जानता है। इसी प्रकार संयोग सम्बन्ध के द्वारा निमित्त से जायमान जो क्रोधादिक हैं उनके साथ यद्यपि आत्मा का ज्ञान की तरह सम्बन्ध नहीं है फिर भी अपने अज्ञान से यह अज्ञानी जीव आत्मा और क्रोधादिक आस्रवों में भेद को नहीं देखता है। इसीसे नि:शङ्क होकर ज्ञान के सदृश क्रोधादिक में आत्मीय बुद्धि से प्रवृत्ति करता है और जब क्रोधादिक में प्रवृत्त होता है तब यद्यपि यह क्रोधादिक क्रिया परभावभूत होने से प्रतिषेध करने योग्य है, किन्तु अज्ञानी उनमें स्वभावभूतपन का अध्यास कर क्रोध भी करता है, राग भी करता है और मोह भी करता है। सो यहाँ यह आत्मा अपने आप अज्ञानस्वरूप होकर स्वकीय ज्ञानभवन मात्र जो उदासीन भाव है उसको त्यागकर कर्ता हो जाता है और अन्तरङ्ग में ज्ञान के भवनमात्र से भिन्न जिन क्रोधादिक को करता है वे इसके कर्म हैं। इस प्रकार यह अनादि तथा अज्ञान से जायमान कर्ता-कर्म की प्रवृत्ति है। इस तरह इस आत्मा की अपने ही अज्ञान से कर्ता-कर्म-रूप से क्रोधादिक में प्रवृत्ति होती है और जब इसकी उनमें प्रवृत्ति होती है तब इसके क्रोधादिक प्रवृत्तिरूप परिणामों के निमित्त से परिणमनशील पुद्गलकर्म का संचय हो जाता है, एवं जीव और पुद्गल का एकक्षेत्रावगाह लक्षण सम्बन्धरूप बन्ध स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। यहाँपर इतरेतराश्रय दोष नहीं हैं क्योंकि बीज-वृक्ष की तरह इनकी संतान, जब तक संसार का नाश नहीं होता तब तक, बराबर अखण्ड प्रवाह से चली जाती है।।६९,७०।।
अब प्रश्न यह है कि इस अनादिकालीन कर्तृ-कर्मप्रवृत्ति का अभाव कब होता है? इसी प्रश्न का उत्तर कहते हैं
जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव। णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से।।७१।।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org