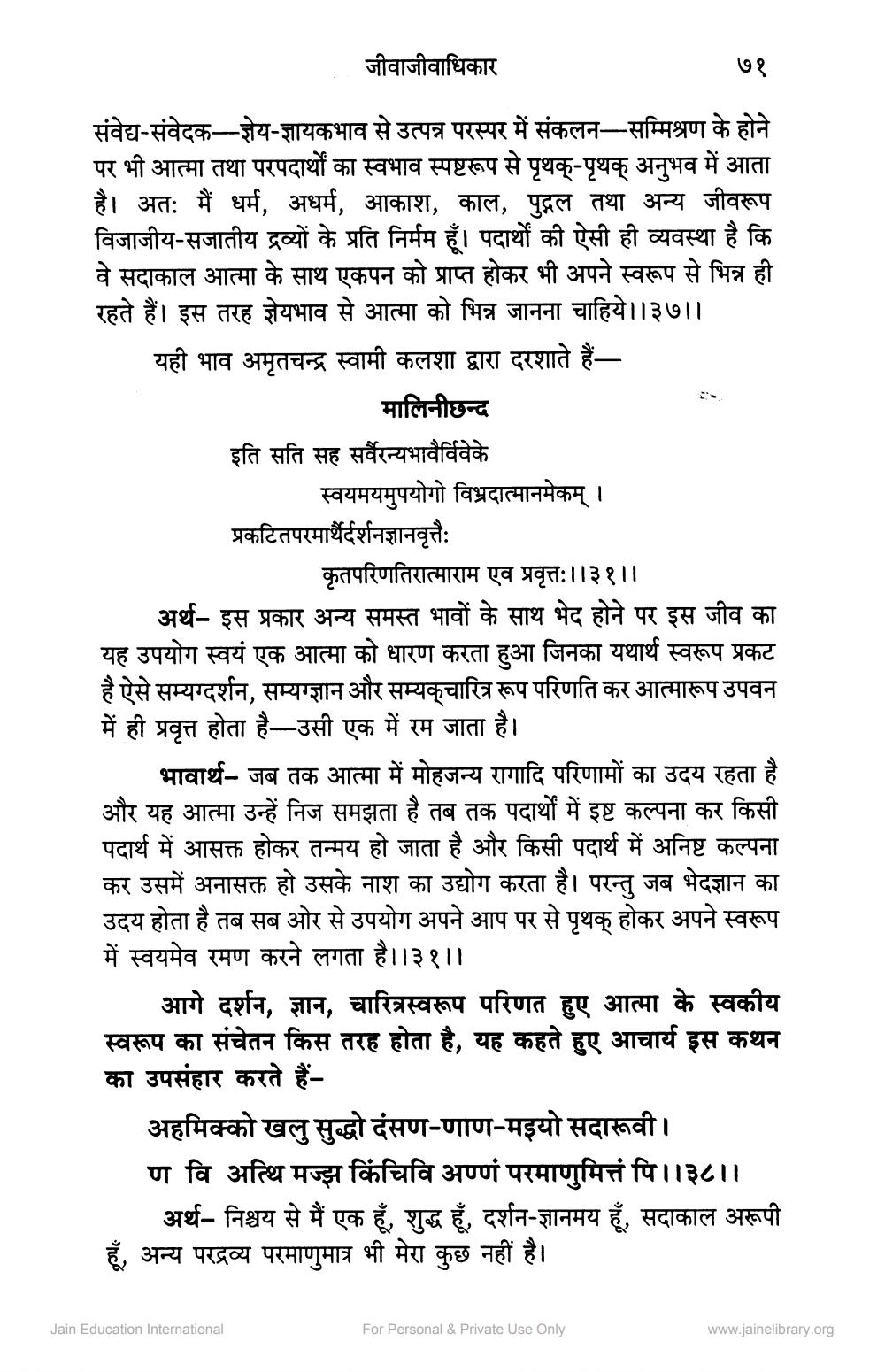________________
जीवाजीवाधिकार
संवेद्य-संवेदक-ज्ञेय-ज्ञायकभाव से उत्पन्न परस्पर में संकलन–सम्मिश्रण के होने पर भी आत्मा तथा परपदार्थों का स्वभाव स्पष्टरूप से पृथक्-पृथक् अनुभव में आता है। अत: मैं धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल तथा अन्य जीवरूप विजाजीय-सजातीय द्रव्यों के प्रति निर्मम हूँ। पदार्थों की ऐसी ही व्यवस्था है कि वे सदाकाल आत्मा के साथ एकपन को प्राप्त होकर भी अपने स्वरूप से भिन्न ही रहते हैं। इस तरह ज्ञेयभाव से आत्मा को भिन्न जानना चाहिये।।३७।। यही भाव अमृतचन्द्र स्वामी कलशा द्वारा दरशाते हैं
मालिनीछन्द इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके
स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकम् । प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः
कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः।।३१।। अर्थ- इस प्रकार अन्य समस्त भावों के साथ भेद होने पर इस जीव का यह उपयोग स्वयं एक आत्मा को धारण करता हुआ जिनका यथार्थ स्वरूप प्रकट है ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप परिणति कर आत्मारूप उपवन में ही प्रवृत्त होता है-उसी एक में रम जाता है।
भावार्थ- जब तक आत्मा में मोहजन्य रागादि परिणामों का उदय रहता है और यह आत्मा उन्हें निज समझता है तब तक पदार्थों में इष्ट कल्पना कर किसी पदार्थ में आसक्त होकर तन्मय हो जाता है और किसी पदार्थ में अनिष्ट कल्पना कर उसमें अनासक्त हो उसके नाश का उद्योग करता है। परन्तु जब भेदज्ञान का उदय होता है तब सब ओर से उपयोग अपने आप पर से पृथक् होकर अपने स्वरूप में स्वयमेव रमण करने लगता है।।३१।।
आगे दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप परिणत हुए आत्मा के स्वकीय स्वरूप का संचेतन किस तरह होता है, यह कहते हुए आचार्य इस कथन का उपसंहार करते हैं
अहमिक्को खलु सुद्धो दंसण-णाण-मइयो सदारूवी। ण वि अस्थि मज्झ किंचिवि अण्णं परमाणुमित्तं पि।।३८॥
अर्थ- निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञानमय हूँ, सदाकाल अरूपी हूँ, अन्य परद्रव्य परमाणुमात्र भी मेरा कुछ नहीं है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org