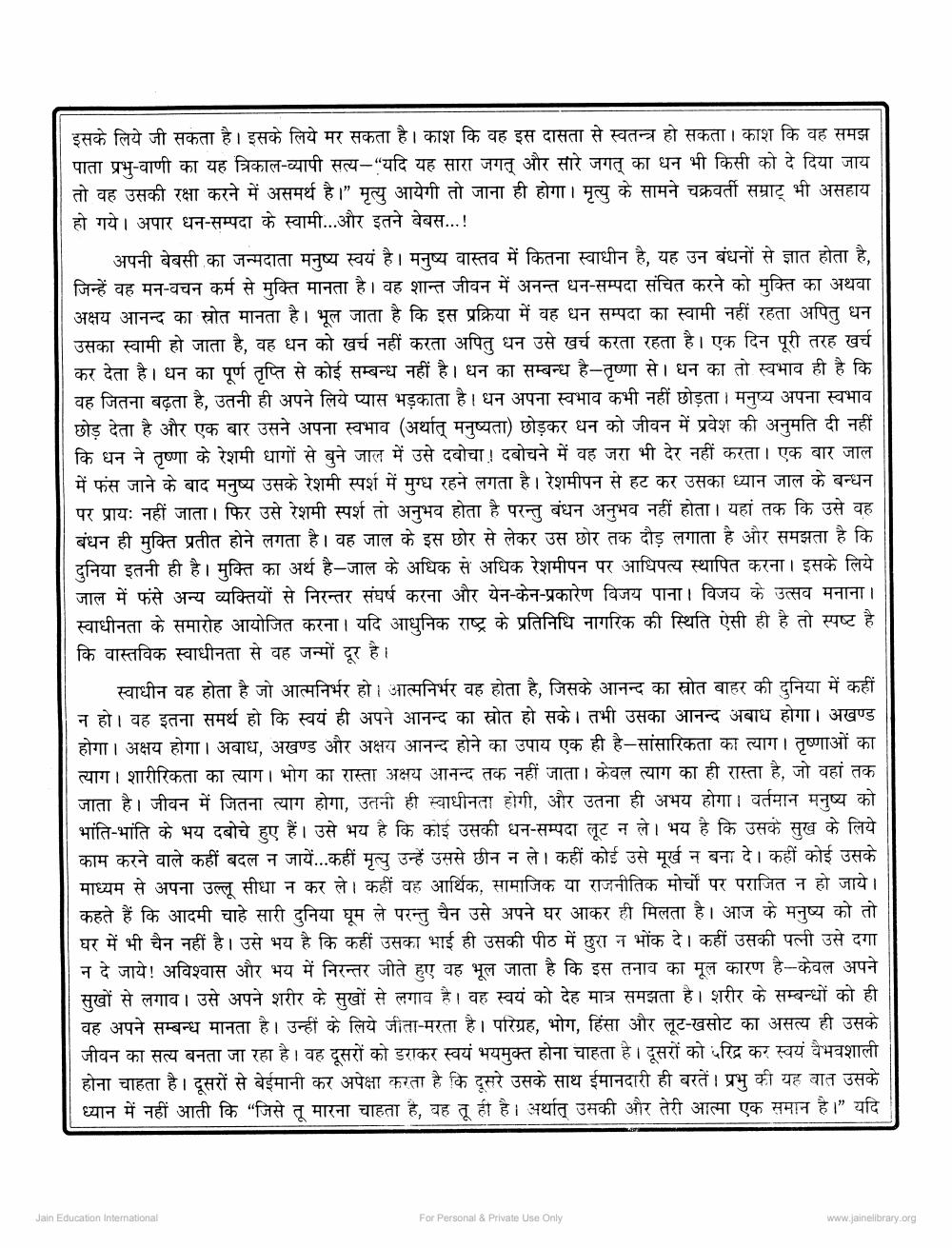________________
इसके लिये जी सकता है। इसके लिये मर सकता है। काश कि वह इस दासता से स्वतन्त्र हो सकता। काश कि वह समझ पाता प्रभु-वाणी का यह त्रिकाल-व्यापी सत्य-“यदि यह सारा जगत् और सारे जगत् का धन भी किसी को दे दिया जाय तो वह उसकी रक्षा करने में असमर्थ है।" मृत्यु आयेगी तो जाना ही होगा। मृत्यु के सामने चक्रवर्ती सम्राट भी असहाय हो गये। अपार धन-सम्पदा के स्वामी...और इतने बेबस...!
अपनी बेबसी का जन्मदाता मनुष्य स्वयं है। मनुष्य वास्तव में कितना स्वाधीन है, यह उन बंधनों से ज्ञात होता है, जिन्हें वह मन-वचन कर्म से मुक्ति मानता है। वह शान्त जीवन में अनन्त धन-सम्पदा संचित करने को मुक्ति का अथवा अक्षय आनन्द का स्रोत मानता है। भूल जाता है कि इस प्रक्रिया में वह धन सम्पदा का स्वामी नहीं रहता अपितु धन उसका स्वामी हो जाता है, वह धन को खर्च नहीं करता अपितु धन उसे खर्च करता रहता है। एक दिन पूरी तरह खर्च कर देता है। धन का पूर्ण तृप्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। धन का सम्बन्ध है-तृष्णा से। धन का तो स्वभाव ही है कि वह जितना बढ़ता है, उतनी ही अपने लिये प्यास भड़काता है। धन अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य अपना स्वभाव छोड़ देता है और एक बार उसने अपना स्वभाव (अर्थात् मनुष्यता) छोड़कर धन को जीवन में प्रवेश की अनुमति दी नहीं कि धन ने तृष्णा के रेशमी धागों से बुने जाल में उसे दबोचा। दबोचने में वह जरा भी देर नहीं करता। एक बार जाल में फंस जाने के बाद मनुष्य उसके रेशमी स्पर्श में मुग्ध रहने लगता है। रेशमीपन से हट कर उसका ध्यान जाल के बन्धन पर प्रायः नहीं जाता। फिर उसे रेशमी स्पर्श तो अनुभव होता है परन्तु बंधन अनुभव नहीं होता। यहां तक कि उसे वह बंधन ही मुक्ति प्रतीत होने लगता है। वह जाल के इस छोर से लेकर उस छोर तक दौड़ लगाता है और समझता है कि दुनिया इतनी ही है। मुक्ति का अर्थ है-जाल के अधिक से अधिक रेशमीपन पर आधिपत्य स्थापित करना। इसके लिये जाल में फंसे अन्य व्यक्तियों से निरन्तर संघर्ष करना और येन-केन-प्रकारेण विजय पाना। विजय के उत्सव मनाना। स्वाधीनता के समारोह आयोजित करना। यदि आधुनिक राष्ट्र के प्रतिनिधि नागरिक की स्थिति ऐसी ही है तो स्पष्ट है कि वास्तविक स्वाधीनता से वह जन्मों दूर है।
स्वाधीन वह होता है जो आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर वह होता है, जिसके आनन्द का स्रोत बाहर की दुनिया में कहीं न हो। वह इतना समर्थ हो कि स्वयं ही अपने आनन्द का स्रोत हो सके। तभी उसका आनन्द अबाध होगा। अखण्ड होगा। अक्षय होगा। अबाध, अखण्ड और अक्षय आनन्द होने का उपाय एक ही है-सांसारिकता का त्याग। तृष्णाओं का त्याग। शारीरिकता का त्याग। भोग का रास्ता अक्षय आनन्द तक नहीं जाता। केवल त्याग का ही रास्ता है, जो वहां तक जाता है। जीवन में जितना त्याग होगा, उतनी ही स्वाधीनता होगी, और उतना ही अभय होगा। वर्तमान मनुष्य को भांति-भांति के भय दबोचे हुए हैं। उसे भय है कि कोई उसकी धन-सम्पदा लूट न ले। भय है कि उसके सुख के लिये काम करने वाले कहीं बदल न जायें...कहीं मृत्यु उन्हें उससे छीन न ले। कहीं कोई उसे मूर्ख न बना दे। कहीं कोई उसके माध्यम से अपना उल्लू सीधा न कर ले। कहीं वह आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक मोर्चों पर पराजित न हो जाये। कहते हैं कि आदमी चाहे सारी दुनिया घूम ले परन्तु चैन उसे अपने घर आकर ही मिलता है। आज के मनुष्य को तो घर में भी चैन नहीं है। उसे भय है कि कहीं उसका भाई ही उसकी पीठ में छुरा न भोंक दे। कहीं उसकी पत्नी उसे दगा न दे जाये! अविश्वास और भय में निरन्तर जीते हुए वह भूल जाता है कि इस तनाव का मूल कारण है-केवल अपने सुखों से लगाव। उसे अपने शरीर के सुखों से लगाव है। वह स्वयं को देह मात्र समझता है। शरीर के सम्बन्धों को ही वह अपने सम्बन्ध मानता है। उन्हीं के लिये जीता-मरता है। परिग्रह, भोग, हिंसा और लूट-खसोट का असत्य ही उसके जीवन का सत्य बनता जा रहा है। वह दूसरों को डराकर स्वयं भयमुक्त होना चाहता है। दूसरों को परिद्र कर स्वयं वैभवशाली होना चाहता है। दूसरों से बेईमानी कर अपेक्षा करता है कि दुसरे उसके साथ ईमानदारी ही बरतें। प्रभु की यह बात उसके ध्यान में नहीं आती कि “जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है। अर्थात उसकी और तेरी आत्मा एक समान है।" यदि
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org