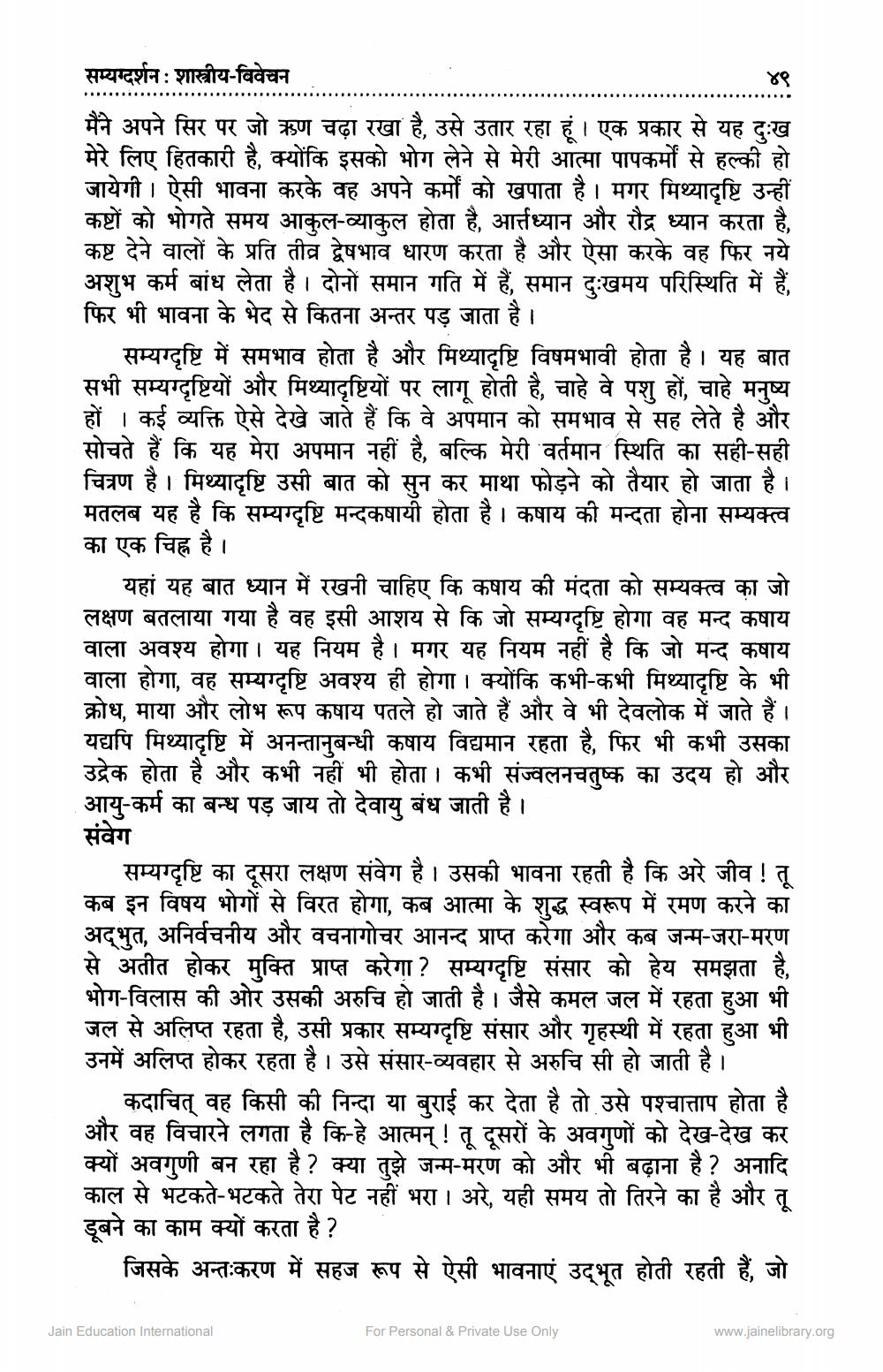________________
सम्यग्दर्शन : शास्त्रीय-विवेचन
४९
मैंने अपने सिर पर जो ऋण चढ़ा रखा है, उसे उतार रहा हूं। एक प्रकार से यह दुःख मेरे लिए हितकारी है, क्योंकि इसको भोग लेने से मेरी आत्मा पापकर्मों से हल्की हो जायेगी । ऐसी भावना करके वह अपने कर्मों को खपाता है। मगर मिथ्यादृष्टि उन्हीं कष्टों को भोगते समय आकुल-व्याकुल होता है, आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान करता है, कष्ट देने वालों के प्रति तीव्र द्वेषभाव धारण करता है और ऐसा करके वह फिर नये अशुभ कर्म बांध लेता है । दोनों समान गति में हैं, समान दुःखमय परिस्थिति में हैं, फिर भी भावना के भेद से कितना अन्तर पड़ जाता है I
सम्यग्दृष्टि में समभाव होता है और मिथ्यादृष्टि विषमभावी होता है । यह बात सभी सम्यग्दृष्टियों और मिथ्यादृष्टियों पर लागू होती है, चाहे वे पशु हों, चाहे मनुष्य हों । कई व्यक्ति ऐसे देखे जाते हैं कि वे अपमान को समभाव से सह लेते है और सोचते हैं कि यह मेरा अपमान नहीं है, बल्कि मेरी वर्तमान स्थिति का सही-सही चित्रण है । मिथ्यादृष्टि उसी बात को सुन कर माथा फोड़ने को तैयार हो जाता है । मतलब यह है कि सम्यग्दृष्टि मन्दकषायी होता है । कषाय की मन्दता होना सम्यक्त्व का एक चिह्न है ।
यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कषाय की मंदता को सम्यक्त्व का जो लक्षण बतलाया गया है वह इसी आशय से कि जो सम्यग्दृष्टि होगा वह मन्द कषाय वाला अवश्य होगा। यह नियम है । मगर यह नियम नहीं है कि जो मन्द कषाय वाला होगा, वह सम्यग्दृष्टि अवश्य ही होगा। क्योंकि कभी-कभी मिथ्यादृष्टि के भी क्रोध, माया और लोभ रूप कषाय पतले हो जाते हैं और वे भी देवलोक में जाते हैं । यद्यपि मिथ्यादृष्टि में अनन्तानुबन्धी कषाय विद्यमान रहता है, फिर भी कभी उसका उद्रेक होता है और कभी नहीं भी होता । कभी संज्वलनचतुष्क का उदय हो और आयु-कर्म का बन्ध पड़ जाय तो देवायु बंध जाती है
1
संवेग
सम्यग्दृष्टि का दूसरा लक्षण संवेग है । उसकी भावना रहती है कि अरे जीव ! तू कब इन विषय भोगों से विरत होगा, कब आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करने का अद्भुत, अनिर्वचनीय और वचनागोचर आनन्द प्राप्त करेगा और कब जन्म- जरा - मरण से अतीत होकर मुक्ति प्राप्त करेगा ? सम्यग्दृष्टि संसार को हेय समझता है, भोग-विलास की ओर उसकी अरुचि हो जाती है । जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार और गृहस्थी में रहता हुआ भी उनमें अलिप्त होकर रहता है । उसे संसार - व्यवहार से अरुचि सी हो जाती है ।
कदाचित् वह किसी की निन्दा या बुराई कर देता है तो उसे पश्चात्ताप होता है और वह विचारने लगता है कि हे आत्मन् ! तू दूसरों के अवगुणों को देख-देख कर क्यों अवगुणी बन रहा है ? क्या तुझे जन्म-मरण को और भी बढ़ाना है ? अनादि काल से भटकते-भटकते तेरा पेट नहीं भरा । अरे, यही समय तो तिरने का है और तू डूबने का काम क्यों करता है ?
जिसके अन्तःकरण में सहज रूप से ऐसी भावनाएं उद्भूत होती रहती हैं, जो
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org