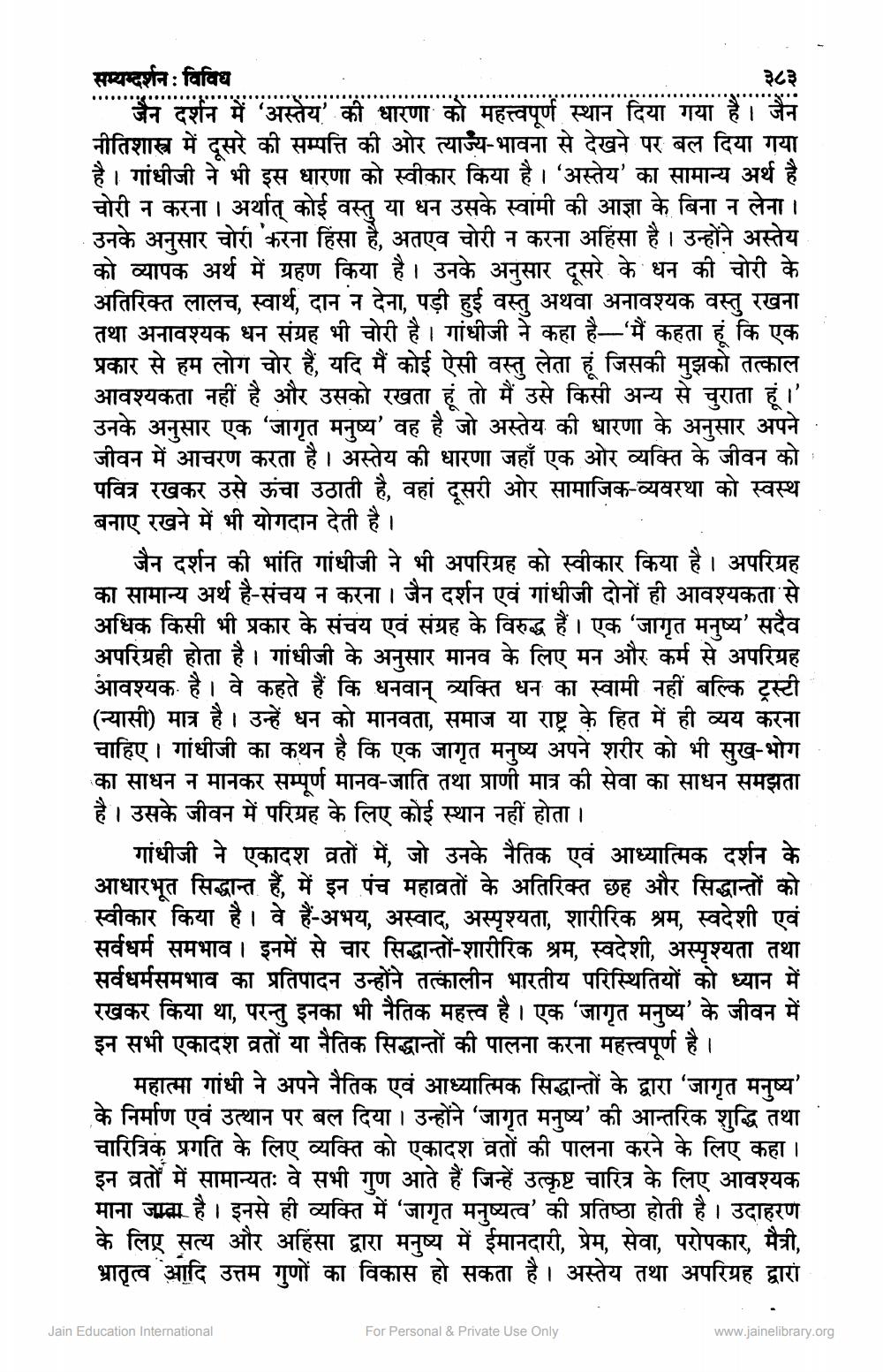________________
सम्यग्दर्शन : विविध
३८३ जैन दर्शन में 'अस्तेय की धारणा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैन नीतिशास्त्र में दूसरे की सम्पत्ति की ओर त्याज्य-भावना से देखने पर बल दिया गया है। गांधीजी ने भी इस धारणा को स्वीकार किया है। 'अस्तेय' का सामान्य अर्थ है चोरी न करना । अर्थात् कोई वस्तु या धन उसके स्वामी की आज्ञा के बिना न लेना। उनके अनुसार चोरी करना हिंसा है, अतएव चोरी न करना अहिंसा है। उन्होंने अस्तेय को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है। उनके अनुसार दूसरे के धन की चोरी के अतिरिक्त लालच, स्वार्थ, दान न देना, पड़ी हुई वस्तु अथवा अनावश्यक वस्तु रखना तथा अनावश्यक धन संग्रह भी चोरी है। गांधीजी ने कहा है—'मैं कहता हूं कि एक प्रकार से हम लोग चोर हैं, यदि मैं कोई ऐसी वस्तु लेता हूं जिसकी मुझको तत्काल आवश्यकता नहीं है और उसको रखता हूं तो मैं उसे किसी अन्य से चुराता हूं।' उनके अनुसार एक 'जागृत मनुष्य' वह है जो अस्तेय की धारणा के अनुसार अपने . जीवन में आचरण करता है। अस्तेय की धारणा जहाँ एक ओर व्यक्ति के जीवन को । पवित्र रखकर उसे ऊंचा उठाती है, वहां दूसरी ओर सामाजिक-व्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने में भी योगदान देती है।
जैन दर्शन की भांति गांधीजी ने भी अपरिग्रह को स्वीकार किया है। अपरिग्रह का सामान्य अर्थ है-संचय न करना। जैन दर्शन एवं गांधीजी दोनों ही आवश्यकता से अधिक किसी भी प्रकार के संचय एवं संग्रह के विरुद्ध हैं। एक 'जागृत मनुष्य' सदैव अपरिग्रही होता है। गांधीजी के अनुसार मानव के लिए मन और कर्म से अपरिग्रह आवश्यक है। वे कहते हैं कि धनवान् व्यक्ति धन का स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी (न्यासी) मात्र है। उन्हें धन को मानवता, समाज या राष्ट्र के हित में ही व्यय करना चाहिए। गांधीजी का कथन है कि एक जागृत मनुष्य अपने शरीर को भी सुख-भोग का साधन न मानकर सम्पूर्ण मानव-जाति तथा प्राणी मात्र की सेवा का साधन समझता है। उसके जीवन में परिग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होता।
गांधीजी ने एकादश व्रतों में, जो उनके नैतिक एवं आध्यात्मिक दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त हैं, में इन पंच महाव्रतों के अतिरिक्त छह और सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। वे हैं-अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता, शारीरिक श्रम, स्वदेशी एवं सर्वधर्म समभाव। इनमें से चार सिद्धान्तों-शारीरिक श्रम, स्वदेशी, अस्पृश्यता तथा सर्वधर्मसमभाव का प्रतिपादन उन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया था, परन्तु इनका भी नैतिक महत्त्व है। एक 'जागृत मनुष्य के जीवन में इन सभी एकादश व्रतों या नैतिक सिद्धान्तों की पालना करना महत्त्वपूर्ण है।
महात्मा गांधी ने अपने नैतिक एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तों के द्वारा 'जागृत मनुष्य' के निर्माण एवं उत्थान पर बल दिया। उन्होंने 'जागृत मनुष्य' की आन्तरिक शुद्धि तथा चारित्रिक प्रगति के लिए व्यक्ति को एकादश व्रतों की पालना करने के लिए कहा। इन व्रतों में सामान्यतः वे सभी गुण आते हैं जिन्हें उत्कृष्ट चारित्र के लिए आवश्यक माना जाता है। इनसे ही व्यक्ति में 'जागृत मनुष्यत्व' की प्रतिष्ठा होती है। उदाहरण के लिए सत्य और अहिंसा द्वारा मनुष्य में ईमानदारी, प्रेम, सेवा, परोपकार, मैत्री, भ्रातृत्व आदि उत्तम गुणों का विकास हो सकता है। अस्तेय तथा अपरिग्रह द्वारा
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org