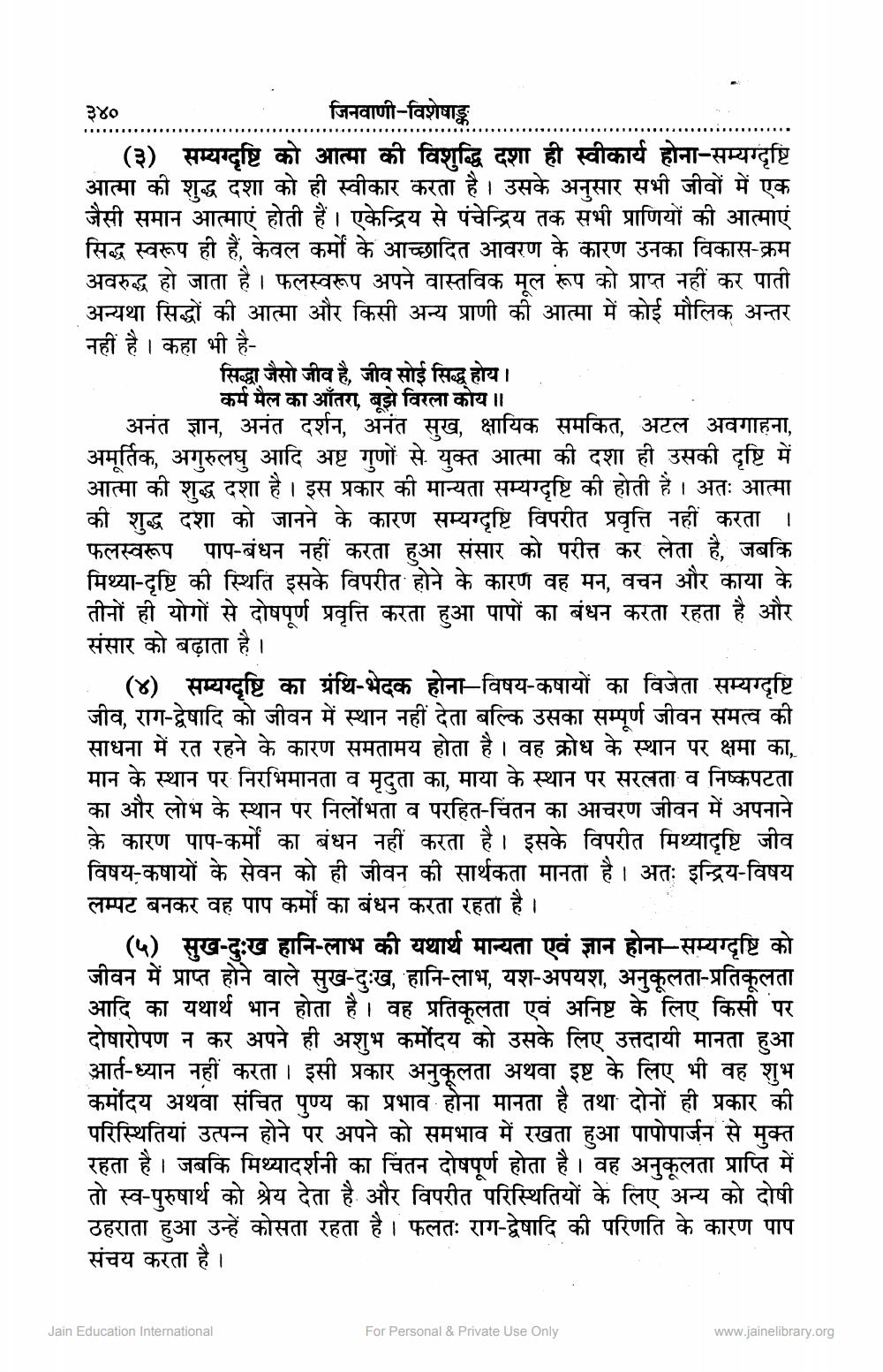________________
३४०
जिनवाणी-विशेषाङ्क ___ (३) सम्यग्दृष्टि को आत्मा की विशुद्धि दशा ही स्वीकार्य होना-सम्यग्दृष्टि आत्मा की शुद्ध दशा को ही स्वीकार करता है। उसके अनुसार सभी जीवों में एक जैसी समान आत्माएं होती हैं। एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक सभी प्राणियों की आत्माएं सिद्ध स्वरूप ही हैं, केवल कर्मों के आच्छादित आवरण के कारण उनका विकास-क्रम अवरुद्ध हो जाता है। फलस्वरूप अपने वास्तविक मूल रूप को प्राप्त नहीं कर पाती अन्यथा सिद्धों की आत्मा और किसी अन्य प्राणी की आत्मा में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। कहा भी है
सिद्धा जैसो जीव है, जीव सोई सिद्ध होय।
कर्म मैल का ऑतरा, बूझे विरला कोय ।। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, क्षायिक समकित, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरुलघु आदि अष्ट गुणों से युक्त आत्मा की दशा ही उसकी दृष्टि में आत्मा की शुद्ध दशा है । इस प्रकार की मान्यता सम्यग्दृष्टि की होती है । अतः आत्मा की शुद्ध दशा को जानने के कारण सम्यग्दृष्टि विपरीत प्रवृत्ति नहीं करता । फलस्वरूप पाप-बंधन नहीं करता हुआ संसार को परीत्त कर लेता है, जबकि मिथ्या-दृष्टि की स्थिति इसके विपरीत होने के कारण वह मन, वचन और काया के तीनों ही योगों से दोषपूर्ण प्रवृत्ति करता हुआ पापों का बंधन करता रहता है और संसार को बढ़ाता है।
(४) सम्यग्दृष्टि का ग्रंथि-भेदक होना-विषय-कषायों का विजेता सम्यग्दृष्टि जीव, राग-द्वेषादि को जीवन में स्थान नहीं देता बल्कि उसका सम्पूर्ण जीवन समत्व की साधना में रत रहने के कारण समतामय होता है। वह क्रोध के स्थान पर क्षमा का, मान के स्थान पर निरभिमानता व मृदुता का, माया के स्थान पर सरलता व निष्कपटता का और लोभ के स्थान पर निर्लोभता व परहित-चिंतन का आचरण जीवन में अपनाने के कारण पाप-कर्मों का बंधन नहीं करता है। इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि जीव विषय-कषायों के सेवन को ही जीवन की सार्थकता मानता है। अतः इन्द्रिय-विषय लम्पट बनकर वह पाप कर्मों का बंधन करता रहता है।
(५) सुख-दुःख हानि-लाभ की यथार्थ मान्यता एवं ज्ञान होना-सम्यग्दृष्टि को जीवन में प्राप्त होने वाले सुख-दुःख, हानि-लाभ, यश-अपयश, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि का यथार्थ भान होता है। वह प्रतिकूलता एवं अनिष्ट के लिए किसी पर दोषारोपण न कर अपने ही अशभ कर्मोदय को उसके लिए उत्तदायी मानता हआ आर्त-ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार अनुकूलता अथवा इष्ट के लिए भी वह शुभ कर्मोदय अथवा संचित पुण्य का प्रभाव होना मानता है तथा दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अपने को समभाव में रखता हुआ पापोपार्जन से मुक्त रहता है। जबकि मिथ्यादर्शनी का चिंतन दोषपूर्ण होता है। वह अनुकूलता प्राप्ति में तो स्व-पुरुषार्थ को श्रेय देता है और विपरीत परिस्थितियों के लिए अन्य को दोषी ठहराता हुआ उन्हें कोसता रहता है। फलतः राग-द्वेषादि की परिणति के कारण पाप संचय करता है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org