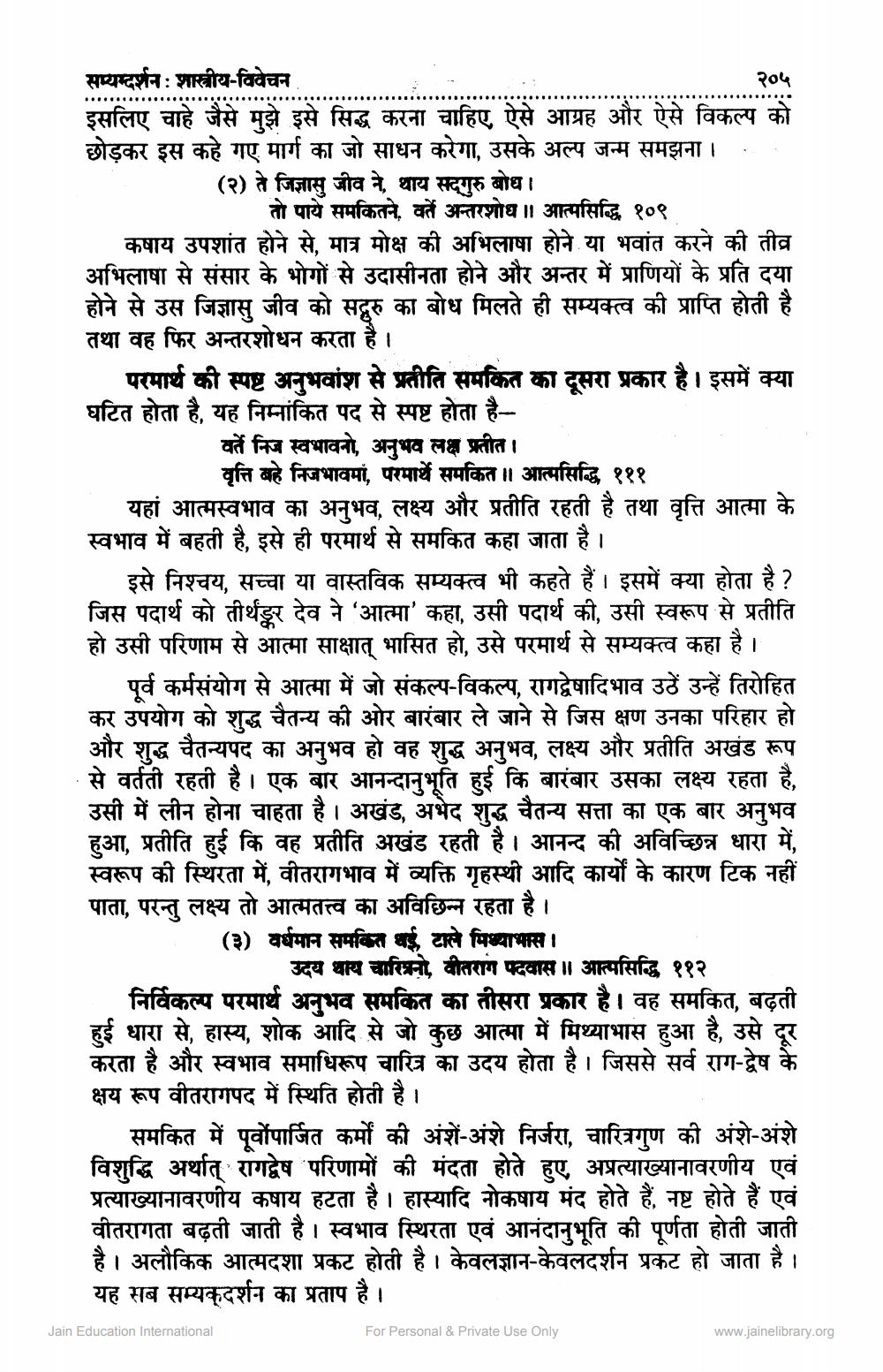________________
सम्यग्दर्शन : शास्त्रीय- विवेचन
२०५
इसलिए चाहे जैसे मुझे इसे सिद्ध करना चाहिए ऐसे आग्रह और ऐसे विकल्प को छोड़कर इस कहे गए मार्ग का जो साधन करेगा, उसके अल्प जन्म समझना । (२) ते जिज्ञासु जीव ने, थाय सद्गुरु बोध ।
तो पाये समकितने वर्ते अन्तरशोध ।। आत्मसिद्धि १०९
कषाय उपशांत होने से, मात्र मोक्ष की अभिलाषा होने या भवांत करने की तीव्र अभिलाषा से संसार के भोगों से उदासीनता होने और अन्तर में प्राणियों के प्रति दया होने से उस जिज्ञासु जीव को सद्गुरु का बोध मिलते ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तथा वह फिर अन्तरशोधन करता है।
1
परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश से प्रतीति समकित का दूसरा प्रकार है। इसमें क्या घटित होता है, यह निम्नांकित पद से स्पष्ट होता है
वर्ते निज स्वभावनो, अनुभव लक्ष प्रतीत ।
वृत्ति बहे निजभावमां, परमार्थे समकित ।। आत्मसिद्धि १११
यहां आत्मस्वभाव का अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति रहती है तथा वृत्ति आत्मा के स्वभाव में बहती है, इसे ही परमार्थ से समकित कहा जाता है ।
इसे निश्चय, सच्चा या वास्तविक सम्यक्त्व भी कहते हैं । इसमें क्या होता है ? जिस पदार्थ को तीर्थंङ्कर देव ने 'आत्मा' कहा, उसी पदार्थ की, उसी स्वरूप से प्र हो उसी परिणाम से आत्मा साक्षात् भासित हो, उसे परमार्थ से सम्यक्त्व कहा है 1
पूर्व कर्मसंयोग से आत्मा में जो संकल्प - विकल्प, रागद्वेषादिभाव उठें उन्हें तिरोहित कर उपयोग को शुद्ध चैतन्य की ओर बारंबार ले जाने से जिस क्षण उनका परिहार हो और शुद्ध चैतन्यपद का अनुभव हो वह शुद्ध अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति अखंड रूप से वर्तती रहती है। एक बार आनन्दानुभूति हुई कि बारंबार उसका लक्ष्य रहता है, उसी में लीन होना चाहता है । अखंड, अभेद शुद्ध चैतन्य सत्ता का एक बार अनुभव हुआ, प्रतीति हुई कि वह प्रतीति अखंड रहती है। आनन्द की अविच्छिन्न धारा में, स्वरूप की स्थिरता में, वीतरागभाव में व्यक्ति गृहस्थी आदि कार्यों के कारण टिक नहीं पाता, परन्तु लक्ष्य तो आत्मतत्त्व का अविछिन्न रहता है ।
(३)
वर्धमान समकित थई, टाले मिथ्याभास ।
उदय थाय चारित्रनो, वीतराग पदवास । आत्मसिद्धि ११२
निर्विकल्प परमार्थ अनुभव समकित का तीसरा प्रकार है । वह समकित बढ़ती हुई धारा से, हास्य, शोक आदि से जो कुछ आत्मा में मिथ्याभास हुआ है, उसे दूर करता है और स्वभाव समाधिरूप चारित्र का उदय होता है । जिससे सर्व राग-द्वेष के क्षय रूप वीतरागपद में स्थिति होती है 1
समकित में पूर्वोपार्जित कर्मों की अंशें- अंशे निर्जरा, चारित्रगुण की अंशे-अंशे विशुद्धि अर्थात् रागद्वेष परिणामों की मंदता होते हुए, अप्रत्याख्यानावरणीय एवं प्रत्याख्यानावरणीय कषाय हटता है । हास्यादि नोकषाय मंद होते हैं, नष्ट होते हैं एवं वीतरागता बढ़ती जाती है । स्वभाव स्थिरता एवं आनंदानुभूति की पूर्णता होती जाती है । अलौकिक आत्मदशा प्रकट होती है । केवलज्ञान- केवलदर्शन प्रकट हो जाता है । यह सब सम्यक्दर्शन का प्रताप है ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org