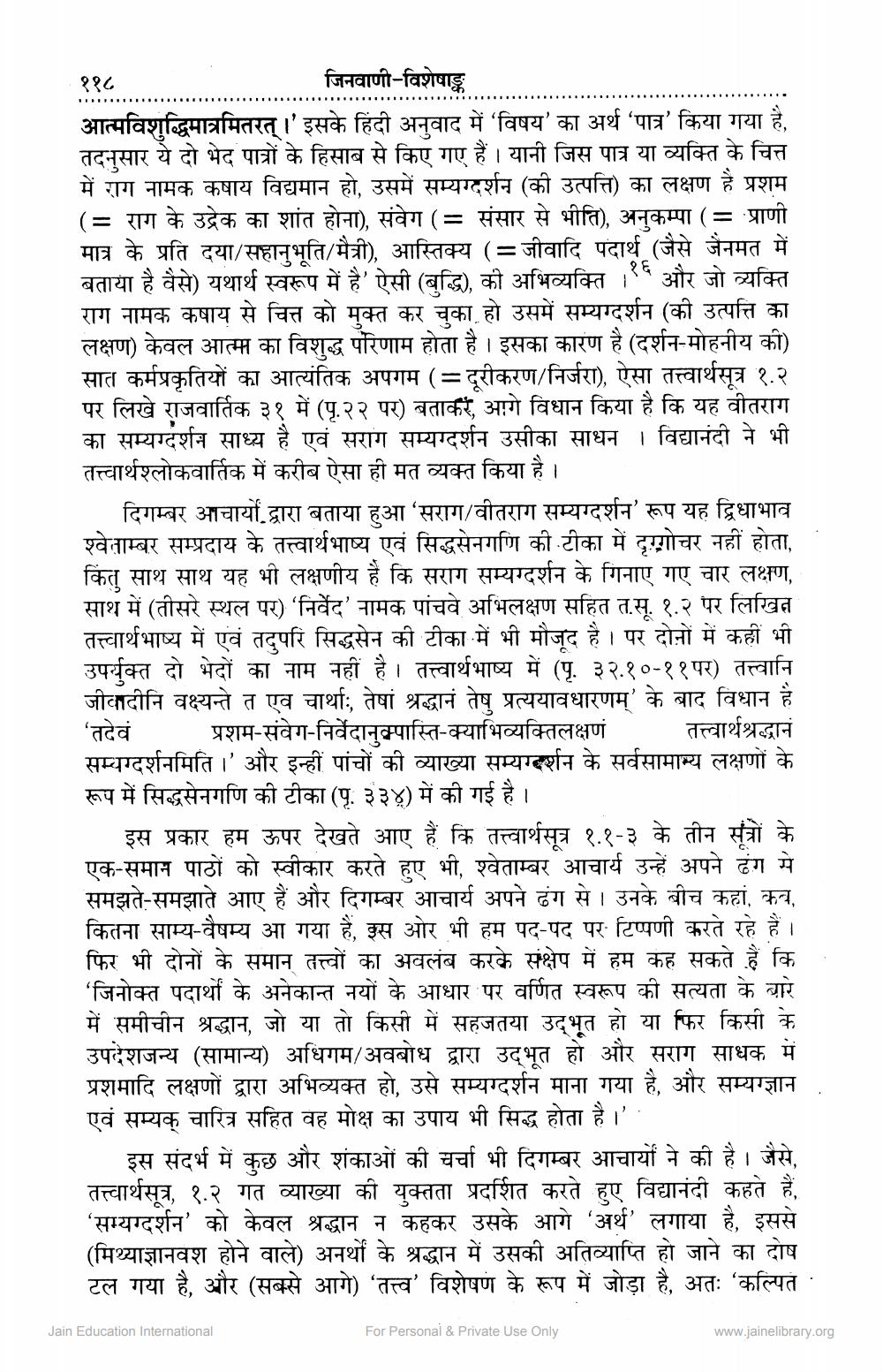________________
११८
जिनवाणी-विशेषाङ्क आत्मविशुद्धिमात्रमितरत्।' इसके हिंदी अनुवाद में 'विषय' का अर्थ ‘पात्र' किया गया है, तदनुसार ये दो भेद पात्रों के हिसाब से किए गए हैं। यानी जिस पात्र या व्यक्ति के चित्त में राग नामक कषाय विद्यमान हो, उसमें सम्यग्दर्शन (की उत्पत्ति) का लक्षण है प्रशम (= राग के उद्रेक का शांत होना), संवेग (= संसार से भीति), अनुकम्पा (= प्राणी मात्र के प्रति दया/सहानुभूति/मैत्री), आस्तिक्य (= जीवादि पदार्थ (जैसे जैनमत में बताया है वैसे) यथार्थ स्वरूप में है' ऐसी (बुद्धि), की अभिव्यक्ति ।१६ और जो व्यक्ति राग नामक कषाय से चित्त को मुक्त कर चुका हो उसमें सम्यग्दर्शन (की उत्पत्ति का लक्षण) केवल आत्मा का विशुद्ध परिणाम होता है। इसका कारण है (दर्शन-मोहनीय की) सात कर्मप्रकृतियों का आत्यंतिक अपगम (= दूरीकरण/निर्जरा), ऐसा तत्त्वार्थसूत्र १.२ पर लिखे राजवार्तिक ३१ में (पृ.२२ पर) बताकर, आगे विधान किया है कि यह वीतराग का सम्यग्दर्शन साध्य है एवं सराग सम्यग्दर्शन उसीका साधन । विद्यानंदी ने भी तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक में करीब ऐसा ही मत व्यक्त किया है।
दिगम्बर आचार्यों द्वारा बताया हुआ ‘सराग/वीतराग सम्यग्दर्शन' रूप यह द्विधाभाव श्वेताम्बर सम्प्रदाय के तत्त्वार्थभाष्य एवं सिद्धसेनगणि की टीका में दृग्गोचर नहीं होता, किंतु साथ साथ यह भी लक्षणीय है कि सराग सम्यग्दर्शन के गिनाए गए चार लक्षण, साथ में (तीसरे स्थल पर) 'निर्वेद' नामक पांचवे अभिलक्षण सहित त.सू. १.२ पर लिखित तत्त्वार्थभाष्य में एवं तद्परि सिद्धसेन की टीका में भी मौजूद है। पर दोनों में कहीं भी उपर्युक्त दो भेदों का नाम नहीं है। तत्त्वार्थभाष्य में (पृ. ३२.१०-११ पर) तत्त्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते त एव चार्थाः, तेषां श्रद्धानं तेषु प्रत्ययावधारणम्' के बाद विधान है 'तदेवं प्रशम-संवेग-निर्वेदानुम्पास्ति-क्याभिव्यक्तिलक्षणं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमिति ।' और इन्हीं पांचों की व्याख्या सम्यग्दर्शन के सर्वसामान्य लक्षणों के रूप में सिद्धसेनगणि की टीका (पृ. ३३४) में की गई है।
इस प्रकार हम ऊपर देखते आए हैं कि तत्त्वार्थसूत्र १.१-३ के तीन संत्रों के एक-समान पाठों को स्वीकार करते हुए भी, श्वेताम्बर आचार्य उन्हें अपने ढंग से समझते-समझाते आए हैं और दिगम्बर आचार्य अपने ढंग से। उनके बीच कहां, कब, कितना साम्य-वैषम्य आ गया है, इस ओर भी हम पद-पद पर टिप्पणी करते रहे हैं। फिर भी दोनों के समान तत्त्वों का अवलंब करके संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 'जिनोक्त पदार्थों के अनेकान्त नयों के आधार पर वर्णित स्वरूप की सत्यता के बारे में समीचीन श्रद्धान, जो या तो किसी में सहजतया उद्भुत हो या फिर किसी के उपदेशजन्य (सामान्य) अधिगम/अवबोध द्वारा उद्भूत हो और सराग साधक में प्रशमादि लक्षणों द्वारा अभिव्यक्त हो, उसे सम्यग्दर्शन माना गया है, और सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र सहित वह मोक्ष का उपाय भी सिद्ध होता है।'
इस संदर्भ में कुछ और शंकाओं की चर्चा भी दिगम्बर आचार्यों ने की है। जैसे, तत्त्वार्थसूत्र, १.२ गत व्याख्या की युक्तता प्रदर्शित करते हुए विद्यानंदी कहते हैं, 'सम्यग्दर्शन' को केवल श्रद्धान न कहकर उसके आगे 'अर्थ' लगाया है, इससे (मिथ्याज्ञानवश होने वाले) अनर्थों के श्रद्धान में उसकी अतिव्याप्ति हो जाने का दोष टल गया है, और (सबसे आगे) 'तत्त्व' विशेषण के रूप में जोड़ा है, अतः ‘कल्पित .
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org