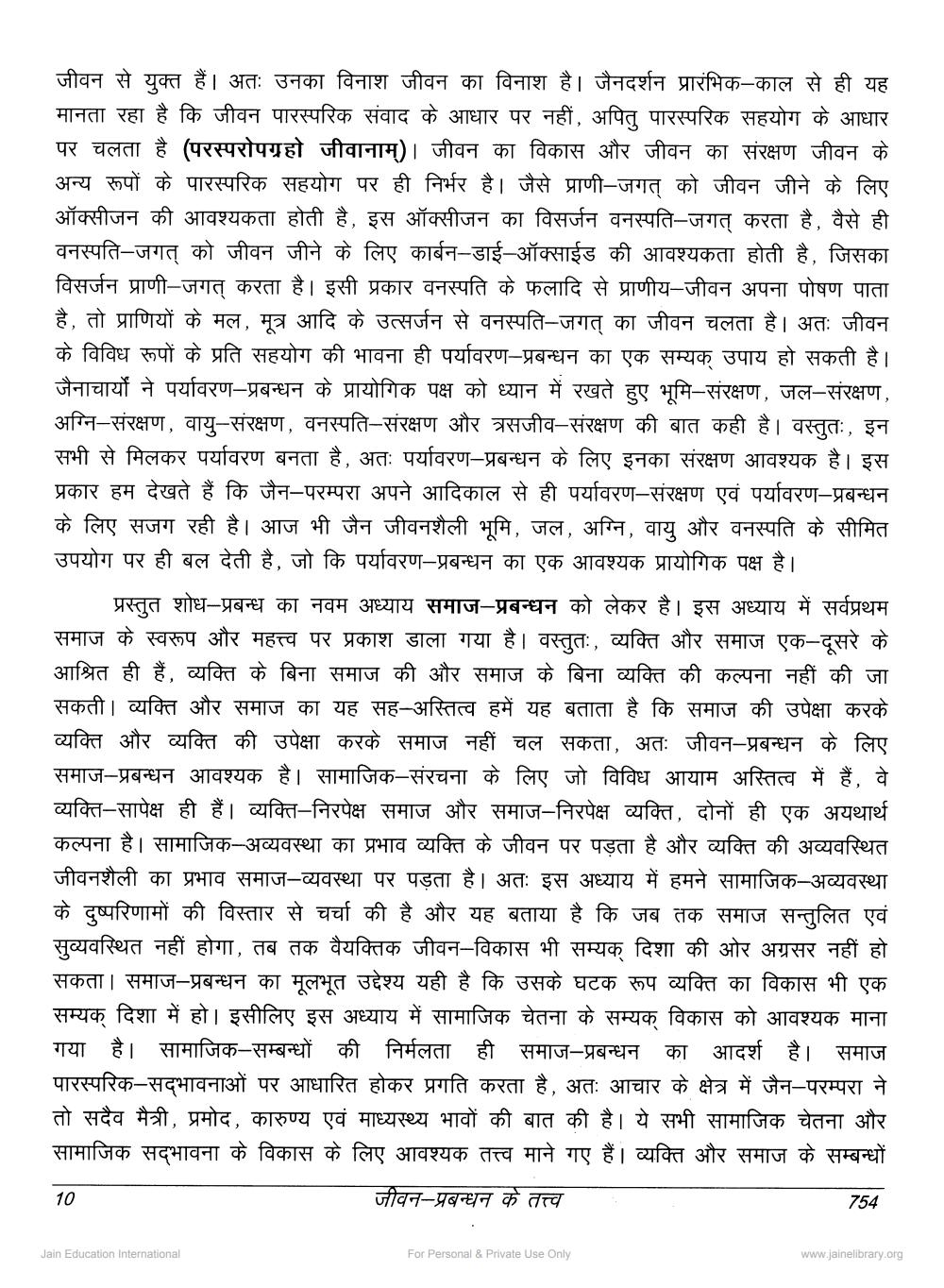________________
जीवन से युक्त हैं। अतः उनका विनाश जीवन का विनाश है। जैनदर्शन प्रारंभिक काल से ही यह मानता रहा है कि जीवन पारस्परिक संवाद के आधार पर नहीं, अपितु पारस्परिक सहयोग के आधार पर चलता है ( परस्परोपग्रहो जीवानाम् ) । जीवन का विकास और जीवन का संरक्षण जीवन के अन्य रूपों के पारस्परिक सहयोग पर ही निर्भर है। जैसे प्राणी जगत् को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस ऑक्सीजन का विसर्जन वनस्पति- जगत् करता है, वैसे ही वनस्पति - जगत् को जीवन जीने के लिए कार्बन-डाई-ऑक्साईड की आवश्यकता होती है, जिसका विसर्जन प्राणी-जगत् करता है। इसी प्रकार वनस्पति के फलादि से प्राणीय-जीवन अपना पोषण पाता है, तो प्राणियों के मल, मूत्र आदि के उत्सर्जन से वनस्पति- जगत् का जीवन चलता है। अतः जीवन के विविध रूपों के प्रति सहयोग की भावना ही पर्यावरण - प्रबन्धन का एक सम्यक् उपाय सकती है। जैनाचार्यों ने पर्यावरण - प्रबन्धन के प्रायोगिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए भूमि संरक्षण, जल-संरक्षण, अग्नि-संरक्षण, वायु-संरक्षण, वनस्पति-संरक्षण और त्रसजीव - संरक्षण की बात कही है। वस्तुतः, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है, अतः पर्यावरण- प्रबन्धन के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन - परम्परा अपने आदिकाल से ही पर्यावरण-संरक्षण एवं पर्यावरण-प्रबन्धन के लिए सजग रही है। आज भी जैन जीवनशैली भूमि, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के सीमित उपयोग पर ही बल देती है, जो कि पर्यावरण - प्रबन्धन का एक आवश्यक प्रायोगिक पक्ष है ।
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का नवम अध्याय समाज - प्रबन्धन को लेकर है । इस अध्याय में सर्वप्रथम समाज के स्वरूप और महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः, व्यक्ति और समाज एक-दूसरे के आश्रित ही हैं, व्यक्ति के बिना समाज की और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती । व्यक्ति और समाज का यह सह-अस्तित्व हमें यह बताता है कि समाज की उपेक्षा करके व्यक्ति और व्यक्ति की उपेक्षा करके समाज नहीं चल सकता, अतः जीवन - प्रबन्धन के लिए समाज-प्रबन्धन आवश्यक है। सामाजिक संरचना के लिए जो विविध आयाम अस्तित्व में हैं, वे व्यक्ति - सापेक्ष ही हैं। व्यक्ति-निरपेक्ष समाज और समाज-निरपेक्ष व्यक्ति, दोनों ही एक अयथार्थ कल्पना है। सामाजिक - अव्यवस्था का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति की अव्यवस्थित जीवनशैली का प्रभाव समाज-व्यवस्था पर पड़ता है। अतः इस अध्याय में हमने सामाजिक - अव्यवस्था के दुष्परिणामों की विस्तार से चर्चा की है और यह बताया है कि जब तक समाज सन्तुलित एवं सुव्यवस्थित नहीं होगा, तब तक वैयक्तिक जीवन - विकास भी सम्यक् दिशा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। समाज–प्रबन्धन का मूलभूत उद्देश्य यही है कि उसके घटक रूप व्यक्ति का विकास भी एक सम्यक् दिशा में हो। इसीलिए इस अध्याय में सामाजिक चेतना के सम्यक् विकास को आवश्यक माना गया है। सामाजिक - सम्बन्धों की निर्मलता ही समाज - प्रबन्धन का आदर्श है । समाज पारस्परिक - सद्भावनाओं पर आधारित होकर प्रगति करता है, अतः आचार के क्षेत्र में जैन - परम्परा ने तो सदैव मैत्री, प्रमोद, कारुण्य एवं माध्यस्थ्य भावों की बात की है। ये सभी सामाजिक चेतना और सामाजिक सद्भावना के विकास के लिए आवश्यक तत्त्व माने गए हैं। व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों
754
जीवन-प्रबन्धन के तत्त्व
10
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org