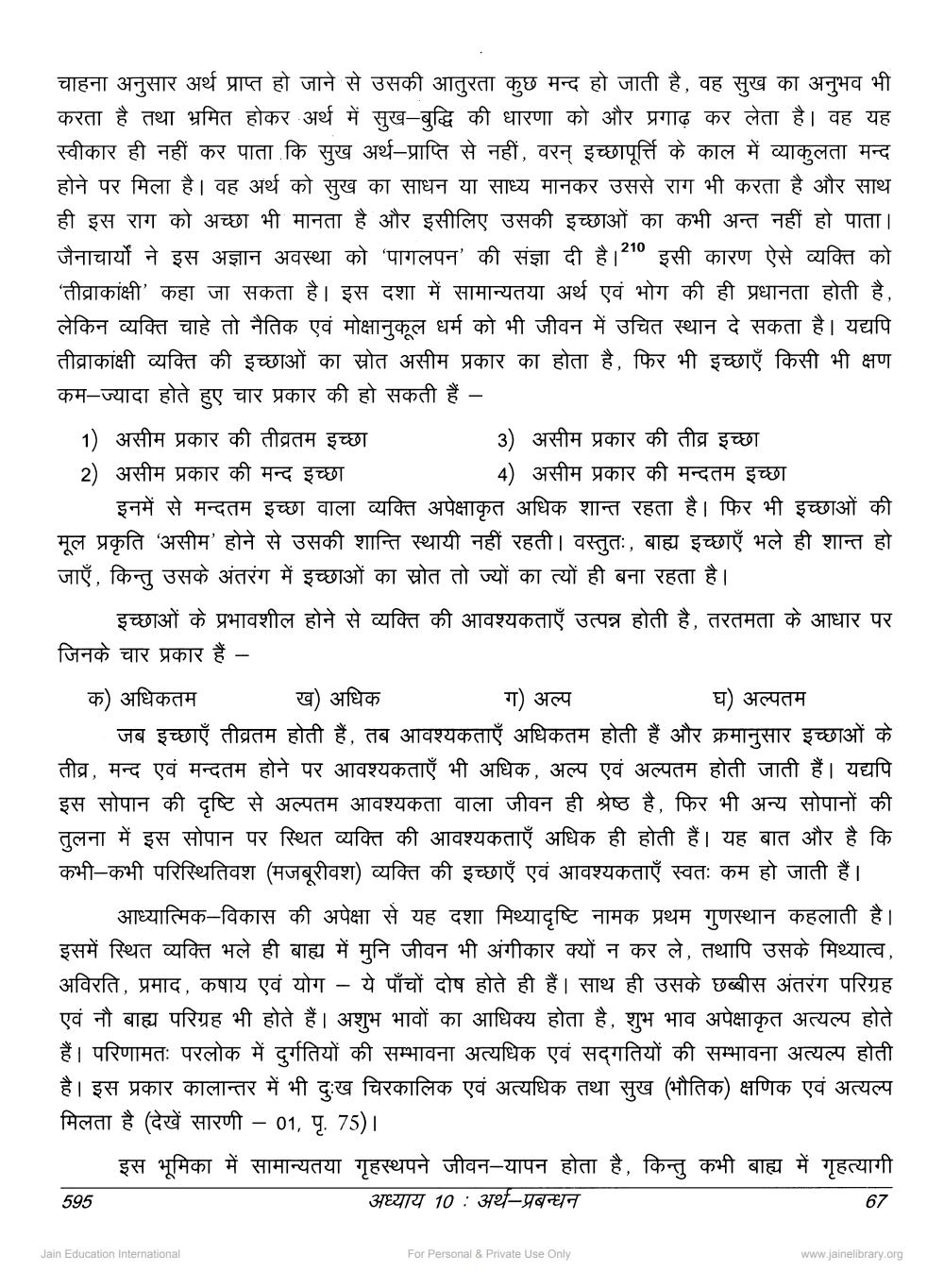________________
चाहना अनुसार अर्थ प्राप्त हो जाने से उसकी आतुरता कुछ मन्द हो जाती है, वह सुख का अनुभव भी करता है तथा भ्रमित होकर अर्थ में सुख-बुद्धि की धारणा को और प्रगाढ़ कर लेता है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि सुख अर्थ-प्राप्ति से नहीं, वरन् इच्छापूर्ति के काल में व्याकुलता मन्द होने पर मिला है। वह अर्थ को सुख का साधन या साध्य मानकर उससे राग भी करता है और साथ ही इस राग को अच्छा भी मानता है और इसीलिए उसकी इच्छाओं का कभी अन्त नहीं हो पाता। जैनाचार्यों ने इस अज्ञान अवस्था को ‘पागलपन' की संज्ञा दी है।210 इसी कारण ऐसे व्यक्ति को 'तीव्राकांक्षी' कहा जा सकता है। इस दशा में सामान्यतया अर्थ एवं भोग की ही प्रधानता होती है, लेकिन व्यक्ति चाहे तो नैतिक एवं मोक्षानुकूल धर्म को भी जीवन में उचित स्थान दे सकता है। यद्यपि तीव्राकांक्षी व्यक्ति की इच्छाओं का स्रोत असीम प्रकार का होता है, फिर भी इच्छाएँ किसी भी क्षण कम-ज्यादा होते हुए चार प्रकार की हो सकती हैं - 1) असीम प्रकार की तीव्रतम इच्छा
3) असीम प्रकार की तीव्र इच्छा 2) असीम प्रकार की मन्द इच्छा
4) असीम प्रकार की मन्दतम इच्छा इनमें से मन्दतम इच्छा वाला व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक शान्त रहता है। फिर भी इच्छाओं की मूल प्रकृति 'असीम' होने से उसकी शान्ति स्थायी नहीं रहती। वस्तुतः, बाह्य इच्छाएँ भले ही शान्त हो जाएँ, किन्तु उसके अंतरंग में इच्छाओं का स्रोत तो ज्यों का त्यों ही बना रहता है।
इच्छाओं के प्रभावशील होने से व्यक्ति की आवश्यकताएँ उत्पन्न होती है, तरतमता के आधार पर जिनके चार प्रकार हैं - क) अधिकतम ख) अधिक
ग) अल्प
घ) अल्पतम जब इच्छाएँ तीव्रतम होती हैं, तब आवश्यकताएँ अधिकतम होती हैं और क्रमानुसार इच्छाओं के तीव्र, मन्द एवं मन्दतम होने पर आवश्यकताएँ भी अधिक , अल्प एवं अल्पतम होती जाती हैं। यद्यपि इस सोपान की दृष्टि से अल्पतम आवश्यकता वाला जीवन ही श्रेष्ठ है, फिर भी अन्य सोपानों की तुलना में इस सोपान पर स्थित व्यक्ति की आवश्यकताएँ अधिक ही होती हैं। यह बात और है कि कभी-कभी परिस्थितिवश (मजबूरीवश) व्यक्ति की इच्छाएँ एवं आवश्यकताएँ स्वतः कम हो जाती हैं।
आध्यात्मिक-विकास की अपेक्षा से यह दशा मिथ्यादृष्टि नामक प्रथम गुणस्थान कहलाती है। इसमें स्थित व्यक्ति भले ही बाह्य में मुनि जीवन भी अंगीकार क्यों न कर ले, तथापि उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योग - ये पाँचों दोष होते ही हैं। साथ ही उसके छब्बीस अंतरंग परिग्रह एवं नौ बाह्य परिग्रह भी होते हैं। अशुभ भावों का आधिक्य होता है, शुभ भाव अपेक्षाकृत अत्यल्प होते हैं। परिणामतः परलोक में दुर्गतियों की सम्भावना अत्यधिक एवं सद्गतियों की सम्भावना अत्यल्प होती है। इस प्रकार कालान्तर में भी दुःख चिरकालिक एवं अत्यधिक तथा सुख (भौतिक) क्षणिक एवं अत्यल्प मिलता है (देखें सारणी – 01, पृ. 75)।
इस भूमिका में सामान्यतया गृहस्थपने जीवन-यापन होता है, किन्तु कभी बाह्य में गृहत्यागी 595
अध्याय 10: अर्थ-प्रबन्धन
67
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org