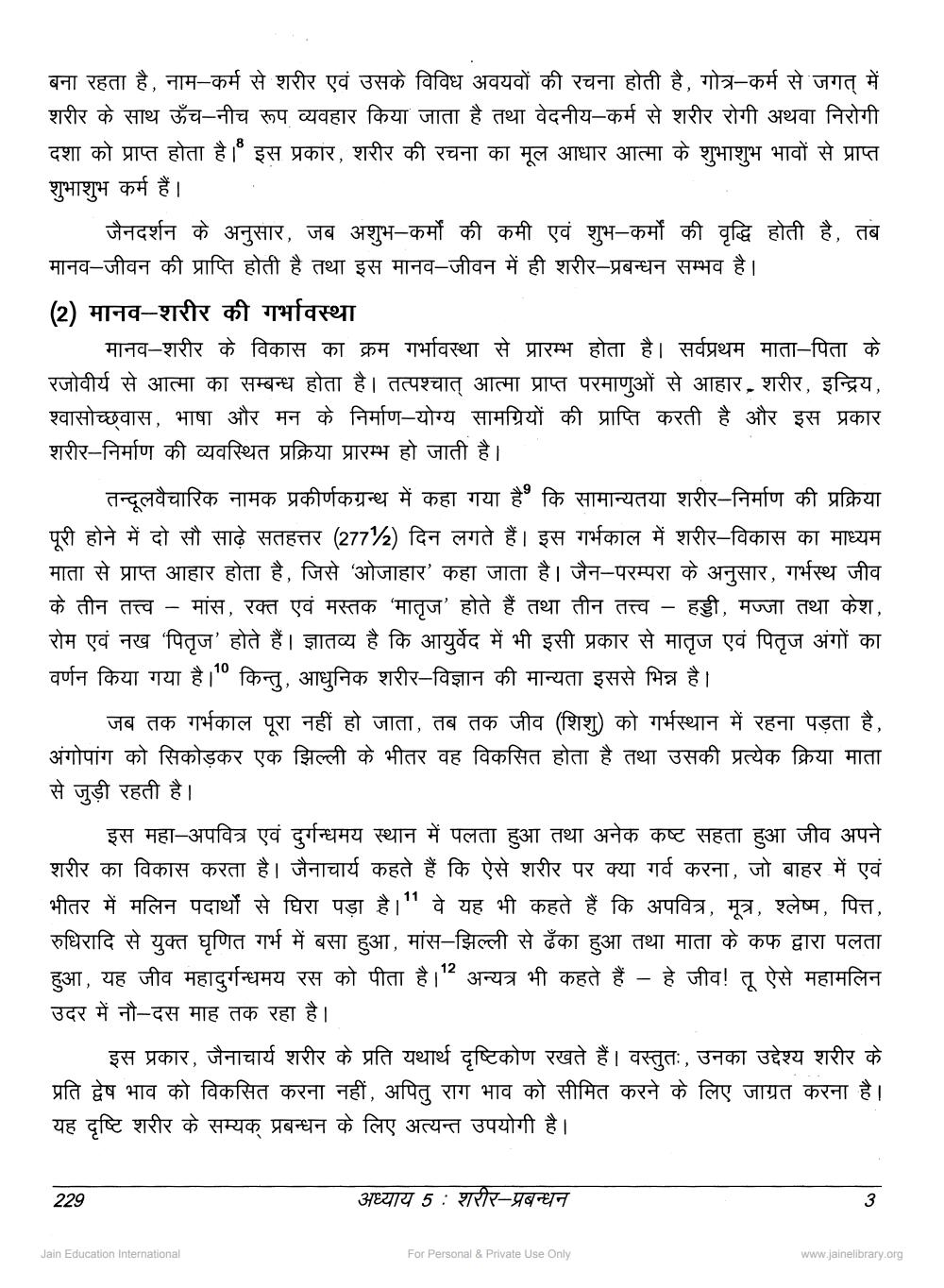________________
बना रहता है, नाम-कर्म से शरीर एवं उसके विविध अवयवों की रचना होती है, गोत्र - कर्म से जगत् में शरीर के साथ ऊँच-नीच रूप व्यवहार किया जाता है तथा वेदनीय कर्म से शरीर रोगी अथवा निरोगी दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार, शरीर की रचना का मूल आधार आत्मा के शुभाशुभ भावों से प्राप्त शुभाशुभ कर्म हैं।
जैनदर्शन के अनुसार, जब अशुभ कर्मों की कमी एवं शुभ कर्मों की वृद्धि होती है, तब मानव-जीवन की प्राप्ति होती है तथा इस मानव-जीवन में ही शरीर - प्रबन्धन सम्भव है ।
(2) मानव - शरीर की गर्भावस्था
मानव-शरीर के विकास का क्रम गर्भावस्था से प्रारम्भ होता है। सर्वप्रथम माता-पिता के रजोवीर्य से आत्मा का सम्बन्ध होता है । तत्पश्चात् आत्मा प्राप्त परमाणुओं से आहार शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन के निर्माण - योग्य सामग्रियों की प्राप्ति करती है और इस प्रकार शरीर - निर्माण की व्यवस्थित प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।
तन्दूलवैचारिक नामक प्रकीर्णकग्रन्थ में कहा गया है कि सामान्यतया शरीर-निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने में दो सौ साढ़े सतहत्तर (2771/2) दिन लगते हैं। इस गर्भकाल में शरीर - विकास का माध्यम माता से प्राप्त आहार होता है, जिसे 'ओजाहार' कहा जाता है। जैन - परम्परा के अनुसार, गर्भस्थ जीव के तीन तत्त्व मांस, रक्त एवं मस्तक 'मातृज' होते हैं तथा तीन तत्त्व हड्डी, मज्जा तथा केश, रोम एवं नख ‘पितृज' होते हैं। ज्ञातव्य है कि आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से मातृज एवं पितृज अंगों का वर्णन किया गया है।1° किन्तु, आधुनिक शरीर - विज्ञान की मान्यता इससे भिन्न है।
10
-
जब तक गर्भकाल पूरा नहीं हो जाता, तब तक जीव (शिशु) को गर्भस्थान में रहना पड़ता है, अंगोपांग को सिकोड़कर एक झिल्ली के भीतर वह विकसित होता है तथा उसकी प्रत्येक क्रिया माता से जुड़ी रहती है।
इस महा - अपवित्र एवं दुर्गन्धमय स्थान में पलता हुआ तथा अनेक कष्ट सहता हुआ जीव अपने शरीर का विकास करता है। जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसे शरीर पर क्या गर्व करना, जो बाहर में एवं भीतर में मलिन पदार्थों से घिरा पड़ा है। 11 वे यह भी कहते हैं कि अपवित्र, मूत्र, श्लेष्म, पित्त, रुधिरादि से युक्त घृणित गर्भ में बसा हुआ, मांस- झिल्ली से ढँका हुआ तथा माता के कफ द्वारा पलता हुआ, यह जीव महादुर्गन्धमय रस को पीता है। 12 अन्यत्र भी कहते हैं हे जीव ! तू ऐसे महामलिन उदर में नौ-दस माह तक रहा है।
229
इस प्रकार, जैनाचार्य शरीर के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण रखते हैं। वस्तुतः, उनका उद्देश्य शरीर के प्रति द्वेष भाव को विकसित करना नहीं, अपितु राग भाव को सीमित करने के लिए जाग्रत करना है। यह दृष्टि शरीर के सम्यक् प्रबन्धन के लिए अत्यन्त उपयोगी है।
Jain Education International
-
अध्याय 5: शरीर-प्रबन्धन
-
For Personal & Private Use Only
3
www.jainelibrary.org