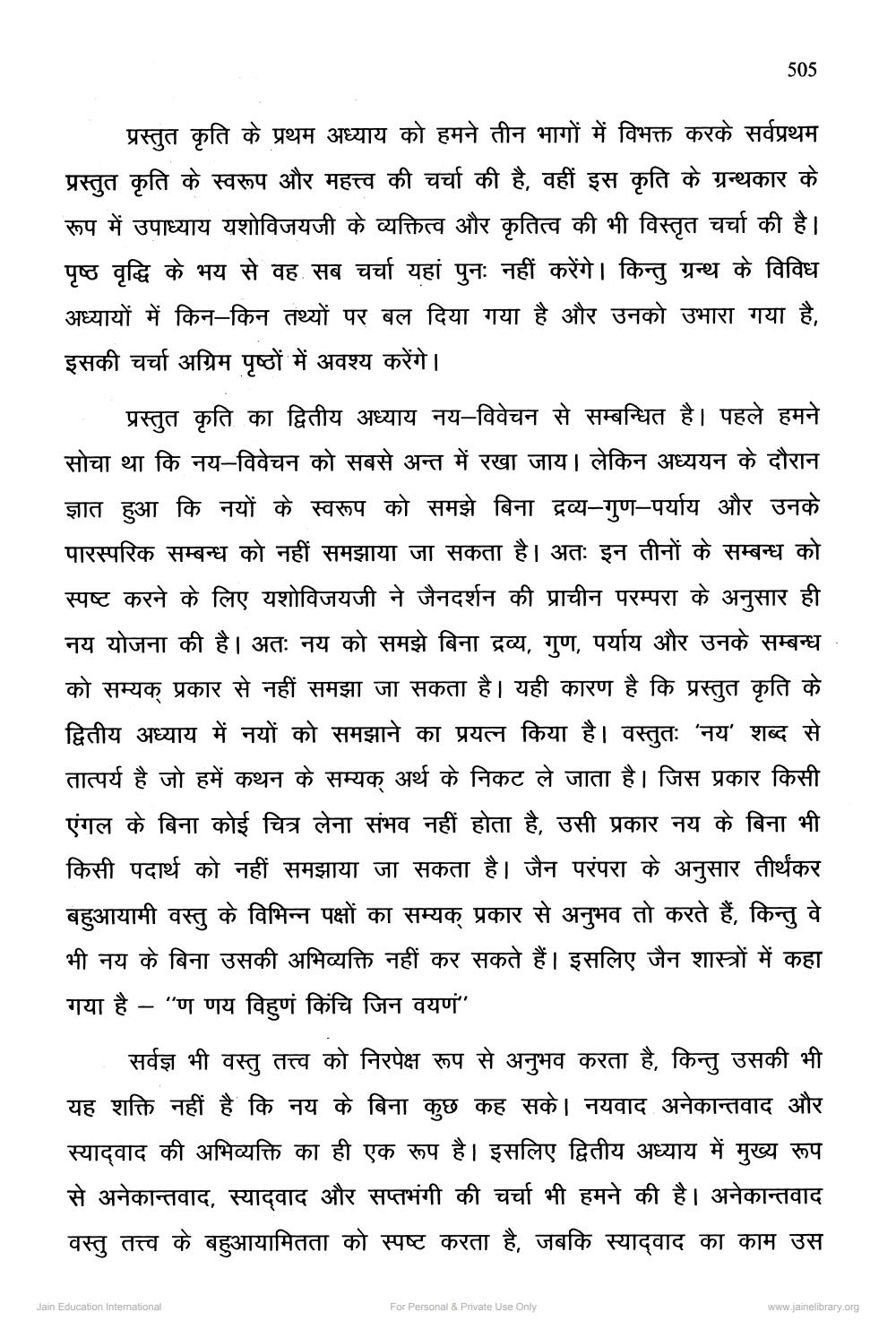________________
प्रस्तुत कृति के प्रथम अध्याय को हमने तीन भागों में विभक्त करके सर्वप्रथम प्रस्तुत कृति के स्वरूप और महत्त्व की चर्चा की है, वहीं इस कृति के ग्रन्थकार के रूप में उपाध्याय यशोविजयजी के व्यक्तित्व और कृतित्व की भी विस्तृत चर्चा की है । पृष्ठ वृद्धि के भय से वह सब चर्चा यहां पुनः नहीं करेंगे। किन्तु ग्रन्थ के विविध अध्यायों में किन-किन तथ्यों पर बल दिया गया है और उनको उभारा गया है, इसकी चर्चा अग्रिम पृष्ठों में अवश्य करेंगे।
प्रस्तुत कृति का द्वितीय अध्याय नय - विवेचन से सम्बन्धित है। पहले हमने सोचा था कि नय - विवेचन को सबसे अन्त में रखा जाय । लेकिन अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि नयों के स्वरूप को समझे बिना द्रव्य - गुण - पर्याय और उनके पारस्परिक सम्बन्ध को नहीं समझाया जा सकता है। अतः इन तीनों के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए यशोविजयजी ने जैनदर्शन की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही नय योजना की है। अतः नय को समझे बिना द्रव्य, गुण, पर्याय और उनके सम्बन्ध को सम्यक् प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। यही कारण है कि प्रस्तुत कृति के द्वितीय अध्याय में नयों को समझाने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः 'नय' शब्द से तात्पर्य है जो हमें कथन के सम्यक् अर्थ के निकट ले जाता है। जिस प्रकार किसी एंगल के बिना कोई चित्र लेना संभव नहीं होता है, उसी प्रकार नय के बिना भी किसी पदार्थ को नहीं समझाया जा सकता है। जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकर बहुआयामी वस्तु के विभिन्न पक्षों का सम्यक् प्रकार से अनुभव तो करते हैं, किन्तु वे भी नय के बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैन शास्त्रों में कहा गया है " ण णय विहुणं किंचि जिन वयणं"
—
505
सर्वज्ञ भी वस्तु तत्त्व को निरपेक्ष रूप से अनुभव करता है, किन्तु उसकी भी यह शक्ति नहीं है कि नय के बिना कुछ कह सके। नयवाद अनेकान्तवाद और स्याद्वाद की अभिव्यक्ति का ही एक रूप है। इसलिए द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से अनेकान्तवाद, स्याद्वाद और सप्तभंगी की चर्चा भी हमने की है । अनेकान्तवाद वस्तु तत्त्व के बहुआयामितता को स्पष्ट करता है, जबकि स्याद्वाद का काम उस
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org