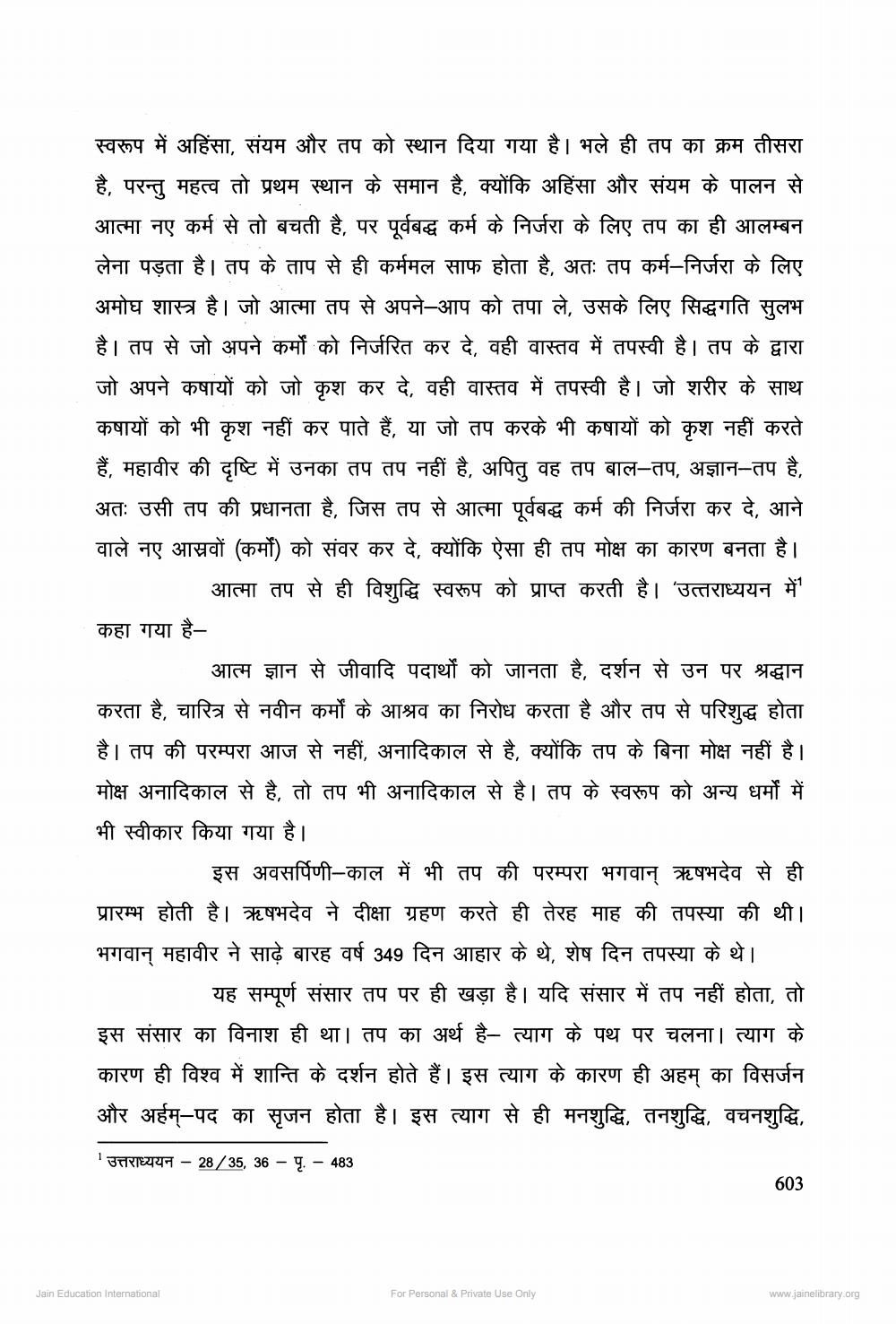________________
स्वरूप में अहिंसा, संयम और तप को स्थान दिया गया है। भले ही तप का क्रम तीसरा है, परन्तु महत्व तो प्रथम स्थान के समान है, क्योंकि अहिंसा और संयम के पालन से आत्मा नए कर्म से तो बचती है, पर पूर्वबद्ध कर्म के निर्जरा के लिए तप का ही आलम्बन लेना पड़ता है। तप के ताप से ही कर्ममल साफ होता है, अतः तप कर्म-निर्जरा के लिए अमोघ शास्त्र है। जो आत्मा तप से अपने-आप को तपा ले, उसके लिए सिद्धगति सुलभ है। तप से जो अपने कर्मों को निर्जरित कर दे, वही वास्तव में तपस्वी है। तप के द्वारा जो अपने कषायों को जो कृश कर दे, वही वास्तव में तपस्वी है। जो शरीर के साथ कषायों को भी कृश नहीं कर पाते हैं, या जो तप करके भी कषायों को कृश नहीं करते हैं, महावीर की दृष्टि में उनका तप तप नहीं है, अपितु वह तप बाल-तप, अज्ञान-तप है, अतः उसी तप की प्रधानता है, जिस तप से आत्मा पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा कर दे, आने वाले नए आस्रवों (कर्मों) को संवर कर दे, क्योंकि ऐसा ही तप मोक्ष का कारण बनता है।
आत्मा तप से ही विशुद्धि स्वरूप को प्राप्त करती है। 'उत्तराध्ययन में कहा गया है
आत्म ज्ञान से जीवादि पदार्थों को जानता है, दर्शन से उन पर श्रद्धान करता है, चारित्र से नवीन कर्मों के आश्रव का निरोध करता है और तप से परिशुद्ध होता है। तप की परम्परा आज से नहीं, अनादिकाल से है, क्योंकि तप के बिना मोक्ष नहीं है। मोक्ष अनादिकाल से है, तो तप भी अनादिकाल से है। तप के स्वरूप को अन्य धर्मों में भी स्वीकार किया गया है।
इस अवसर्पिणी-काल में भी तप की परम्परा भगवान् ऋषभदेव से ही प्रारम्भ होती है। ऋषभदेव ने दीक्षा ग्रहण करते ही तेरह माह की तपस्या की थी। भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष 349 दिन आहार के थे, शेष दिन तपस्या के थे।
यह सम्पूर्ण संसार तप पर ही खड़ा है। यदि संसार में तप नहीं होता, तो इस संसार का विनाश ही था। तप का अर्थ है- त्याग के पथ पर चलना। त्याग के कारण ही विश्व में शान्ति के दर्शन होते हैं। इस त्याग के कारण ही अहम् का विसर्जन और अर्हम्-पद का सृजन होता है। इस त्याग से ही मनशुद्धि, तनशुद्धि, वचनशुद्धि,
1 उत्तराध्ययन - 28/35, 36 – पृ. - 483
603
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org