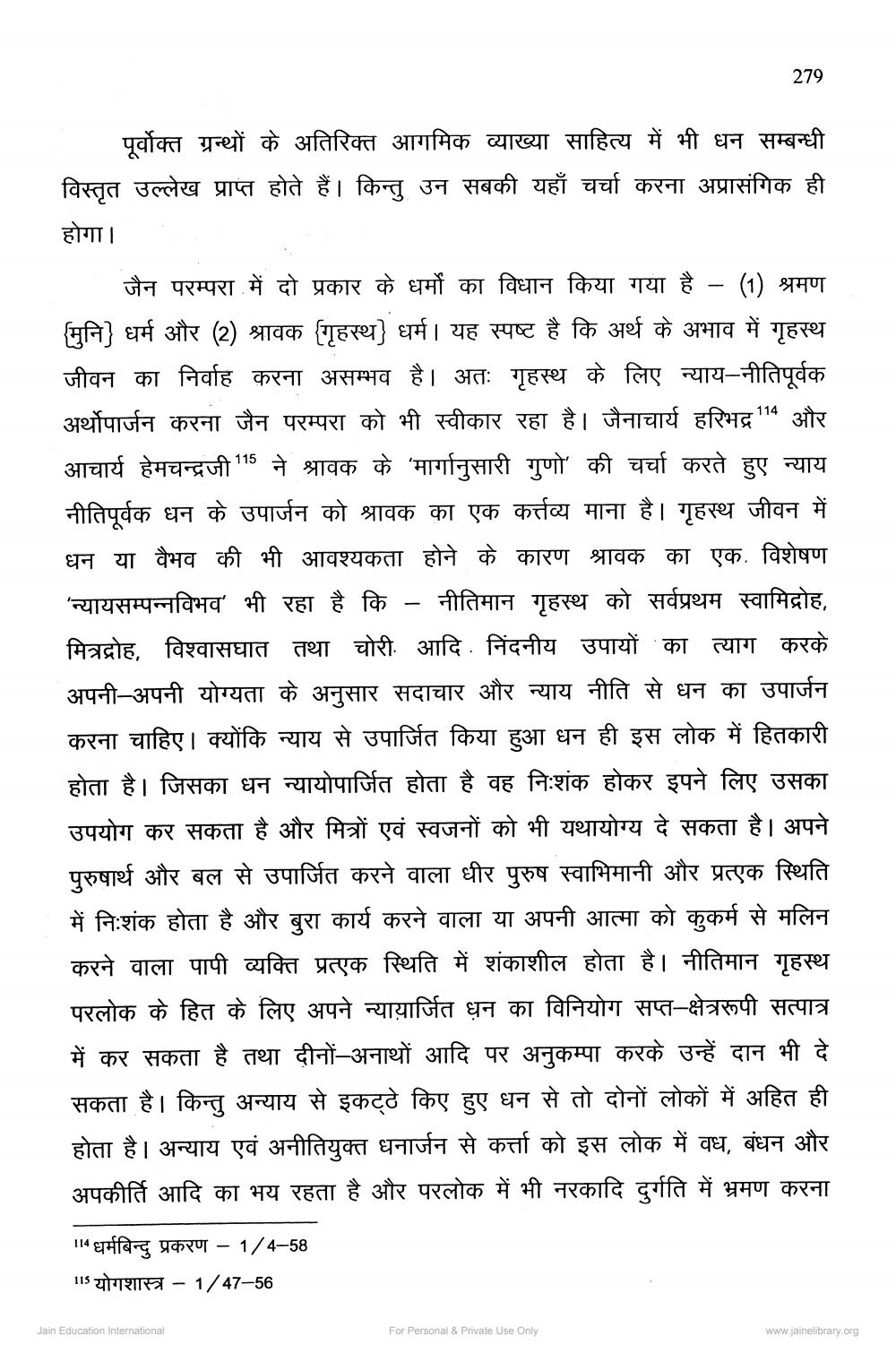________________
279
पूर्वोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त आगमिक व्याख्या साहित्य में भी धन सम्बन्धी विस्तृत उल्लेख प्राप्त होते हैं। किन्तु उन सबकी यहाँ चर्चा करना अप्रासंगिक ही होगा।
___ जैन परम्परा में दो प्रकार के धर्मों का विधान किया गया है - (1) श्रमण (मुनि) धर्म और (2) श्रावक (गृहस्थधर्म। यह स्पष्ट है कि अर्थ के अभाव में गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना असम्भव है। अतः गृहस्थ के लिए न्याय-नीतिपूर्वक अर्थोपार्जन करना जैन परम्परा को भी स्वीकार रहा है। जैनाचार्य हरिभद्र 114 और आचार्य हेमचन्द्रजी 115 ने श्रावक के 'मार्गानुसारी गुणो' की चर्चा करते हुए न्याय नीतिपूर्वक धन के उपार्जन को श्रावक का एक कर्त्तव्य माना है। गृहस्थ जीवन में धन या वैभव की भी आवश्यकता होने के कारण श्रावक का एक. विशेषण 'न्यायसम्पन्नविभव' भी रहा है कि - नीतिमान गृहस्थ को सर्वप्रथम स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात तथा चोरी. आदि . निंदनीय उपायों का त्याग करके अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार सदाचार और न्याय नीति से धन का उपार्जन करना चाहिए। क्योंकि न्याय से उपार्जित किया हुआ धन ही इस लोक में हितकारी होता है। जिसका धन न्यायोपार्जित होता है वह निःशंक होकर इपने लिए उसका उपयोग कर सकता है और मित्रों एवं स्वजनों को भी यथायोग्य दे सकता है। अपने पुरुषार्थ और बल से उपार्जित करने वाला धीर पुरुष स्वाभिमानी और प्रत्एक स्थिति में निःशंक होता है और बुरा कार्य करने वाला या अपनी आत्मा को कुकर्म से मलिन करने वाला पापी व्यक्ति प्रत्एक स्थिति में शंकाशील होता है। नीतिमान गृहस्थ परलोक के हित के लिए अपने न्यायार्जित धन का विनियोग सप्त-क्षेत्ररूपी सत्पात्र में कर सकता है तथा दीनों-अनाथों आदि पर अनुकम्पा करके उन्हें दान भी दे सकता है। किन्तु अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन से तो दोनों लोकों में अहित ही होता है। अन्याय एवं अनीतियुक्त धनार्जन से कर्ता को इस लोक में वध, बंधन और अपकीर्ति आदि का भय रहता है और परलोक में भी नरकादि दुर्गति में भ्रमण करना
14 धर्मबिन्दु प्रकरण - 1/4-58 115 योगशास्त्र - 1/47-56
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org